बीज का देरी से सही, बेहतरीन फल देना
साइकिलों पर बदहवास पैडल मारते तीन हज़ार छात्र सप्ताह में छः दिन ठीक समय पर पहुँच जाते। कपड़े कम हों या फटे पुराने. गरमी हो या बरसात या कड़ाके की सर्दी, वे हर मौसम की मार झेलते देर रात घर लौटते क्योकि कोई कोई क्लास रात को ग्यारह बजे ख़त्म होती थी। इन के पास रईसज़ादों जैसे साधन नहीं थे, दिन में होमवर्क करने का समय नहीं था। छोटे घरों में एकांत न मिल पाने के कारण ये लोग वार्षिक परीक्षाओं से पहले एक महीने की छुट्टी ले कर धूप से बचने के लिए पार्कों में पेड़ों के नीचे बैठ साल भर का कोर्स दोहराते थे।
बी.ए. की क्लास में उस सुहानी शाम वह बड़े शाहाना अंदाज़ से खिड़की की राह उतर आई। किसी शरारती लड़के ने छींटा कसा, ‘हीअर कम्स क्वीन मेरी!’ शोख़ हसीना चूकने वाली नहीं थी। तपाक से बोली, ‘क्वीन मेरी तक तो ठीक, ब्लडी मेरी मत कहना…!’ इतने सारे लड़कों के बीच उस लड़की के हौसले, बिंदासपन और रूप पर क्लास का एक शरमीला सा लड़का रीझ गया।
यह कालिज था — दिल्ली में पंजाब विश्वविद्यालय का कैंप कालिज। पंजाब से बाहर यह विशेष रूप से खोला गया था। हालात ही कुछ ऐसे थे। १९४७ में देश के टुकड़े हो जाने पर दिल्ली पाकिस्तान से आए लोगों से भर गई थी। उन्हें रिफ़्यूजी या शरणार्थी कहा जाता था। अपनी धरती से उखड़ कर नई ज़मीन पर फिर से जमने के लिए इन की जी तोड़ मेहनत देखते एक सुंदर नाम दिया गया था पुरुषार्थी। नौजवान शरणार्थियों के पास इतने साधन न थे कि दिन में किसी कालिज में बाक़ायदा पढ़ कर कोई कैरियर बना सकें। इन की मज़बूरी थी दिन में काम करना–कुछ भी, कोई भी काम, क्लर्की या बाबूगीरी, टाइपिंग, स्टेनोग्राफ़ी (उन दिनों मध्यम वर्गीय पढ़े लिखों के लिए यही प्रमुख रोज़गार थे) या किसी कारख़ाने में मज़दूरी… मतलब यह कि जो भी काम पंजाब से आए नौजवान अपना और अपने घरबार का पेट पालने के लिए कर सकें। मेरे कई मित्र तो दो दो या तीन तीन काम तक करते थे। मुख्यतः इन्हीं के लिए यह कालिज खोला गया था। इस के छात्रों में मुझ जैसे भी कुछ थे, जो शरणार्थी तो नहीं थे लेकिन पुरुषार्थी अवश्य थे। जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण पैतृक परिवार के भरण पोषण में हाथ बँटाने के लिए दिन में नौकरी करनी पड़ती थी।
शाम के साढ़े पाँच बजे खुलने वाला यह कालिज हम जैसों के लिए वरदान था, उन्नति का बंद दरवाज़ा खोलने की कुंजी था, बिगड़ी तक़दीर बनाने की तदबीर था। गोल मार्केट से सीधे बिरला मंदिर वाली सड़क पर ‘टी जंक्शन’ के ठीक सामने था अँगरेजी ज़माने का बना शानदार इमारत वोला हरकोर्ट बटलर स्कूल। पीछे अरावली शृंखला की पहाड़ियाँ होने के कारण यह जगह कुछ ऊँचाई पर थी। (इन्हीं पहाड़ियों के बबूल वृक्षों के बीच नाथूराम गोडसे ने गाँधी जी की हत्या के लिए गोलीबारी का अभ्यास किया था।) स्कूल तक पहुँचने के लिए दो मरहलों में सीढ़ियाँ चढ़ती थीं। फिर बरामदे वाले क्लास रूम। शाम होते ही स्कूल कैंप कालिज बन जाता।
साइकिलों पर बदहवास पैडल मारते तीन हज़ार छात्र सप्ताह में छः दिन ठीक समय पर पहुँच जाते। कपड़े कम हों या फटे पुराने. गरमी हो या बरसात या कड़ाके की सर्दी, वे हर मौसम की मार झेलते देर रात घर लौटते क्योकि कोई कोई क्लास रात को ग्यारह बजे ख़त्म होती थी। इन के पास रईसज़ादों जैसे साधन नहीं थे, दिन में होमवर्क करने का समय नहीं था। छोटे घरों में एकांत न मिल पाने के कारण ये लोग वार्षिक परीक्षाओं से पहले एक महीने की छुट्टी ले कर धूप से बचने के लिए पार्कों में पेड़ों के नीचे बैठ साल भर का कोर्स दोहराते थे। सामान्य विद्यार्थियों और इन में एक ज़मीनी अंतर था। यह अंतर इन के पक्ष में था। उन में से अधिकांश के लिए कालिज की शिक्षा विलास की वस्तु थी, मौजमस्ती का आलम थी। इन के लिए यह भविष्य की एकमात्र आस थी। उन में अनुभवहीनता थी, लड़कपन था, इन के पास जीवन का कठोर अनुभव था, मन में उद्देश्यपूर्ण लगन थी, और व्यावहारिक ज्ञान था।
तो इस कैंप कालिज की जिस लड़की को क्वीन मेरी कहे जाने पर ऐतराज़ नहीं था, वह थी सत्या, क्लास की चार पाँच लड़कियों की अकथित नेता, जिसे ख़ाली घंटों में निकट ही बिरला मंदिर के बाहर सहेलियों के साथ चाट पकौड़ी खाने चले जाना पसंद था। …क्वीन मेरी के अंदाज़ पर लट्टू होने वाला शरमीला लड़का था द्रोणवीर कोहली। (इंग्लैंड मेँ ट्यूडर काल की तेज़तर्रार क्वीन मेरी को अंत में सिर गँवाना पड़ा था, और वह ब्लडी मेरी कहलाई थी। एक ब्लडी मेरी और होती है–वोडका, टमाटो प्यूरी, नमक आदि के मिश्रण से बनने वाली नशीली काकटेल।) क्वीन मेरी द्रोणवीर के सर नशीली ब्लडी मेरी बन कर चढ़ गई। मिलना जुलना शुरू हुआ, कभी पब्लिकेशंस डिवीज़न के पास वाली पहाड़ियों पर, कभी कनाट प्लेस, कभी फ़िरोज़ शाह कोटला के उपवनित खंडहर… फिर एक दिन दोनों जीवन साथी बन गए। तब से अब तक वे निष्ठापूर्ण साथ निभाते आ रहे हैं।
बीज अपनी ज़मीन तैयार कर रहा था
१९ जनवरी १९३२ को जन्मे द्रोण नाम के इस लड़के ने रावलपिंडी (पाकिस्तान) से आ कर शाहाबाद जैसे पिछड़े कस्बे से पेट पर पट्टी बाँध कर मैट्रिक की परीक्षा पास की (१९४८)। भटकता भटकता वह अकेला दिल्ली पहुँचा, गली कूचों में मारा मारा फिरता रहा। कई बार सड़क पर सोया। किसी ने सलाह दी टाइपिंग सीखो। परिणामतः द्रोण राजपुर रोड पर ओल्ड सेक्रेटेरिएट में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में क्लर्क-टाइपिस्ट बन गया (१९४९)। कहता है नौकरी भारी सिफ़ारिश से मिली थी, ढंग से टाइप करना भी नहीं आता था। इसी का परिणाम था कि अपने अफ़सर के नाम में ‘जे’ की जगह ‘जी’ टाइप कर बैठा, और ‘नंजानाथ’ को ‘नंगानाथ’ बना दिया। शामत तो आनी ही थी, लेकिन पूरे दफ़्तर में १७ बरस का यह छोकरा जाना पहचाना बन गया। हर तरफ़ अलोकप्रिय ‘नंजानाथ’ के ‘नंगानाथ’ बन जाने का क़िस्सा चटख़ारे ले कर सुनाया जाने लगा।
प्रकाशन विभाग में काम क्या मिला, द्रोण के लिए ज्ञान का द्वार खुल गया। ऐसा नहीं कि उस विभाग में उस जैसे पद पर काम करने वाले सभी के लिए यह दरवाज़ा खुला हो। ये दरवाज़े उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं, जो मन में कुछ साध लिए होते हैं और वर्तमान से संतुष्ट न हो कर भविष्य को सँवारने की जुगाड़ में रहते हैं। द्रोण जैसे क्लर्क और भी थे, वे तो लेखक नहीं बने। आरंभ में द्रोण को अँगरेजी में संपादित पांडुलिपियाँ टाइप करने को भी मिलती थीं। इस प्रकार लिखना सीखने से पहले वह सीख रहा था कि अच्छा लेखन क्या होता है, संपादन क्या होता है। संपादन विभाग में जो विद्वान काम करते थे उन में कई देश विदेश में प्रसिद्ध थे– डा. शशधर सिन्हा, ए. ऐस. रामन, ख़ुशवंत सिंह, भवानी सेन गुप्त, जोश मलीहाबादी, अर्श मलसियानी, जगन्नाथ आज़ाद, देवेंद्र सत्यार्थी, मन्मथ नाथ गुप्त, चंद्रगुप्त विद्यालंकार…
वातावरण में भाषा सौष्ठव था, साहित्य था। यह सब उस के लिए था, जो यह लेना चाहता था। द्रोण ऐसा ही लड़का था जो वह सब बटोर रहा था, जो उसे चाहिए था। वह एक ऐसा बीज था, जो अपने में सृजन ऊर्जा भर रहा था, अपने लिए ज़मीन तैयार कर रहा था, खाद बना रहा था, और सिंचाई भी स्वयं कर रहा था। जीवन भर वह कभी किसी लेखकीय गुट में नहीं रहा, कभी किसी से बिना मतलब पंगा नहीं लिया। अपने काम से काम। सब से विनम्र शिष्ट व्यवहार। कहते हैं आरंभ में पंजाबी में कहें तो झल्लों जैसे आधे गंदे कपड़े सलवार कमीज़ पहनता था। मैं ने उसे जब भी देखा अच्छे कपड़ों में देखा–पूरी तरह प्रैस्ड, साफ़ सुधरे कपड़े। लेकिन मैं ने तर देखा जब सत्या उस का घर चलाने लगी थी।
द्रोण के मन में कल्पनाएँ जागने लगीं, सपने पनपने लगे। वह सौभाग्य समझता है कि दफ्तर की संपादित पांडुलिपियों के साथ साथ उस ने रजिस्टर के पन्नों पर ख़ुशवंत का हाथ से लिखा उपन्यास आई शैल नाट हियर द नाइटिंगेल टाइप किया था। लेकिन उसे यह भी याद है कि एवज़ में उसे थमाया गया था कुल पचास रुपए का चैक, जो उस ने लौटा दिया–इस से कहीं अधिक तो उस ने ख़ुशवंत के घर बसों में आने जाने पर ख़र्च कर दिया था। और ख़ुशवंत ने वह चैक ख़ुशी ख़ुशी वापस ले लिया।
द्रोण को पढ़ने का चस्का लगा। उसे यह भी पता चला कि लिखो तो पारिश्रमिक मिलता है। पैसे की उसे सख़्त जरूरत रहती थी। वहाँ की पत्रिकाओं में छपी कहानियाँ देख कर लगता कि वह भी लिख सकता है। वह कहता है पैसे के लिए झोंक में आ कर उस ने एक कहानी लिख मारी। यह बात पचती नहीं। पैसे कमाने के लिए वह अपने सहकर्मियों की तरह प्राइवेट तौर पर टाइपिंग भी कर सकता था, जैसे कि स्वयं उस ने पैसे दे कर अपनी पहली कहानी हिंदी में टाइप कराई थी। कहानी थी एक नपुंसक पति की जिस की नई नवेली आत्महत्या कर लेती है। और थमा दी बच्चों की पत्रिका बाल भारती की बनीठनी, ख़ुशबुओं से महकती गर्वीली उप संपादिका सावित्री देवी वर्मा को। ज़बरदस्त लताड़ पड़ी, और जाने अनजाने सीख भी कि पहले बच्चों के लिए लिख। दफ़्तर में खिल्ली उड़ी, सो अलग। फिर भी किशोर द्रोण झोंक में कह बैठा, ‘देखना एक दिन मैं इसी पत्रिका का संपादक बनूँगा!’ यह बका पूरी हुई कई साल बाद। इस बीच इलाहाबाद सें निकलने वाली पत्रिका ‘मनमोहन’ के संपादक सत्यव्रत जी ने उस की कहानियाँ छापीं, प्रोत्साहन दिया। उसे उदीयमान लेखक कहा। द्रोण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, और उत्साह दुगुना।
क्लर्क से संपादक तक
कैरियर में बढ़ना हो, तो यह समझ होनी चाहिए कि हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है। सरकारी नौकरी में तरक़्क़ी के लिए केवल ज्ञान काफ़ी नहीं होता–डिगरी भी चाहिए। और तभी खुल गया कैंप कालिज… जो सैकड़ों लड़के लड़कियाँ हर महल्ले में खुले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ कर रत्न भूषण प्रभाकर आदि हिंदी के कोर्स कर के अँगरेजी की परीक्षा में बैठ कर बी.ए. बन रहे थे, या जो ऐस.ऐन. दास गुप्ता जैसे प्राइवेट कालिजों (यानी टीचिंग शापों) में हज़ारों की तादाद में दाख़िल हो रहे थे (प्रसंगवश : निर्मल वर्मा दिल्ली विश्व विद्यालय में पढ़े थे, और करौल बाग़ की एक टीचिंग शाप में कुछ दिन पढ़ाते भी थे), उन्हें बाक़ायदा डिगरी हासिल करने का सुअवसर मिल गया। द्रोण और मुझ जैसे उस पर टूट पड़े। द्रोण मुझ से दो साल दो दिन छोटा है इस लिए (या फिर इस लिए कि हम दोनों के विषय अलग थे) एक कालिज में होते हुए भी हम वहाँ कभी एक दूसरे से नहीं मिले। हालांकि हम दोनों सरिता के दफ़्तर में मिलते थे, जहाँ मैं बाल श्रमिक से धीरे धीरे उप संपादक बन चुका था और वह अपनी रचनाएँ देने के लिए आया करता था।
सरिता के दफ़्तर में द्रोण का आना जाना उस की अपनी सक्रिय जीवंतता का ही परिणाम था। द्रोण कहता है कि रुपए कमाने के लिए (मैं कहूँगा कि मन की ललक पूरा करने के लिए) उस ने जासूसी उपन्यास लिखा–एक हत्या की बदौलत और सरिता कैरेवान पत्रिकाओं के संस्थापक संपादक विश्वनाथ जी के पास भेज दिया। मैं ने जो कुछ भी सीखा वह विश्वनाथ जी से सीखा, और हमेशा उन्हें अपना गुरु माना और अब भी मानता हूँ। उन की ख़ूबी थी कि जहाँ कहीं जिस किसी में संभावनाएँ दिखें उसे प्रोत्साहन दो। उन्हों ने द्रोण का बुलाया। किसी कारण उपन्यास सरिता में नहीं छप सका। छपा मनोहर कहानियाँ में–कोई रायल्टी नहीं। फिर अनधिकृत तरीक़े से वह पेपरबैक में भी आ गया। कोई रायल्टी नहीं। किसी ने द्रोण से कहा मुक़दमा कर दो। मुक़दमा तो अंत में द्रोण ने वापस ले लिया, पर प्रकाशकों के क्षमा माँगने पर।
(प्रसंगवश- सरिता कैरेवान पत्रिकाओं के पन्नों में हिंदी और अँगरेजी के अनेक प्रसिद्ध लेखक पहली बार छपे, एक दो नाम : राजेंद्र यादव, मनोज दास, रस्किन बांड. मोहन राकेश सरिता मेँ नियमित लेखक थे. उन्हों ने सरिता के एक अंक का संपादन भी किया। )
एक और वरदान
१९४९ में जो द्रोण प्रकाशन विभाग में क्लर्क भरती हुआ था, ’५७ में उप संपादक बन गया। कभी वह डाक छाँटता था, डायरी करता था, टाइपिंग करता था, कहाँ उप संपादक बना, फिर सहकारी संपादक, और १९६४ में एक दिन अचानक बाल भारती का संपादक– उन्हीं सावित्री वर्मा के स्थान पर जिन्हों ने कभी उसे लताड़ा था। छह सात साल वह बाल भारती को संवारता सुधारता रहा। संपादक के रूप मे नाम कमाता रहा। आपात्काल वाले दिन वहाँ से तबादला हुआ, सूचना कार्यालय, आकाशवाणी, सैनिक समाचार, फिर आकाश वाणी। चक्कर दर चक्कर तबादले होते रहे। पाँच साल निकल गए। अचानक वह आजकल का संपादक बन गया। बंबई से धर्मवीर भारती ने लिखा, ‘मन करता है कि संपादक के कमरे में आ कर उन्हें बधाई दूँ।’ एक दिन द्रोण की अनुपस्थिति में जैनेंद्र जी उस के दफ़्तर हो कर गए। द्रोण का बढ़ता व्यक्तित्व और महत्त्व सरकारी बाबूगीरी और छुटभैये उच्चस्थ सहकर्मियों की प्रौफ़ैशनल जैलसी में तरह तरह की चालबाज़ियों का केंद्र बन गया। उस ने लिखा है, ‘‘आजकल में मेरी स्थिति उस बिलाव जैसी थी जो अचानक टीन की तपती छत पर कूद पड़ा हो।’’ आजकल में वह बस एक साल ही रह पाया। फिर तबादले होने लगे... गर्दिश के तीन साल कभी वह आकाशवाणी, कभी पत्र सूचना कार्यालय. दृश्य श्रव्य निदेशालय, रक्षा मंत्रालय की ख़ाक़ छानता रहा… तीन साल उसे सैनिक समाचार जैसे सड़ियल अख़बार के अँगरेजी संस्करण में बिताने पड़े, जो कभी कभी तीन महीनों तक नहीं निकलता था, और आर्थिक भ्रष्टाचार का अड्डा था। तंग आ कर १९८५ में द्रोण ने स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर लिया।
एक और वरदान
यह एक और वरदान सिद्ध हुआ। दफ़्तर की उठापटक से दूर रचनात्मक काम का कपाट धड़ाके से पूरा खुल गया। अब शुरू हुआ देर से फल देने वाले कल्पवृक्ष का उपजाऊ काल।
सन १९८० में उस का पहला महत्त्वपूर्ण और मेरी तरह बहुत लोगों की पसंद का उपन्यास हवेलियों वाले आ चुका था, जिस ने सब को चौंका दिया। चौंकना स्वाभाविक था। साहित्य जगत में अब तक द्रोण की छवि साधारण प्रतिभा के लेखक की थी। लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था कि कुछ बीज होते हैं जो मौसमी फल देते हैं, जिन की कहानी बस दो तीन महीनों की होती है। कुछ बीज ऐसे पेड़ बनते हैं, जो साल दो साल में फल देते हैं, और कुछ बीज पहली फ़सल देने के लिए कई लंबे साल लगाते हैं। द्रोण नाम के बीज ने अपने को पचासादि दशक में बनाया और बोया, सन १९५७ से उस में कच्चे फल आए, बालोपयोगी किताबें आनी शुरू हुई, पर असली फल शुरू हुए १९८० में हवेलियों वाले से।
साहित्य जगत को जो बात तब तक नज़र नहीं आई थी, वह थी द्रोण का पत्रपत्रिकाओं में निरंतर लेखन, विशेषकर धर्मयुग में। अंधायुग के लेखक और धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती आसानी से कोई लेखक नहीं पकड़ते थे। पूरी तरह आश्वस्त हो कर ही वे किसी को धर्मयुग के पन्नों पर छापते थे। उन्हों ने द्रोण से असंख्य रिपोर्ताज लिखवाए, जो लोकप्रिय हुए। वहीं द्रोण ने बुनियाद अली उपनाम से बेदिल दिल्ली स्तंभ लिखा। रिपोर्ताज ऐसी विधा है जिस के लिए लेखक को नज़र पैनी करनी होती, आँखों देखी सामयिक घटनाओं के पीछे छिपे स्थायी सत्य तलाशने होते हैं। तब धर्मयुग में सहायक संपादक कन्हैया लाल नंदन को आशंका हुई थी कि द्रोण कहीं कोरा पत्रकार बन कर न रह जाए। उन्हीं दिनों द्रोण ने मेरे कहने पर माधुरी के लिए फ़िल्मों पर भी लिखा।
मधुर याद भाषा तेरी
द्रोण जो कुछ लिखता है बड़ी मेहनत से, कई बार बरसों मन मार कर साधना करता हुआ लिखता है। बार बार लिखता है, दोहराता है। हवेलियों वाले से पहले उस का बालोपयोगी उपन्यास टप्पर गाडी १९७९ में आया था। अनोखी पृष्ठभूमि। सिकंदर के आक्रमणों के काल में तक्षशिला की चरमराती व्यवस्था में गाँव से टप्पर गाड़ी पर आया एक परिवार जिसे बड़े शहर में बच्चे का इलाज कराना है। संकटों से जुझता परिवार अंततः लौट जाता है। इस ने द्रोण का सिक्का जमवा दिया था। सोलह साल में ९ रिवीज़न करने के बाद ही टप्पर गाड़ी छपा था। स्पष्ट है कि पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही द्रोण कोई किताब पाठक तक पहुँचने देता है। अगर वह मात्र पैसों के लिए लिख रहा होता, तो पहला ही ड्राफ़्ट किसी मेरठिया प्रकाशक को पकड़ा देता, जो किताब को किलो के भाव से विक्रेताओं को सप्लाई करता। यदि आप इस लेख के साथ छपी द्रोण की रचनावली देखें तो पाएँगे कि अकसर कोई उपन्यास लिखने में उसे चार साल लगते हैं। ये चार साल मन में उस उथलपुथल से भरे होते हैं जो किसी सजग लेखक के मन में लगातार होती है, उस संघर्ष के होते हैं जो मन में उभरी तस्वीरों और दृश्यों को शब्दों के माध्यम से काग़ज़ पर उतारते बीतते हैं।
मैं अपने को साहित्य समालोचकों की श्रेणी में रखने की हिमाक़त नहीं करता। मेरा अपना पढ़ा लिखा बेहद कम है। जो है उसे साहित्य कह पाना कठिन है। हाँ, अपनी पसंद के दो चार द्रोण उपन्यासों के बारे में कुछ बताने की आधी अधूरी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ–सिर्फ़ उस की क़लम की विविधता दरशाने के लिए।
प्रतीकात्मक पात्र नामों वाले उपन्यास काया स्पर्श में द्रोण ने मनोविज्ञान पर अपनी गहरी पकड़ का सबूत दिया है। ऐसे विषय पर हिंदी में इतना सूक्ष्म लिखा गया यह एकमात्र उपन्यास है। अपार धन के मालिक हृदय सुगति के मनोक्षीण बेटे इक्षवाकु (घर पर ‘इच्छु’ के नाम से ज्ञात) और मनोचिकित्सिका काया के संबंधों की यह गाथा अपनी तरह की पहली, और अब तक शायद एकमात्र, रचना है।
हवेलियों वाले में रावलपिंडी के निकट के गाँव थोबा मार्हम ख़ाँ के एक परिवार की कहानी है–संयुक्त परिवार में रहने वालों के परस्पर संबंधों का वर्णन जो देखा जाए तो मानव मात्र के आपसी संबंधों का ब्योरा है। पर कुछ ऐसा भी हो जो केवल मार्हम ख़ाँ में ही घट सकता था। टप्पर गाड़ी से ले कर बरास्ते हवेलियों वाले द्रोण का ८० प्रतिशत साहित्य विभाजन से त्रस्त पंजाबी मानस का प्रतीक है। देश का बँटवारा इस संघर्षशील समाज को गहरे तक आहत कर गया था। यह टीस पीढ़ियाँ बीत जाने पर भी कम नहीं हुई है। लेखक चाहे भीष्म साहनी हों या कोई अन्य समकालीन पंजाबी, वह अविभाजित पंजाब को नहीं भूल पाया। जो तमस है, तमस के पीछे की भावभूमि है, वह मंटो में है, कृशनचंदर में है, यशपाल में है… कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान किसी पंजाबी का विभाजन पर लिखा उपन्यास कभी नहीं हो सकता था। कितने पाकिस्तान में एक अ-पंजाबी द्वारा भारत के विभाजन पर प्रतिक्रिया है, वह भी एक सुररीयलिस्टिक अंदाज़ में। इसी लिए द्रोण के वाह कैंप को कमलेश्वर ‘महत्त्वपूर्ण, रचनात्मक और यातनाप्रद’ पाते हैं।
विभाजन से अब तक साठ साल की दूरी ने द्रोण के पुराने पैतृक जीवन स्थल पर दूर के ढोल की तरह सुहानेपन का मुलम्मा चढ़ा दिया है। रचना का विषय कोई परिवार हो या क्षेत्र, उस पर अलगाव की त्रासदी और जड़ों के प्रति मोह छाया रहता है। कुछ आलोचकों ने कहा है कि आंगन कोठा हिंदी का आंचलिक युग समाप्त होने के काफ़ी बाद आया। सही है कि विभाजन संबंधी सभी रचनाएँ एक तरह से आंचलिक हैं। पर वे आंचलिक कम, अपनी और अपनेपन की तलाश ज़्यादा हैं। तकसीम में परिवार बँटता है तो वाह कैंप में देश। इन में आंचलिकता के जिस पुट की बात की जाती है उस का संबंध भाषा से है, शब्दावली से है। लेखक अपने बचपन में सुनी भाषा को मोह ममता से याद करता है। द्रोण की उपन्यास शृंखला में पुरानी मिट्टी की गंध है और भूली बिसरी सी मातृभाषा की सुमधुर स्मृति है।
नानी एक अलग तरह की आधुनिक रचना है। तरह तरह के पेशवर हिंदुस्तानी डाक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ दुनिया भर में बसे हैं। जब कभी उन्हें माँ बाप बनना होता है तो याद आते हैं अपने माँ बाप, और उन्हें बुला लिया जाता है विदेश, जहाँ माँ बाप एक तरह से फ़ाइव स्टार जेल में क़ैद हो जाते हैं। मैं ने स्वयं अमरीकी नगर डैलस में अनेक बूढ़ों को देखा है जो सुबह की सैर पर मिलने पर एक दूसरे से पूछते हैं कौन सेवें बच्चे की डिलीवरी पर आना हुआ? वहां के तेज़ रफ़्तार ट्रैफ़िक में वे न तो घर से निकल सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। दिन भर एअरकंडीशंड कमरों में क़ैद रहते है। इस विषय पर बहुत ही कम लिखा गया है। यह द्रोण का ही बूता था कि अपनी विदेश यात्राओं में देखे गए सच को बेहद मार्मिक और रोचक उपन्यास की शकल दे पाए। द्रोण के रचना संसार का असली आकलन तो आने वाले के बाद भी आने वाला युग सही तरह कर पाएगा, मुझ जैसे लोग तो केवल अपनी मुग्धता का ही बयान कर सकते हैं।
ब्लडी मेरी बन गई जीवन का रस
भाई महीप ने मुझे द्रोणवीर की जीवन संध्या के बारे में लिखने को कहा था। द्रोण का जीवन प्रभात दिखाए बग़ैर, और जीवन में कोई जगह बनाने के संघर्ष के वर्णन के अभाव में द्रोण की जीवन संध्या के बारे में लिखना मेरे लिए संभव नहीं था…
उस लड़के पर जो लड़की ब्लडी मेरी बन कर चढ़ी थी, आज आधी सदी बीत जाने पर वह जीवन का सुखद रस बन चुकी है। अभी तक वे एक दूसरे में रमे हैं। लेखकों वाला वह ऐब द्रोण में कभी नहीं आया जो उन्हें लगातार एक से अधिक प्रेमिकाएँ रखने को उकसाता है। मैं जानता हूँ कि द्रोण और सत्या एक दूसरे के लिए बने है। अब भी एक दूसरे पर फ़िदा हैं, और छोटी मोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते सुखी पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं, जैसा कि अकसर दंपतियों के बीच होता है। सत्या का कहना है, ‘वह दांपत्य ही क्या जिस में रोज़ हर किसी छोटी मोटी बात पर झगड़े ना हों।’
सत्या द्रोण के बारे में बहुत कुछ बता सकती है… लेकिन उस की शिकायतें बस ऐसी हैं… द्रोण घर का कोई काम नहीं करता… हद से हद किया तो बहुत कहने पर कोई स्विच आफ़ कर देना, और फिर कहना मैं ने अपना आज का काम कर दिया है, इस के बाद कुछ और काम मत बता देना… और सत्या जो प्रेमिका थी, पत्नी बनी, सरकारी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर हो कर, अब पूरे दिन घर में रहने वाली पूरी माँ बन चुकी है। बिल्कुल वैसे जैसे गाँधी जी ने कहा था कि पत्नी बुढ़ापे में माँ बन जाती है। सुबह से शाम उस का समय मदरिंग में बीतता है। वह द्रोण का ख़्याल उसी तरह रखती है जैसे बेटे दक्षवीर (ऋषि) का। हर समय उन के सुख, उन की सुविधा का ध्यान रखना, खाना खिलाने के लिए पीछे पड़े रहना। सुबह तुलसी के पत्ते देगी, नीबू का पानी देगी, चाय देगी, भीगे बादाम देगी… द्रोण और दक्षवीर टालते रहते हैं। और हार कर झुक जाते हैं… बेटी मुद्रा और दामाद राकेश अमरीका में डाक्टरी करते हैं। उन की चिंता, उन से टेलिफ़ोन पर बात न हो जाए तो परेशानी। जब कभी वे दिल्ली (आजकल गुड़गाँव) आएँ, तो वही दक्षवीर और द्रोण की तरह उन के सुख, उन की सुविधा की सतत चिंता…
जहाँ तक द्रोण का सवाल है इसे जीवन संध्या कहा जाए या जीवन का चरम विकास यह कहना कठिन है। सच कहूँ तो उस का चरम विकास अभी होना है। द्रोण जैसे देर से फल देने वाले खजूर के पेड़ की जवानी ही तब शुरू होती है दूसरे पेड़ बूढ़े हो चुके होते हैं, या दुनिया से कूच कर चुके होते हैं। अभी तो फल आने शुरू हुए हैं। द्रोण को अभी और फल देने हैं। कई उपन्यास उस के मन में भरे हैं। समय आने पर वे पेड़ पर लगेंगे ही।
द्रोण को यम के आने का डर नहीं सताता, यह चिंता सताती है कि जो अभी अनलिखा है वह अनलिखा न रह जाए, और कहीं शरीर और मस्तिष्क वह सब लिख पाने से पहले दग़ा न दे जाएँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा इस लिए नहीं होगा कि मानसिक जिजीविषा तन मन को दुरुस्त रखती है….
अंत में थोहा मार्हम ख़ाँ के श्री हरनाम दास और श्रीमती वीराँवाली को धन्यवाद देता हूँ कि उन्हों ने हमें द्रोण दिया।
❉❉❉
आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ
©अरविंद कुमार
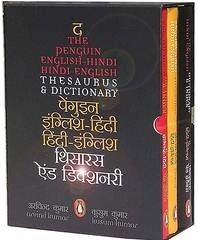
Comments