मेरठ मेँ मेरा बचपन
बिजली के झटकोँ से पूरा शरीर फड़फड़ा रहा था. तभी किसी ने करंट आफ़ कर दिया. लेकिन मैँ बेहोश था. कई दिन रात तक मैँ जागते सोते दहलता रहा. पिताजी से कहता बिजली होती ही क्योँ है. आज तक मेरी उस उँगली में इस घटना का निशान है.
मेरठ मशहूर है सन १८५७ के ग़दर के लिए, मय राक्षस की राजधानी, मंदोदरी का जन्मस्थान और रावण की ससुराल होने के लिए, नौचंदी मेले के लिए, ख़स्ता रेवड़ी ग़ज़क के लिए, हलवा पूरी, चाट पकौड़ी के लिए. हम मेरठ वाले कहीँ भी चले जाएँ मेरठ को, नौचंदी को और चाट पकौड़ी को नहीँ भूल पाते.
मेरा जन्म वहाँ शकट चौथ (जिसे हम लोग संकट चौथ कहते थे) पर १७ जनवरी १९३० को हुआ, और पहले १२-१४ साल वहीँ बीते. फिर हम दिल्ली चले आए. पर सारे रिश्तेदार वहीँ थे. हर साल कई बार वहाँ जाना होता था–कभी शादी ब्याह के लिए, कभी यूँ ही, और जब कभी भी मौक़ा मिले, होली के दो सप्ताह बाद होने वाले नौचंदी मेले के लिए. लाला का बाज़ार महल्ले मेँ हमारा घर था. कई साल शहर मेँ बिजली नहीँ थी. रात को सड़कोँ पर मंदी लालटेनेँ जलती थीँ. उन से अँधेरा मिटता नहीँ था. औरतेँ कहती थीँ– साँझ पड़े, मर्द मानस घर भले. सुबह खाना खा कर लोग घर से निकलते, लगभग पाँच बजे तक घर आ जाते. आते ही खाना खा लेते. फिर पिताजी शाम की सैर के लिए निकलते. मुझे भी साथ ले जाते. थोड़ी ही दूर घंटाघर था. लाल ईँटोँ पर लाल पुताई वाला. उस मेँ नीचे तीन बड़े बड़े फाटक हैँ. दूसरी मंज़िल के ऊपर ऊँ�ची चौकोर बुरजी पर चारोँ तरफ़ एक एक घंटा था, जो दूर से दिखाई देता था. हर चौथाई, आधे, पौने और पूरे घंटे पर टनटन बजता था. बच्चे गाते थे –
घंटाघर मेँ चार घडी, चारोँ मेँ ज़ंजीर पड़ी,
जब घंटाघर बजता है, खड़ा मुसाफ़िर हँसता है.
1 आजकल घंटाघर मेँ घड़ी नहीँ
घंटाघर से निकलते ही टाउन हाल था, पार्क था, लाइब्रेरी थी. क्यारियोँ की सिँचाई के लिए छोटी छोटी पक्की गहरी नालियोँ जैसी नहरोँ मेँ पानी का चलना मुझे बहुत अच्छा लगता था. लाइब्रेरी मेँ पिताजी अख़बार और मैँ बच्चोँ की कोई किताब पढ़ता. बचपन से ही पिताजी ने मुझे किताबोँ का शौक़ लगा दिया था. नौचंदी के मेले मेँ भी मैँ किताबेँ ज़रूर ख़रीदता था. उन दिनोँ मेरठ से बच्चोँ की पत्रिका शिशु (?) निकलती थी. एक भूगोल अध्यापक अनियमित पत्रिका देशदर्शन निकालते थे. मैँ वे दोनोँ पढ़ता था. अध्यापक जी साल भर बचत कर के सस्ते मेँ किसी न किसी देश जाते. यात्रा विवरण और जानकारी से भरपूर सामग्री सहज भाषा मेँ छापते थे. मुझे उस का एक अंक अभी तक याद है — यह अफ़गानिस्तान पर था.
❉
गरमियोँ मेँ साढ़े छः सात बजे तक हम लोग लौट आते. अब सुबह होने तक घर ही हमारा जीवन था. मिला जुला परिवार था–बाबा, दादी, अविवाहित बुआ चाचा सभी थे. उसी मकान मेँ हमारे मँझले बाबा सपरिवार रहते थे. पतली सी गली मेँ सामने वाला मकान हमारे छोटे बाबा का था. दीयाबाती के बाद सब लोग साथ बैठ कर बातेँ करते. बड़ी बूढियाँ क़िस्से कहानियाँ सुनातीँ. सदर वाली बुआ जब कभी रहने आतीँ तो श्याम जी की कहानियाँ सुनातीँ. कहीँ किसी पर कोई संकट हो, जैसे द्रौपदी का चीर हरण या फिर कोई बच्चा जंगल मेँ भटक जाए, तो श्याम जी को पुकारा जाता था. श्याम जी तुरंत आ कर रक्षा करते थे.
घर मेँ धार्मिक वातावरण था. ताऊजी, पिताजी और दोनोँ चाचा आर्य समाजी थे. लेकिन बाक़ी लोग सनातनी थे, देवी देवताओँ को मानते थे, कथा कीर्तन करते कराते और जाते रहते थे. कुछ भजनोँ मेँ भगवान कृष्ण से प्रार्थना की जाती थी दीनदुखी आरत भारत माता को अँगरेजोँ के जुलुम से उबारेँ. हमारी गली का नाम था क़ानूनगोयान स्ट्रीट. सामने वाली गली थी छत्ता. उस के नुक्कड़ वाले चबूतरे पर कुआँ था, पीपल का बड़ा पेड़, और शिव मंदिर. गली मेँ हर साल रामचरितमानस का पाठ होता था. कथा आरंभ करने से पहले पंडित जी हनुमान जी को बुलाते और अंत मेँ भेजते. वह कहते थे कि रामकथा मेँ हनुमान सब से पहले आते हैँ, और सब के बाद जाते हैँ. भला मैँ उन से पीछे क्यों रहता! कथा शुरू होने से बहुत पहले पहुँचता, दरियाँ बिछवाता और सब के बाद वहाँ से चलता.
घर मेँ कभी सत्ता (सात दिन का भागवत पाठ) होता था, कभी सुखसागर, कभी सत्यनारायण की कथा. अम्माँ को कीर्तन कराने का बड़ा शौक था. कीर्तनोँ मेँ जाती भी थीँ. मैँ भी साथ जाता. ज़ोर ज़ोर से भजन गाता. उन्होँ ने पिताजी के प्रैस मेँ भजनोँ की छोटी सी किताब छपवाई थी. नाम था प्रेम मेँ भगवान. मूल्य था केवल प्रेम. काफ़ी बाद तक सोलह पन्नोँ की वह पुस्तक मेरे पास थी.
❉
हमारे खेल थे स्कूल के मैदान मेँ कबड्डी, हाकी और फ़ुटबाल, अखाड़े मेँ कसरत और कुश्ती, गली मेँ गिल्ली डंडा और गेँद पिट्ठू, छत पर पतंगबाज़ी और कबूतरबाज़ी. कभी कभी सड़क पर तीतर और मुर्गे की लड़ाई देखने को मिलती थी.
तीजत्योहार बड़े जोश से मनाए जाते थे. कभी होली, कभी दीवाली, कभी गणेश पूजा, कभी अनंत चौदस, कभी दशहरा, राखी… तीजोँ पर झूले पड़ते थे. बारहमासी गीत गाए जाते थे. अहोई पर अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाया जाता था. साँझी पर लड़कियाँ साँझी रखती थीँ–मतलब गोबर और मिट्टी से साँझी के चित्र बनातीँ, शाम को गीत गा कर आरती उतारतीँ. टेसू पर बच्चोँ को बड़ा मज़ा आता था. शाम को टेसू बना कर, उस की गोदी मेँ दीया जला कर निकलते, घर घर जाते, गाते, मेरा टेसू यहीँ अड़ा, खाने को माँगे दही बड़ा! जब तक कुछ मिल न जाता आगे नहीँ बढ़ते थे. गीत मेँ मेरठ से दिल्ली का रास्ता बताया जाता था. रास्ते मेँ जमना का पुल भी आता था.
जन्माष्टमी पर पहले दिन आधी रात तक निर्जल उपवास रखते थे, दूसरे दिन फूलडोल (झाँकी) सजाए जाते. बच्चे और जवान तरह तरह की सजावट और दृश्य बनाने मेँ जुट जाते. रात को सब लोग निकलते घर घर के फूलडोल देखते, पसंद नापसंद की टिप्पणी करते. मुझे अभी तक याद है. एक फूलडोल की भयानक घटना.
मैँ कोई सात आठ साल का रहा होऊँगा. शायद कुछ ज़्यादा का भी. तब कुछ घरोँ मेँ बिजली आ चकी थी. इधर उधर घूमता मैँ देख रहा था. बड़े बच्चे तरह तरह के खिलौने और माटी की मूरतेँ पेड़ पौधे हरियाली आदि लगा सजा रहे थे. बाद मेँ वहाँ रोशनी करने करने लिए बल्ब लगाने के लिए बिजली के साकेटोँ वाली झालर टँकी थी. बल्ब अभी लगाए नहीँ गए थे. उन का ख्याल था कि अभी करंट का स्विच आन नहीँ किया गया है. पर यह क्या? मेरे बाएँ हाथ की पहली उँगली जाने कैसे एक साकेट मेँ चली गई—और जो हुआ वह अभी तक मुझे दहला देता है. मुझे बिजली ने पकड़ लिया था. उन दिनोँ डीसी करंट हुआ करता था. यह करंट अपनी तरफ़ खीँचता है. मेरे शरीर के साथ पूरी लड़ी खिँचती चली आई. बिजली के झटकोँ से पूरा शरीर फड़फड़ा रहा था. तभी किसी ने करंट आफ़ कर दिया. लेकिन मैँ बेहोश था. कई दिन रात तक मैँ जागते सोते दहलता रहा. पिताजी से कहता बिजली होती ही क्योँ है. आज तक मेरी उस उँगली में इस घटना का निशान है.
दशहरे के दिन बड़े मज़े के होते थे. रामलीला होती. हम धनुषबाण ख़रीदते, रामचंदर जी की तरह धोती पहन कर तीर चलाते, राक्षसोँ को मार गिराते. शाम को रामलीला की सवारी निकलती. भक्त जन रथ रुकवा कर आरती करते, रामचंदर जी, सीता जी और लक्ष्मण को चढ़ावा चढ़ाते. शहर मेँ तरह तरह की सवारियाँ अकसर निकलती रहती थीँ. छोटे बाबा की बाल्कनी दर्शकोँ से खचाखच भर जाती. मुहर्रम पर शीया अपना शरीर लहूलुहान करते निकलते थे. कभी हज़रत मुहम्मद के दुलदुल घोड़े की सवारी निकलती थी. हम बड़े शौक़ से सभी को देखते थे. दीवाली पर अपने अपने घर दीए जला कर, सब निकल पड़ते नगर की शोभा देखने.
वसंत पंचमी पर सब पीले कपड़े पहनते. घर मेँ पीले चावल या ताहिरी बनाई जाती. उसी के आसपास फुलेरा दोज होती थी. छोटी लड़कियाँ वनकन्या बन कर डोली मेँ फूल सजातीँ, घर घर बाँटती. ज़िद कर के मैँ भी वैसे ही कपड़े पहन कर साथ लग लेता था.
होली की धूम कई सप्ताह पहले शुरू हो जाती थी. आलू से ठप्पे बना कर राह चलतोँ की पीठ पर छापे ठापने मेँ हमेँ बड़ा मज़ा आता था. किसी ठप्पे पर लिखा होता उल्लू, किसी पर गधा या पागल. सड़कोँ पर लोग पहली मंज़िल से काँटे वाली डोरी डाले रहते. कोई बेख़बर गुज़रता तो नीचे छिपा खड़ा साथी उस की टोपी मेँ काँटा फँसा देता, ऊपर वाले टोपी खीँच लेते. रंग अबीर की मत पूछो! कई दिन पहले से टेसू (पलाश) के सूखे फूल ख़रीद कर रख लिए जाते थे. रात रात भर उबाल कर फिर हलका सा चूना डाल कर बड़ा बढ़िया केसरिया रंग निखारा जाता था. पिचकारियोँ मेँ वही भरा जाता था. आजकल जैसे सस्ते रासायनिक रंग उन दिनोँ नहीँ चलते थे.
होली का पहला दिन दामादों का होता था. जीजा साले, सालियाँ सलहज इस दिन अपने अरमान निकालते. फिर साल भर याद करते कैसे जीजा जी को रंग से सराबोर किया. आजकल बड़े शहरोँ मेँ होली शाम को ही जला दी जाती है. तब मुहूरत होने पर ही होलिका दहन होता था. मुहूरत कभी रात के बारह बजे या और भी देर से हो सकता था. ख़ास बात यह थी कि सब लोग लंबे बाँसोँ के अगले सिरे पर जौ की ताज़ा बालियाँ बाँध कर होली की लपटोँ पर भूनते थे. यह नई फ़सल की अग्निपरीक्षा होती थी. घर लौट कर सभी रिश्तेदारोँ पड़ोसियोँ के घर जा कर अपने भुने दाने दिखाते थे, उन के देखते थे. माथोँ पर गुलाल मलते थे.
दुलहँडी पूरे शहर के लिए होती थी. होली के भड़ुए और हुड़दंगे नाचगाना करते. कोई एक विलायती साहब बन जाता–सिर पर टूटाफूटा टोप, हाथ मेँ छड़ी, कमर पर फटके से बाँधी ढीलीढाली पतलून! सब उस विलायती जैंटलमैन के इस भदरूप का मखौल उड़ाते, छड़ी से पीटते, फटकारते. दोपहर होते ही रंग का खेल ख़त्म हो जाता. नाचरंग का स्तर बदल जाता. सब से लोकप्रिय नाच था गाँव वालोँ का काग़ज़ के घोड़े पहन कर स्त्री पुरुष दंपति का नाच. स्त्री का भेष भी पुरुष ही धरते थे. यह नाच एक तरह से पुराने किन्नरोँ का नाच होता था.
दुलहँडी से अगला दिन बसोड़ा कहलाता था. घर की मालकिन (हमारे घर मेँ मेरी माँ) भंगी की पूजा करती थीँ. (आजकल के बच्चे नहीँ जानते कि उन दिनोँ फ़्लश वाले टायलेट नहीँ होते थे. खुड्डियोँ वाला पाख़ाना बाहर वाले हिस्से मेँ या घुसते ही कोने मेँ बनाया जाता था. हर दिन दोहपर मेँ भंगी भंगिन पाख़ाना कमाने यानी साफ़ करने आते थे, मैले की टोकरी सिर पर रख कर ले जाते थे.) भंगी बसोड़े पर मुरग़ा ले कर आता था. मुरग़े की भी पूजा की जाती थी. पूजा के बाद भंगी को उपहार दिए जाते थे, साथ ही होली का बचाखुचा बासी खाना. बासी शब्द से ही बसोड़ा शब्द बना होगा.
हमारे भंगी का नाम कीड़ी था. शकल अजीब सी थी, गाल पिचके हुए, पतला दुबला, हँसमुख. वह घर के सदस्य ही की तरह था. घर की कोई बात उस से छिपी न रहती थी. लेकिन न वह हमेँ न हम उसे छू सकते थे. कभी भिड़ गए तो सोने की अँगूठी से चुल्लू भर पानी छू कर अपने पर छिड़क कर हम पवित्र हो जाते थे. आजकल अछूत प्रथा का उन्मूलन हो गया है. कीड़ी मेरे कई काम आता था. मुझे बार बार दस्त लग जाते थे. माना जाता था कि मेरी ढूडी उतर गई है—गुदा के ऊपर की हड्डी. कीड़ी ढूडी ठीक करने मेँ दक्ष था. मुझे औँधा लेटा दिया जाता. कीड़ी पैर की एड़ी से उस हड्डी को ज़ोर से दबाता. सच मानिए—दस्त बंद हो जाते थे. बाद मेँ यह कला मेरी माँ ने कीड़ी से सीख ली. दस्त एक अन्य कारण से भी होते माने जाते थे. नाभि को नाफ़ कहते थे. कई बार बोझ उठाओ तो नाफ़ उतर जाती थी. और दस्त शुरू! नाफ़ ठीक करने के लिए पीठ के बल लेटते थे, और कोई अन्य व्यक्ति खाट के पाए जैसा कोई डंडा वहाँ ख़ास तरह से दबाता था. नाफ़ ठीक हो जाती थी. नाफ़ बार बार न उतरे इस लिए पैर के अँगूठे मेँ काला धागा बाँधा जाता था. ऐसा माना जाता था कि यह धागा बाँध लेने पर नाफञ नहीँ उतरती. इन का असर भी होता था. कम से कम मुझे तो अभी तक यही लगता है.
❉
होली से दूसरे शनिवार को नौचंदी शुरू होती थी. बच्चोँ और औरतोँ के लिए वह बड़ा आकर्षण थी. उन दिनोँ औरतेँ ख़रीदारी के लिए घर से नहीँ निकलती थीँ. सागसब्जी घर के मर्द लाते थे. बजाज फेरी पर सिर पर कपड़े लाद कर आते थे. बादाम, अखरोट किशमिश आदि बेचने काबुलीवाला घर पर आता था. (आप ने नोबल पुरस्कार विजेता रवींद्र नाथ ठाकुर की कहानी काबुलीवाला पढ़ी है क्या? या उस पर बनी फ़िल्म देखी है? नहीँ तो ज़रूर पढ़िएगा, और फ़िल्म देखना भी ना भूलिए. सिनेमाघर मेँ तो नहीँ मिलेगी, लेकिन पुरानी फ़िल्मेँ टीवी पर आती हैँ या उन की सीडी या डीवीडी मिल जाती है.) मनिहार चूड़ियाँ पहनाने घर आते…
हाँ, नौचंदी पर औरतेँ मेला देखने निकलती थीँ, बड़े शौक़ से, खूब सजधज कर. साल भर की ख़रीदारी वहीँ करती थीँ. मेला रात भर चलता, सुबह बंद होता था. दोपहर को गाँव के लोग आते थे. शहर के मध्यमवर्गीय लोग खा पी कर, रात को नौ दस बजे आराम से टहलते निकलते थे. खेल तमाशे, ज़िंदा नाचगाने, कवि सम्मेलन, मुशायरा… चलते फिरते सिनेमाघर… सरकस.. मौत का कुआँ… हम सब के लिए वह साल द रखने वाला अनुभव होता था. ख़ूब मज़ा आता. हर मेरठ वाला कोशिश करता है कि नौचंदी पर मेरठ जाए… पचहत्तर साल से ज़्यादा का हो जाने पर भी मैँ वहाँ जाना चाहता हूँ. लेकिन पहले बंबई, बाद मेँ बंगलौर, चेन्नई और पौंडीचेरी मेँ रहने के कारण ऐसा हो नहीँ पाता था. अब गाज़ियाबाद मेँ हमारे घर से नौचंदी मैदान कोई 55 किलोमीटर दूर ही है.
❉
कुछ दिन पहले मैँ मेरठ गया था. घंटाघर देखने भी गया. सारे इलाक़े की हालत बदली थी. बेरौनक़ टाउन हाल. पार्क मेँ अजीब सी भीड़भाड़ थी. यही हाल बाज़ार का था. पहले यह खुला खुला था, हर तरफ़ मुन्नालाल साबुन की दुकानें थीँ, सोडावाटर की एक मशीन थी. अब भीड़भाड़ और घंटाघर की घड़ियाँ टूटी फूटी थीँ. मेरे मन मेँ पुराना गीत नहीँ गूँजा. मन से दुखभरी आवाज़ निकली
घंटाघर मेँ घड़ी नहीँ, चारोँ मेँ ज़जीर नहीँ
अब घंटाघर बजता नहीँ, खड़ा मुसाफिर हँसता नहीँ.
नगरपालिकाएँ पता नहीँ क्यों पुरानी इमारतोँ की देखभाल नहीँ करतीँ?
❉❉❉
आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ
और अपने परिचितोँ को भी बताएँ.
©अरविंद कुमार
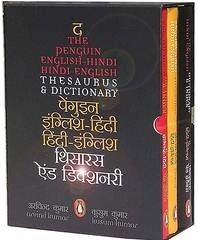


Comments