एक प्रस्तुति मन में – तीन प्रस्तुतियाँ मंच पर…
–अरविंद कुमार
सितंबर १९९२ में मैं ने जब श्री रामगोपाल बजाज निर्देशित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों द्वारा अंधा युग की प्रस्तुति देखी तो अभिभूत हो कर डाक्टर धर्मवीर भारती को एक पत्र लिखा, जिस में उस का विभोर वर्णन किया. उस पत्र में मैं ने मेरी देखी पिछली कुछ प्रस्तुतियों का ज़िक्र भी किया था. तब भारती जी ने मुझे एक पत्र लिखा. वह चाहते थे कि मैं उन सब प्रस्तुतियों की विशिष्ठताओं को एक लेख में वर्णित करूँ. मुझे वह सब लिखने में काफ़ी समय लगा. ३ फ़रवरी १९९३ को मैं ने निम्न लेख उन्हें भेजा. भारती जी की अस्वस्थता के कारण वह उन के पास कहीं रखा रह गया. अब जब पुष्पा जी उन के पुराने काग़ज़ तलाश रही थीं, तो उन्हें यह लेख भी मिला. इस की टाइप प्रति में कई जगह मैं ने काट छाँट कर रखी थी. वह चाहती थीं कि मैं इसे कंप्यूटर पर फिर से लिख दूँ. बिना किसी परिवर्तन के यह लेख अब भारती जी की स्मृति को अर्पित है. जैसा कि मैं ने अपने पत्र में १९९२ में उन्हें लिखा भी था – यह मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे उन जैसे महान रचनाकार को निकट से जानने का अवसर मिला.
मेरे अपने अज्ञान के कारण अंधा युग से मेरा पहला संपर्क कुछ देर से हुआ, लेकिन मेरे मन पर वह एक अमिट छाप छोड़ गया.
सन १९५९ में भारती जी के धर्मयुग का संपादक बनने की ख़बर नई दिल्ली पहुँची तो अकसर शामों को बैठने के हमारे अड्डे टी हाउस में तहलक़ा मच गया. सब की ज़बान पर एक ही नाम था. धर्मवीर भारती. सब के सब ऐसे बातें कर रहे थे कि वे भारती जी को और उन के कृतित्व को बड़ी नज़दीकी से जानते हों. और कुछ वाक़ई थे जिन के बारे में यह सच था. एक मैं था जो अपने आप को लगभग अजनबी और अँधेरे में पा रहा था.
हर धंधे की तरह पत्रकारों और साहित्यकारों के भी अपने रागद्वेष होते हैं. मैं पत्रकार ज़रूर था, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला. आपसी रागद्वेष से दूर. सक्रिय और नियमित लेखक मैं न तब था, न अब हूँ. अपने थोड़े बहुत लिखे को साहित्य मानने की धृष्ठता मैं ने कभी नहीं की. इसलिए किसी साहित्यकार को मैं और कोई साहित्यकार मुझे प्रतिद्वंद्वी नज़र नहीं आया. हाँ, सुरुचिपूर्ण पाठक मैं अपने आप को तब भी मानता था. पाठक को लेखकों के आपसी द्वेषों से कोई सरोकार नहीं होता.
मैं पाठक तब भी था, और अब भी हूँ. लेकिन निजी व्यस्तताओं के कारण समकालीन साहित्य से सजग संपर्क नहीं रख पाता था. मैं ने भारती जी की छिटपुट रचनाएँ ज़रूर पढ़ी थीं. लेकिन उन की विशिष्ठ छवि मेरे मन पर अंकित होने की सीमा तक उन के कृत्तित्व से मैं परिचित नहीं था. इस लिए जब हरएक की ज़बान पर उन का नाम था, तो मैं अपने आप को अँधेरे में पा रहा था. कोई कोई उन की प्रशंसा भी कर रहा था. अधिकांश को इस नए पद पर उन के आसीन हो जाने से ईर्षा थी. कुछ को उन से घृणा तक थी. न वे ईर्षा छिपाते थे, न घृणा. उस चर्चा के कस्बाती स्तर से मैं हैरान था. कई लोग उन्हें इलाहाबाद से जानते थे. उन का छोटापन रेखांकित करता कोई कहता – अरे, कल तक वह जूतियाँ चटखारता फिरता था! कोई कहता – वह साइकिल पर मारा मारा फिरता था! कोई उन की छकड़ा कार का ज़िक्र करता… और वह! आज धर्मयुग का संपादक बन गया!
मैं पूछ उठता : हर कोई एक समय घुटरियों चलता है, तो क्या यह अर्थ होगा कि वह कभी दौड़ नहीं सकता या उसे दौड़ने का अवसर न मिले?
मेरे मन में भारती जी के कृतित्व के बारे में जानने की इच्छा प्रबल हो उठी. मेरे एक सहकर्मी थे. वे इलाहाबाद से भारती जी को जानते थे, और ईर्षा से भरे थे. उन के एक मित्र थे. वह स्वयं कोई ख़ास नहीं लिखते थे. हाँ, साहित्यकार होने का और साहित्य पर फ़तवे देने का दंभ उन में भरा था. भारती जी के प्रति घृणा से ओतप्रोत रहते थे. भारती जी के कृतित्व के बारे में मैं ने उन से पूछा, तो वह बोले : वाहियात! बकवास!
मैं ने पढ़ने के लिए भारती जी की कोई रचना उन से माँगी. घटियापन का नमूना बता कर जो रचना उन्हों ने मुझे दी, वह थी – अंधा युग! मैं अभी तक उन का आभारी हूँ कि उन की कृपा से मुझे इस युग का प्रतिनिधित्व करने वाला नाटक पढ़ने को मिला…
मन का मंच…
उसी रात मैं ने अंधा युग पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता ही चला गया.
मेरे मन के असीम मंच पर कुछ बृहद् घटित होने लगा. एक विराट आकार उभरने लगा. वह आकार पूरे युग का था. वह आकार पूरे युग से बड़ा था. वह मानवता के शाश्वत रागद्वेष का, निरंतर संकट का, हलचलपूर्ण, क्रंदनपूर्ण, चिंघाड़ता, रिरियाता, मिनमिनाता, भिनभिनाता, घनघनाता परिवर्तनशील परिदृश्य था. पता नहीं – वह द्वापर था या कलियुग, वह विगत था या वर्तमान. जो था, वह था मानव अस्मिता का, जिजीविषा का, युयुत्सा का, जीत का, जीत की हार का, विभीषिका का, अकुलाहट का, छटपटाहट का, आशंका का, निरर्थकता का हरहराता लहराता महासागर…
रात के सन्नाटे में अजब सा तरल विरल मंचन था वह – मेरे मन पर.
महाकवि व्यास की रचना महाभारत जीवंत मानवता का महासागर है. मुझे लगा, और आज तक लगता है, कि इस महासागर के मंथन का सघन निष्कर्ष है – अंधा युग.
कुरुक्षेत्र में युद्ध की आसन्न विभीषिका के सम्मुख अर्जुन के मन में जो मोह व्यापा था और कृष्ण ने उस महासमर की सार्थकता का जो उपदेश अर्जुन को दिया था, उस युद्ध की विगत निरर्थकता के बोध से आरंभ होता है अंधा युग के पहले दृश्य में असंपृक्त तटस्थ प्रहरियों का वार्तालाप. और इति होती है कृष्ण की मृत्यु के साथ साथ द्वापर युग के अवसान और कलियुग के अवतरण से.
इस विस्तृत मर्म को घनीभूत कर के अंधा युग उस रात के गहन अंधकार में मेरे सामने एक उफनते सागर में उद्दंड उद्दाम लहरों को झेलता अडिग विशाल शिलाखंड सा मन को झकझोरता, चुनौतियाँ उछालता खड़ा था.
इतने बड़े कथ्य को अंधा युग के इतने छोटे कलेवर में समेट लेने के दुस्साहसपूर्ण प्रयास की परिकल्पना मात्र से अगर मैं विस्मित था, तो उस के कुशल निर्वाह से चमत्कृत, अवाक् और अभिभूत. मेरा मन पूछ रहा था – कैसे हैं ये लोग जो अंधा युग के रचेता को हीन हेय साबित करने पर तुले हैं!
पचासादि दशक हिंदी साहित्य में नए वादों के उदय का काल था. साहित्यिक गतिविधि में एकाएक आशाप्रद जीवंत तरंगता आ गई थी. जाने कहाँ से इतने सारे लेखक उमड़ आए थे और नए से नए प्रयोग कर रहे थे. हर रचनाकार अपनी अलग पहचान बनाने के लिए किसी नए वाद का प्रवर्तक बनने को बेचैन था. लगता था कि साहित्य में स्थापित होने के लिए यह एक आवश्यक शर्त बन गई है. एक नई तरह के थे ये लेखक – तीस और चालीस आदि दशकों के लेखकों से बिल्कुल अलग. न ये छायावादी थे, न हालावादी, न रोटी रोज़ी के नारे लगाने वाले, न देशप्रेम के गायक. ये मानव मन के अन्वेषक थे. इस अर्थ में यह दशक हिंदी का समृद्ध दशक कहलाने का हक़दार है.
राजनीतिक स्वतंत्रता ने देश को एक नया बोध दिया था. यह मानसिक स्वतंत्रता के स्तर पर भी परिलिक्षत हो रहा था. साहित्य में इस का मतलब था पुरानी प्रणालियों, विधाओं और धाराओं से मुक्ति. प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी. लेकिन वह क्षीण सी धारा अब महागंगा या अमेज़न बन गई थी. छंदों की जो पहचान गीतों में बची खुची थी, वह इस दशक में धूमिल होते होते मिटती गई या फ़िल्मी गीतों में सिमटने लगी. भावों और विचारों को पंक्ति की सीमा में बाँधने वाला छंदों का बंधन अब स्वीकार्य नहीं था. क्षणिक रागात्मकता का कोई भावुक पल हो या भावों के उद्दाम प्रवाह का रेला – दोनों के लिए मुक्त छंद एक मात्र रास्ता बचा रह गया.
नवजात विश्व चेतना
हमारी नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना पूरे संसार से जुड़ी थी. अब हम सारी दुनिया को, उस के औद्योगिक और भौतिक विकास को, उस के सरोकारों को, और इस दुनिया में चल रहे त्रासक शीत युद्ध को देख और आँक रहे थे. हमारी मानसिक सीमाओं के, कहें तो हमारे अंधे कूएँ की मुँडेरों के, परे जो अर्धज्ञात सा विस्तार था, हम उस में अपने आप को स्थापित करने की कोशिशें कर रहे थे. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद एक महात्रासक सर्वनाशकारी युद्ध आसन्न नज़र आता था, जिस पर परमाण्विक विनाश का भय ब्रह्मास्त्र की तरह लटक रहा था. हम गुट निरपेक्ष थे. लेकिन यह निरपेक्षता हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी. इस अल्पज्ञात विकराल परिवेश में हमें जीने की शर्तें तलाशनी थीं.
पचासादि दशक से हमारी कलाओं में जो सिलसिला शुरू हुआ, उस की आधार भूमि हमारी यह नवजाग्रत विश्व चेतना ही थी. हमारे सारे सृजनशील तत्त्व पूरे संसार, विशेषकर पश्चिमी संसार, के कलाबोध को आत्मसात करने को उतावले थे. आत्मसात वे कम कर पा रहे थे, थोक में आयात, या फ़िल्मी संवाद की भाषा में कहें तो, उधर का माल इधर ज़्यादा कर रहे थे. यहाँ वहाँ से कुछ पढ़ कर, कभी कभी गंभीर अध्ययन कर के और उस से चमत्कृत या प्रभावित हो कर वे विदेशी क़लमें हमारी धरती में गाड़ रहे थे, कभी कभी ठोंक रहे थे. कोई कोई रोप भी रहा था. लेकिन हमारे अधिकांश शैलीकार यह तथ्य नज़रअंदाज़ कर रहे थे कि पश्चिम में ये वाद रातो रात नमूदार नहीं हो गए थे. पूरी एक-डेढ़ सदियों के औद्योगिक विकास ने और संप्रेषण के क्षेत्र में मुसलसल प्रयोग, वादविवाद और परिवर्तन ने उन के लिए ज़मीन और खाद तैयार की थी.
तो यह था वह परिदृश्य जिस में अंधा युग अवतरित हुआ था. अपने समकालीन बहुचर्चित रचना संसार में वह भारतीय परंपराओं से पूरी तरह संलग्न था. साथ ही नए युग की चेतना से ओतप्रोत और विश्व मंच पर मँडराते संकट से आक्रांत. इसी बात में उस का महत्त्व था – और है. हमारे अपने धरातल पर यह हमारा अपना अनोखा बिरवा उगा था.
वीभत्स, रौद्र और वीर रसों के माध्यम से अंधा युग पाठक-दर्शक को करुण और शांत रसों तक ले जाता था. इसी में उस के आशावाद का सूत्र अंतर्निहित था और इसी के आधार पर नाटककार ने प्रारंभिक स्थापना के अंत में कहा था -
यह…
… कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से.
शिल्प के स्तर पर अंधा युग संस्कृत नाटकों की परंपरा से पूरी तरह जुड़ा था. स्थापना का आरंभ होता है परंपरागत शैली में मंगलाचरण से –
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ।।
यह नाटक को स्वयं महाभारत से जोड़ता है, क्योंकि यह महाभारत के प्रथम श्लोक का किंचित् परिवर्तित रूप है. इस के बाद विष्णु पुराण के एक श्लोक के आकर्षक अनुवाद के साथ नाटक की भूत और भावी घटनाओं की सूचना संस्कृत नाटकों के ‘विष्कंभक’ के रूप में दी जाती है.
पूरे नाटक में इसी पारंपरिक प्रणाली का अनुसरण किया गया है. हर अंक के आरंभ में कथा गायन होता है, जिसे हम अंकास्य कह सकते हैं. यह उस अंक या दृश्य की घटनाओं की भूमिका के साथ साथ भावी का आभास देता है. परंपरा निभाने के लिए यह कथा गायन छंदबद्ध है, जब कि नाटक में संवाद गद्य में न हो कर ऐसे मुक्त छंद में हैं, जो भावोद्रेकपूर्ण प्रवहमान गद्य का स्थान बख़ूबी ले लेता है.
यहाँ मैं नाटक के शिल्प की परंपरागतता की पूरी गहराई में नहीं जाना चाहता. लेकिन आगे बढ़ने से पहले कथा गायन के छंदों और उन के तुक विधान की विविधता का ज़िक्र न करना मेरे लिए कठिन हो रहा है. आरंभ होता है तीन पंक्तियों वाले एक छंद से. इस में पहली और तीसरी पंक्तियाँ परस्पर तुकांत हैं – क ख क. इसी अंश के अंत में चार पंक्तियों वाला एक छंद है जिस का वज़न उतना ही है, पर दूसरी और चौथी पंक्तियों में तुक मिलाई गई है – क ख ग ख.
चौथा अंक है गांधारी के शाप का अंक. युद्ध के उपरांत अश्वत्थामा बदले की भावना से ग्रस्त है. वह रात के अँधेरे में शत्रु के अरिक्षत शिविर में घुस कर पांडव पुत्रों की निर्मम हत्या कर देता है. इस अंक के मुख पर जो कथा गायन है, उस के छंद विलक्षण हैं. थोड़ी थोड़ी देर में छंद और लय का परिवर्तन होता है. यह सब इस अंक की वीभत्सता को मूर्त्तमान ध्वनि प्रदान करता है.
परंपरागत शैली में और हमारी चिरपरिचित कथा पर आधारित होने के बावजूद अंधा युग विश्व चेतना से संश्लिष्ठ है. इस में जिन रसों का परिपाक होता है, वे ग्रीक त्रासदियों के हैं. हमारे यहाँ भी कुछ पुराने नाटकों में इन रसों को आधार बनाया गया है. पर इस स्तर तक नहीं. जब मैं ने इसे पहली बार पढ़ा और मन के मंच पर घटते देखा, तो बार बार ग्रीक त्रासदियों के दृश्य मन पर उभरते रहे. ऐसा इस लिए नहीं होता था कि इस में ग्रीक त्रासदी का शिल्प है. वास्तव में, यह उस से बहुत दूर है. ग्रीक नाटकों में जो काल, दृश्य और घटनाक्रम की एकता या यूनिटी होनी चाहिए, वह इस में नहीं है. फिर भी इसे पढ़ते देखते ग्रीक त्रासदियों की याद आती है तो इस लिए कि पात्रों का व्यवहार कुछ कुछ उन जैसा है. ग्रीक नाटकों की ही तरह इस में कोरस है. कथा गायन कोरस का काम करता ही है, दोनों प्रहरी तो एकदम कोरस ही हैं. उन का काम है मुख्य पात्रों के क्रियाकलापों पर प्रतिक्रिया प्रकट करना. कई बार मुझे इन दोनों प्रहरियों ने उस रात शैक्सपीयर के नाटक हैमलेट के दोनों क़ब्र खोदने वालों की याद दिलाई. बड़े लोगों पर जो बीतती है, उस से असंपृक्त, तट पर खड़े दो प्रेक्षक जो दूर से तूफ़ान का नज़ारा कर रहे हैं. और उस पर कटाक्ष करते हैं.
पढ़ना भी एक प्रकार का मंचन होता है
हज़ारों ऐसे पाठक हैं जिन्हों ने अब तक अंधा युग की एक भी प्रस्तुति नहीं देखी, केवल पढ़ा है. और मन ही मन उसे मंचित किया है. क्यों कि जो पढ़ना होता है, वह भी एक प्रकार का मंचन होता है. हमारा मन किसी भी रचना के शब्दों को बिंबों में परिवर्तित करता है. यह रचना, यह कृति, कुछ भी हो सकती है – कविता, कहानी, नाटक, दर्शन ग्रंथ…
मंच पर जो प्रस्तुति होती है, वह मूर्त्त, रूढ़ और ससीम होती है. मंच सज्जा, विधान, अभिनय कर्मियों की शक्ल सूरत, हावभाव, चालढाल, आवाज़ – सब कंकरीट होते हैं – वास्तविक. जो वास्तविक है, वह मूर्त्त होता. उस की सीमा होती है. यह किसी कृति या मंचन की वक्रोक्ति क्षमता या पावर आफ़ सजेशन ही होती है, जो हमारे मनों को उद्वेलित कर के कला सृष्ठि या रस निष्पत्ति के लिए उकसाती है.
इस के विपरीत पढ़ा या सुना शब्द अमूर्त्त, अरूढ़ और असीम होता है. उसेे पढ़ या सुन कर मन जो रचता है, वह हर पाठक-श्रोता के लिए सामूहिक व सहभुक्त होते हुए भी नितांत निजी और आपबीती जैसा अनोखा होता है. इसी लिए वह स्वतंत्र और विविध होता है. हम सब अपनी कल्पनाशीलता के अनुरूप दृश्यविधान की, दृश्यावली की, अभिनय की, घटना की सृष्ठि करते हैं.
पचासादि दशक में दिल्ली में सरिता-कैरेवान पत्रिकाओं में संपादन कर्मी के रूप में मैं जो बहुत सारे काम करता था, उस में अँगरेजी कैरेवान पत्रिका के लिए मंच समीक्षा भी थी. साथ ही अपने निजी जीवन में मैं एक अदना से पार्श्वकर्मी के रूप में भी रंगमंच से जुड़ा था. दिल्ली में एक नाट्य मंडल हुआ करता था और अब तक है – दिल्ली आर्ट थिएटर. इस की नेता थीं पंजाबी कवियित्री, नाटककार और निर्देशिका श्रीमती शीला भाटिया. मेरा काम था मंच निर्देशकों की सहायता करना. किसी भी हालत में मेरा काम सर्जनात्मक नहीं कहा जा सकता था. लेकिन मेरे लिए शिक्षाप्रद ज़रूर था. मैं रंगमंच को यवनिका के दोनों ओर से देख रहा था, और समझने की कोशिश कर रहा था. मेरा अंधा युग का पठन इस काल के शीर्ष पर हुआ था.
दसेक वर्षों के दीर्घ काल में केवल कुछ ही प्रस्तुतियाँ थीं जिन में कोई गहरी छाप छोड़ने की क्षमता थी. जैसे, काल आफ़ द वैली (कश्मीर पर एक राजनीतिक व्यंग्य) या हीर राँझा. एक और कृति जो अभी तक याद है – वह थी आर.जी. आनंद लिखित और निर्देशित हम हिंदुस्तानी (बाद में इस से प्रेरित हो कर मोहन सहगल ने नई दिल्ली फ़िल्म बनाई.) और हाँ, बाहर से आने वालों की प्रस्तुतियाँ तो थीं ही. जैसे कलकत्ते के बहुरूपी के बंगाली नाटक, या दिल्ली में इप्टा समारोह के कुछ नाटक. और पृथ्वीराज जी के नाटक.
सन ६३ के आते आते कई कारणों से मैं ने मंच समीक्षा करना बंद कर दिया था. तब मुझे पता नहीं था कि कुछ ही सप्ताहों में मुझे दिल्ली छोड़ कर बंबई जाना होगा और वहाँ से फ़िल्म पत्रिका माधुरी का संपादन करना होगा.
ऐसे में पता चला कि दिल्ली में अक्तूबर १९६३ में अंधा युग का मंचन होने वाला है.
पहली मंच प्रस्तुति – खंडित इतिहास में
जैसे अंधा युग नाटक की परिकल्पना मात्र ही रोमांचक थी, वैसी ही यह प्रस्तुति होने वाली थी. इसके साथ कई प्रथम जुड़े थे. ये सब प्रथम अपने आप में अनोखे थे.
संगीत नाटक अकादमी के तत्त्वावधान में रंगमंच को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय नाट� विद्यालय (रानावि) की स्थापना १९५९ में हुई थी. अब इस के निदेशक बनाए गए थे – ख्यातिप्राप्त रंगकर्मी इब्राहिम अल्काज़ी.
अल्काज़ी का व्यक्तित्व अपने आप में आकर्षणों से भरा है. वह अरब मूल के भारतीय हैं. उन के कुवैती माता पिता व्यापार के लिए भारत आए और पुणें में बस गए. वहीं इब्राहिम की शिक्षा दीक्षा हुई. लंदन की ख्यातिप्राप्त राडा (रायल अकाडेमी आफ़ ड्रमैटिक आट्र्स) में उन्हों ने रंगकर्म में दक्षता प्राप्त की और अनेक पुरस्कार जीते. मुंबई (तब बंबई) आ कर उन्हों ने १९५४ में थिएटर यूनिट नामक रंगमंडल की स्थापना की. इस के अनेक हिंदी अँगरेजी नाटकों ने न केवल प्रशंसा पाई बल्कि नई चेतना वाले कटिबद्ध रंगकर्मियों और दर्शकों का एक पूरा वर्ग तैयार किया. सुप्रसिद्ध मराठी नाटककार और तत्कालीन संसद सदस्य मामा वरेरकर की अनुशंसा पर भारत सरकार ने उन्हें रानावि का निदेशक नियुक्त किया. रानावि के छात्रों द्वारा अभिनीत और मंचित अंधा युग दिल्ली में उन की पहली प्रस्तुति होने वाला था.
और यह भी उत्सुकता का विषय था कि यह प्रस्तुति किसी सभागार में न हो कर फ़ीरोजशाह कोटले की ऐतिहासिक प्राचीरों के बीच होने वाली थी.
यह कोटला दिल्ली का एक बहुचर्चित भग्नावशेष है. शाहजहाँ ने जो दिल्ली बसाई थी, उस के दिल्ली गेट से निकल कर सामने बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर चलो तो आधा पौना किलोमीटर दूर सड़क के बीचोबीच एक प्राचीन टूटी फूटी ऊँ�ची दरवाज़ानुमा मीनार सी खड़ी है. सन अट्ठारह सौ सत्तावन के विद्रोह को कुचलने के लिए यहाँ अँगरेजों ने ख़ून की नदियाँ बहा दी थीं. इस लिए इसे ख़ूनी दरवाज़ा कहते हैं. जहाँ तक मुझे याद है उन दिनों तक भी यहाँ सड़क के दाहिनी ओर एक ऊँ�चा परकोटा हुआ करता था. यह दिल्ली की जेल की चहारदीवारी थी. गिरफ़्तार हो कर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी यहाँ रखे जाते थे. इस लिए दिल्ली वालों के लिए यह चहारदीवारी जीवित इतिहास का अंग थी.
बाईं ओर सामने – चौड़े मैदान के पार है तुग़लक सुल्तान फ़ीरोजशाह का कोटला. इस की ऊँची चौड़ी दीवारों के नंगे अधनंगे काही लगे पत्थर एक भव्य काल के भग्न इतिहास की कहानी कहते मालूम पड़ते हैं. निश्चय ही फ़ीरोजशाह शौक़ीन सुल्तान रहा होगा. उसे भारत के प्राचीन गौरव का पूरा भान रहा होगा. इसी लिए उस ने कहीं कहीं से उखड़वा कर और बड़े जतन से पचासियों बैलगाड़ियों में रूई के गट्ठरों में लपेट और ढुलवा कर सम्राट अशोक की दो लंबी लाटें दिल्ली में गड़वा दी थीं. इन में से एक को उस ने इसी कोटले के सब से ऊँ�चे भवन के शिखर पर स्थापित करवाया था. (इतनी लंबी और भारी लाट को इतनी ऊँ�चाई पर चढ़ा कर खड़ा करना पिरामिड बनाने से कम करतब का काम नहीं रहा होगा.)
उन दिनों इस कोटले से आगे प्रैस कांप्लैक्स नहीं था, जहाँ से आजकल दिल्ली के कई प्रसिद्ध दैनिक पत्र निकलते हैं. कोई दो किलोमीटर दिक्षण है पुराना क़िला. इसे शाहजहाँ के पड़बाबा मुग़ल सम्राट हुमायूँ ने बनवाया था. इसी में दुर्घटनाग्रस्त हो कर उस की मृत्यु हुई थी. मान्यता है कि यह पुराना क़िला उस दुर्ग के खंडहरों पर बसा है जहाँ पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई थी, और जिस के उद्घाटन समारोह पर द्रौपदी ने कौरव राजकुमार दुर्योधन पर ऐतिहासिक कटाक्ष किया था. कहते हैं कि पांडवों के इंद्रप्रस्थ से भी हज़ारों साल पहले इसी स्थान पर खांडवप्रस्थ हुआ करता था…
आसपास चारों ओर है आधुनिक दिल्ली. नई दिल्ली – स्वतंत्र भारत की राजधानी. भारतीय गणतंत्र का महत्त्वपूर्ण स्तंभ सर्वोच्च नयायालय बस थोड़ी ही दूर पर है.
खंडित इतिहास – युगोँ का संयोजक स्थल
इस प्रकार यह कोटला दिल्ली वालों के मानस पर पौराणिक, प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन इतिहास का संयोजक स्थल बन जाता है. यहाँ अंधा युग की प्रस्तुति होना खंडित इतिहास को जीवित इतिहास के बीच रखने जैसा था.
इस कोटले में मंच प्रस्तुति का यह पहला अवसर नहीं था. श्रीराम भारतीय कलाकेंद्र वाले यहाँ कई वर्षों से दशहरे के अवसर पर अपनी नृत्यनाटिका रामलीला का मंचन करते रहे थे. इस का मंचन कोटले के बाहर वाले मैदान में टीन की चादरों से परकोटा खींच कर मुक्ताकाशीय हुआ करता था. मंचविधान और दर्शक दीर्घा की परिकल्पना प्रोसेनियम थिएटर की ही तरह होती थी. और टीन का परकोटा कोटले की ऐतिहासिकता से इसे बिल्कुल काट देता था.
अंधा युग में कोटला स्वयं एक उपांग का काम कर रहा था. उसे नाटक में संप्रेषण का एक अविभाज्य अंग बना दिया गया था. पुरानी प्राचीरों से घिरा एक आंगन तलाशा गया था. सामने की दीवार में कुछ ऊँचाई पर एक अभिनय मंच बनाया गया था. उस तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं. नीचे धरातल पर भी अभिनय के लिए स्थान रखा गया था. दीवार की चौड़ी मुँडेर का उपयोग प्रहरियों की गश्त और उन के अधिकांश संवादों के लिए किया गया था. मानों वे सचमुच हस्तिनापुर की प्राचीरों पर पहरा दे रहे हों.
रंगमंच और दर्शक दीर्घा के बीच कोई यवनिका नहीं थी. स्थान ग्रहण करने के लिए आता दर्शक पुरानी प्राचीरों को, एक कोने में प्राचीर के सहारे बने मंच को, उस के नीचे अभिनय स्थल को और अग्रभूमि को एक साथ देखता और आत्मसात करता था.
भग्न भव्यता की प्रतीति को प्रबलित करने के लिए अग्रभूमि में किसी पौराणिक रथ के जैसा एक बड़ा लेकिन टूटा पहिया खड़ा किया गया था. बिना कुछ कहे यह दर्शकों के मन में महारथी कर्ण के रथ का टूटा पहिया बन जाता था – उस अंधे युग के मानव मूल्यों के विघटन की प्रतिमा, मानव के नैतिक भ्रंश का मुखर प्रतीक.
अब दर्शक एक संघर्षपूर्ण विराट अनुभव से साक्षात्कार के लिए तैयार था.
यह विराटता, भव्यता, विलक्षणता, और रेखांकित ऐतिहासिकता ही अल्काज़ी की उस प्रस्तुति का मुख्य कथ्य थी. इतना विलक्षण मंच विधान, इतनी भव्य प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था, इतना विराट आकार – ये सब दिल्ली के दर्शकों ने इस से पहले कभी नहीं देखे थे, जो पात्रों के क्रियाकलाप इतने विशाल पैमाने पर प्रस्तुत कर रहे हों. न रंगमंडलों के पास इतने साधन होते थे, न सरकार से उन्हें कोई अनुमति मिल सकती थी कि किसी आरिक्षत पुरावशेष की दीवारों का उपयोग नाटकीय मंचन के लिए कर सकें. यहाँ यह भी कहना चाहिए कि ऐसा करने की कल्पना तक इस से पहले किसी के मन में न आई होगी.
अगर भौतिक विराट अल्काज़ी के नेतृत्व में तैयार किया गया था, तो इतिहास की भग्नता का भाव पक्ष भारती जी की कृति में पहले से ही मौजूद था. जो विशाल धरातल तैयार किया गया था वह अभिनय कर्मियों को पात्रों के अनुभावों को सजीव करने की खुली प्रेरणा दे रहा था. वे स्वयं कुछ ऐतिहासिक कर दिखाने के बोध से अनुप्राणित थे. विशाल के बीच जब वे चलते फिरते या संवाद बोलते थे, तो सशक्त कथ्य विराट बनने लगता. इस बिगनैस को, इस बृहद्ता को रेखांकित करती थी – पात्रों के संवाद की उच्चारण शैली. गतिशील पौरुषेय गद्य जैसा काव्य का यति और आघात सहित चमत्कारी वाचन. काव्य होते हुए भी वास्तव में यह लयबद्ध काव्य वाचन नहीं था. इस में ओतप्रोत लय थी – संवादों की.
दिल्ली वालों के लिए यह अपनी तरह का पहला अनुभव था. दिल्ली में इस के बाद अंधा युग के मंचन स्वयं पुराने क़िले में भी हुए – वह मैं ने नहीं देखे, क्यों कि मैं तब बंबई चला गया था.
दूसरी मंच प्रस्तुति – बंबई में प्रोसेनियम मंच पर
महान अभिनेता स्वर्गीय ओम शिवपुरी के सहयोग से प्रस्तुत अल्काज़ी का अंधा युग का मंचन अगर मेरे लिए दिल्ली में देखा अंतिम नाटक सिद्ध हुआ तो बंबई में जो नाटक मैं ने सब से पहले देखा – वह था पंडित सत्यदेव दुबे के निर्देशन में अंधा युग. इस मंचन को देखने वालों में स्वयं भारती जी भी थे. मैं १९६४ वाले मंचन की बात कर रहा हूँ जो वहाँ के बिरला मातुश्री सभागार में हुआ था.
दस साल पहले बंबई में अल्काज़ी ने थिएटर यूनिट की स्थापना की थी. दुबे उस से जुड़े आ रहे थे. दुबे से पहले उस के निदेशक फ़िल्म निर्देशक अभिनेता विजय आनंद रह चुके थे. जब मैं बंबई पहुँचा तो थिएटर यूनिट के कर्ता धर्ता और चलते फिरते दफ़्तर दुबे ही नज़र आते थे. उन के साथ अमरीष पुरी जैसे कुशल रंगकर्मियों का एक पूरा दल था, जिस की दुबे में पूरी निष्ठा थी.
आधुनिक हिंदी रंगमंच के इतिहास में दुबे का नाम अंधा युग से अविभाज्य रूप से जुड़ गया है. सुना है सब से पहले इसे इलाहाबाद से रेडियो पर प्रसारित किया गया था. शायद मंचन भी हुआ था. बंबई में थिएटर यूनिट के लिए दुबे के निर्देशन में १९६२ में नवंबर दिसंबर में एक अपार्टमैंट हाउस की खुली छत पर इस का जो प्रथम मंचन हुआ था, वह आधुनिक हिंदी रंगमंच के इतिहास में एक मोड़ माना जाता है. मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में अल्काज़ी की प्रस्तुति उस से कहाँ तक प्रभावित थी, या प्रभावित थी भी या नहीं. क्यों कि मैं ने दुबे की वह प्रस्तुति नहीं देखी. उस के बारह प्रदर्शन हुए थे. कहा जाता है कि लगभग इतने ही सौ दर्शकों ने उसे देखा. इस का अर्थ है प्रति प्रदर्शन कोई एक सौ दर्शक. इस से ज़्यादा दर्शक उस छत पर आ भी नहीं सकते थे. यह भी कल्पना की जा सकती है कि दर्शकों और कलाकारों के बीच कितने निकट का तादात्म्य स्थापित हो जाता होगा.
खचाखच भरे बिरला मातुश्री सभागार की दर्शक क्षमता कोई छः सात सौ रही होगी. हर प्रोसेनियम थिएटर की तरह इस में भी मंच और दर्शक दीर्घा के बीच एक दूरी हो जाती थी. लेकिन ऐसे हर सभागार में अंधकार के बाद दर्शक अपने पड़ोसी से कट कर मंच के क्रियाकलाप से सीधे जुड़ जाता है.
बिरला मातुश्री जैसे छोटे सभागारों में विशाल और विराट की सृष्ठि भौतिक उपकरणों से नहीं की जा सकती. यदि नाटक की आवश्यकता हो तो यह काम अभिनय और आवाज़ से करना होता है. लेकिन दुबे की रुचि दर्शकों पर विराट का प्रभाव डालने की नहीं थी. वह उन्हें कथाक्रम के भीतर पैठने के लिए आमंत्रित और बाध्य कर रहे थे. उन की प्रस्तुति नाटक थी, भव्यता का, स्पैटेकल का प्रदर्शन नहीं.
सच कहा जाए तो दुबे सही अर्थों में आधुनिक सूत्रधार हैं. मंच पर हर कर्म का सूत्र उन के हाथ में रहता है. मैं समझता हूँ कि उन की कला के सर्वाधिक शक्तिशाली तत्त्व हैं – कथ्य के मर्म में उन की गहरी पैठ, पात्रों की मानसिकता की तीखी समझ, और संवादों के वाक्यांशों में छिपे भावों की सही पहचान. बंबई में उन के द्वारा निर्देर्शित मंचित कई नाटक मैं ने देखे हैं. मोहन राकेश का आधे अधूरे, जहाँ तक याद है सार्त्र पर आधारित बंद दरवाज़े, इब्सन का शायद डाल्स हाउस, विजय तेंडूलकर के कई नाटक गिधाड़े, शांतता कोर्ट चालू आहे… और इसी नाटक पर हिंदी फ़िल्म… हरएक में वह दर्शकों को पात्रों से संपृक्त करने में सफल रहते थे. यही उन्हों ने अंधा युग की उस प्रस्तुति में भी किया था. दर्शक अपने आप को हर पात्र से सहानुभूति में पाता था, फिर सर्वांगीण घटनाक्रम का तटस्थ विश्लेषक भी बन जाता था.
तीसरी मंच प्रस्तुति – दिल्ली में चतुर्दिक् घिरा दर्शक
और इस के अट्ठाईस साल बाद[1]… सितंबर १९९२ में मैं ने दिल्ली में देखा अंधा युग का एक और ही रूप. कैसा नाटक है यह जिसे किसी भी साँचे में ढाला जा सकता है!
यह अनोखी प्रस्तुति थी राम गोपाल बजाज द्वारा निर्देशित और रानावि के छात्रों द्वारा अभिनीत. मेरे लिए यह अपनी तरह का एकमात्र, और अभी तक एकमात्र, अनुभव था. मंचन शैली में शायद पूरे विश्व में अपनी तरह का एकमात्र अभिनव सफल प्रयोग. मैं नहीं समझता कि हर ओर से दर्शक को घेर लेने वाली, ओतप्रोत कर देने वाली कोई और प्रस्तुति मैं ने देखी या सुनी हो.
अंधा युग से बजाज का निजी संबंध बहुत पुराना है. सन ६३ वाली अल्काज़ी की प्रस्तुति में उन्हों ने धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु की भूमिका की थी – जिस के लिए विजय भी पराजय बन जाती है. इस बीच दिल्ली में अंधा युग कई बार मंचित हो चुका था. उन मंचनों से भी बजाज का सक्रिय संबंध रहा था. अतः अंधा युग को वह गहराई से जानते पहचानते हैं. वह स्वयं कविहृदय हैं. संस्कृत और हिंदी काव्य में उन की गहरी रुचि है. काव्य पाठ की उन की अपनी शैली है और इस के वह धनी माने जाते हैं. इस का संप्रेषण वह अपने छात्र अभिनेताओं में भी कर पाए – यह उन के मंचन से स्पष्ठ था.
पर सब से पहले इस प्रस्तुति के मंच विधान के बारे में बात करनी होगी.
मैं ने सुना है कि दिल्ली में थिएटर इन द राउंड के प्रयोग इस से भी पहले भी हो चुके थे. जैसे गाँवों में साँगों या नट के तमाशों में होता है, या दशहरे के अवसर पर हर जगह होने वाली पारंपरिक रामलीला में, दर्शक रंगमंच के चारों ओर होते हैं, वैसा ही इस में भी था. लेकिन उस से कुछ बढ़ कर भी था. मैं ने न्यू यार्क में ब्राडवे पर किसी सभागार में बरनार्ड शा के किसी नाटक का मंचन थिएटर इन द राउंड शैली में देखा है. वह एक बहुत बड़ा सभागार था. छतदार चौकोर स्टेडियम जैसा. बीचोबीच पिट में, या तल में, एक बड़ा और चौकोर रंगस्थल था. चारों ओर सीढ़ियों पर दर्शक दीर्घा थी. हर ओर दर्शकों की कम से कम दस बारह पंक्तियाँ ज़रूर रही होंगी. मंच पर ड्राइंग रूम का छतहीन सैट लगा था. दर्शक नाट� व्यापार को सामने से नहीं ऊपर से एक कोण से देख रहे थे. दर्शक दीर्घाओं की सीढ़ियों के नीचे ग्रीन रूम आदि की व्यवस्था थी. वहीं से पात्र मंच पर प्रवेश करते थे.
दिल्ली के कोटले में अंधा युग के मंच विधान में इस से केवल इतनी साम्यता थी कि मंच क्षेत्र तल में बीचोबीच था. लेकिन मंच पर किसी प्रकार का कोई सैट नहीं था, न ही स्टेज प्रापर्टी – साजसामान. मुक्ताकाशीय गोलाकार मंच पूर्णतः शून्य था. उस के केंद्र में था कोई दो तीन फ़ुट का चबूतरा जैसे सड़कों के चौराहों पर सिपाही के लिए होता है. यह अपने आप में एक पूर्णतः अमूर्त्त रचना थी. यह दर्शकों के मन पर किसी प्रकार का कोई भाव उपस्थित नहीं कर रही थी. मंच और मन ख़ाली सलेट की तरह थे. अब इन पर कुछ भी लिखा जा सकता था.
थिएटर इन द सराउंड
चारों ओर थी दर्शक दीर्घा. दर्शकों के बैठने के लिए केवल दो पंक्तियाँ थीं. स्टेडियम जैसी चौड़ी सीढ़ियों पर आप पालथी मार कर बैठ सकते थे, या पैर फैला कर पसर सकते थे, या फिर नीचे पैर लटका कर. इन दीर्घाओं तक आने के लिए चारों कोनों पर चार रैंप थे – जो बाहर से चढ़ा कर हमें वहाँ तक लाते थे, और फिर नीचे रंग मंडल तक उतर जाते थे. बाद में पता चला कि अभिनय कर्मी भी इन्हीं पर से प्रवेश करेंगे. दर्शकों की दूसरी पंक्ति के पीछे चारों ओर एक चौड़ी पटरी थी. ऐसी व्यवस्था की गई थी कि दर्शक इन पटरियों के किसी भाग को घेर न सकें. मैं इन पटरियों की उपयोगिता के बारे में विस्मय में था.
भेद तब खुला जब मंचन आरंभ हुआ. संगीत के स्वर छिड़े. कोई साठेक अभिनेता पंदरह सोलह के समूहों में बाहर से (यानी हमारे पीछे और सामने से दाहिने और बाएँ वाले रैंपों पर) चढ़े और चारों पटरियों पर मंच की ओर मुँह कर के खड़े हो गए. वे चुस्त चाल से आए थे. उन के आने में एक गति थी, जीवंतता थी, लय थी, जो संगीत की लय थी. अब हम दर्शक चारों ओर से अभिनेताओं से घिरे थे.
मंगलाचरण का पाठ, उद्घोषणा और पहले अंक का कथा गायन अंधा युग की प्रस्तुतियों में अकसर नेपथ्य से ही होता रहा है. यहाँ हमारे चारों ओर से, सामने से, पार्श्व से, पीछे से यह गाया जा रहा था. मंच कर्मियों से और कुछ देर बाद स्वयं मंच कर्म के खंडों से घिर जाने का दर्शकों के लिए संसार में यह शायद पहला अनुभव रहा होगा. हम नाटक के दर्शक होने के साथ साथ उस के घटनाक्रम में समाहित हो गए थे. लगता था कि हम स्वयं महाभारत में और अंधा युग में प्रवेश कर गए हैं. जो कुछ हो रहा है हम उस से अलग नहीं, बल्कि उस के बीच में हैं. थिएटर इन द राउंड के मुक़ाबले मैं इसे, यदि अँगरेजी का व्याकरण असम्मत मुहावरा गढ़ना हो तो, थिएटर इन द सराउंड कहूँगा.
रामलीला में मंच कर्म करने से पहले अभिनेता रंगमंडल का पूरा चक्कर लगा कर अपने को दिखाते हैं – जैसे स्टेडियम में खेल शुरू होने से पहले सारी मंडलियाँ घूमती हैं. यहाँ वे हमारे पीछे घूम रहे थे. हम पीछे मुड़ कर न देखने लगें, इस लिए चारों पटरियों वाले अभिनेता नृत्यात्मक चाल से चल कर नई पटरियों पर जाते रहते थे और गाते रहते थे. ये जो सारे अभिनेता थे, इन में से सभी को नाटक में भूमिका नहीं निभानी थी. ये सब कथा गायक का काम कर रहे थे. कथा गायन समाप्त होने पर इन में से कुछ तलस्थ मंच के चारों ओर बैठ गए, कुछ नेपथ्य में चले गए.
अब बचे केवल दो प्रहरी, जो इस पटरी से उस पटरी पर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे और संवाद बोल रहे थे –
थके हुए हैं हम
पर घूम घूम पहरा देते हैं
इस सूने गलियारे में…
विदुर के प्रवेश के साथ क्रियाकलाप तलस्थ मंच पर होने लगता है. पात्रों के मंच प्रवेश का मतलब है – उस के चारों ओर बैठे किसी अभिनेता का उठ कर गोल मंच पर आना या कभी कभी सभागार से बाहर से होते हुए रैंप से उतर कर मंच पर जाना. मंच का क्रिया कलाप फैल कर कभी कभी रैंपों पर आ जाता है, और कभी रैंपों पर होता हुआ चतुर्दिक् पटरियों पर चारों ओर बिखर जाता है.
वास्तव में इस संपूर्ण प्रस्तुति की शैली को इस अनोखे मंच विधान ने निश्चित और प्रभावित किया होगा. अधिकांश अंश नाटकों की गति से ही प्रस्तुत किए गए थे. लेकिन जब समूहों का काम आता था, तो उस की गति तीव्र हो जाती थी, पद संचालन नृत्य न होते हुए भी लयशील हो जाता था. अनेक स्थलों पर, कहना चाहिए अधिकतर स्थलों पर, संगीत में और मंच कलाप में महाप्रभु चैतन्य का वैष्णव भक्ति जैसा आभास होता था. कथानक के कृष्ण से संबद्ध होने के कारण यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता था.
बजाज ने अंधा युग को न केवल मानवता के बाह्य और आंतरिक संकट का प्रतीक बना दिया, बल्कि उस के वृद्ध याचक और जरा व्याध को बुद्धिजीवियों के मूल्यों के संकट का प्रतिरूप भी.
एक स्थल पर – अंतराल में – वृद्ध याचक के लंबे अभिभाषण में उन्हों ने काल के अमूर्त्त प्रवाह को रंगीन साड़ियों की नदी सा मंच के आरपार बहा दिया. वृद्ध याचक कह रहा था -
जीवन एक अनवरत प्रवाह है…
और बाहर से एक रैंप पर साड़ियों की लड़ी बन लहराता काल चला आया और मंच पर बहता सामने वाले रैंप से बाहर निकल गया…
इस प्रस्तुति की बहुत सी चीज़ें हैं जो मन पर अंकित हैं, क्यों कि यह प्रस्तुति अभी हाल (सितंबर १९९२) में हुई थी. अगर मुझे ऐसे किसी एक बिंब का नाम लेने को कहा जाए, तो मैं कहूँगा – अंतराल के बाद जब गांधारी के शाप वाला चौथा अंक शुरू होता है, तो उस समय का कथा गायन, शिव का तांडव, उस का संगीत, और काव्य के ये शब्द –
वे शंकर थे
वे रौद्रवेषधारी विराट
प्रलयंकर थे
जो शिविर द्वार पर दीखे
अश्वत्थामा को
अनगिनत विष भरे साँप
भुजाओं पर
बाँधे
वे रोम रोम में अगणित
महाप्रलय
साधे
जो शिविर द्वार पर दीखे
अश्वत्थामा को
और इस के कुछ ही पल बाद अश्वत्थामा की शिव पूजा –
जटा कटाह संभ्रमन्निलिंप निर्झरी समा
विलोल वीचि वल्लरि विराजमान् मूर्धनि
धगद्धगद्धगज्ज्वलललाट पट्ट पावके
किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम.
और
वे आशुतोष हैं
हाथ उठा कर बोले
अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय
हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय…
© अरविंद कुमार
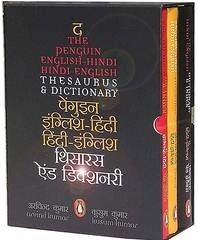
Comments