—अरविंद कुमार
दिन 1 – 1963
आर. के. स्टूडियोज़ के मुख्य ब्लाक में पहली मंज़िल पर छोटे से फ़िल्म संपादन कक्ष में राज कपूर और मैं नितांत अकेले थे. उन के पास मुझे छोड़ कर शैलेंद्र न जाने कहाँ चले गए.
1963 के नवंबर का अंतिम या दिसंबर का पहला सप्ताह था. दिल्ली से बंबई आए मुझे पंदरह-बीस दिन हुए होंगे. टाइम्स आफ़ इंडिया संस्थान के लिए 26 जनवरी 1964 गणतंत्र दिवस तक बतौर संपादक मुझे एक नई फ़िल्म पत्रिका निकालनी थी. बंबई मेरे लिए सिनेमाघरों में देखा शहर भर था. फ़िल्मों के बारे में जो थोड़ा बहुत जानता था, वह कुछ फ़िल्में देखने और सरिता कैरेवान में उन की समीक्षा लिख देने तक था. अच्छी बुरी फ़िल्म की समझ तो थी, लेकिन वह अच्छी क्यों है, और कोई फ़िल्म बुरी क्यों होती है – यह मैं नहीँ जानता था. फ़िल्म वालों की दुनिया क्या है, कैसी है, कैसे रहती है, कैसे चलती है, वे फ़िल्में क्योँ और कैसे बनाते हैँ – यह सब मेरे लिए अभी तक अनपढ़ी किताब था.
उस भरीपूरी गुंजान दुनिया में मेरे दो ही हीरो थे. एक: गीतकार शैलेंद्र. दो: निर्दशक-निर्माता-अभिनेता राज कपूर.
शैलेंद्र यानी जन नाट्य संघ (इप्टा) के सक्रिय सदस्य, जिन्होँ ने इप्टा का यह थीम गीत लिखा था– तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यक़ीन कर
तू ज़िंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पर यक़ीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन,
ये दिन भी जायेंगे गुज़र, गुज़र गए हज़ार दिन,
कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार कि नज़र,
अगर कहीँ है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
तू ज़िंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पर यक़ीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर,
तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर,
तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
तू ज़िंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पर यक़ीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
हज़ार वेश धर के आई, मौत तेरे द्वार पर,
मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर,
नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर.
और राज कपूर यानी मेरी नज़र में सर्वोत्तम निर्दशक-निर्माता-अभिनेता. राज की हर फ़िल्म मुझे अच्छी लगती थी. राज का अभिनय, राज की विचारधारा, फ़िल्मोँ के ज़रिए समाज को झकझोर देने की राज की ताक़त. और इस ताक़त के पीछे शैलेंद्र के गीतों का जो योगदान था, वह भी मैं जानता था. मेरा सौभाग्य ही था कि उस दुनिया में मेरी पहली निजी मुलाक़ात शैलेंद्र जी से हुई और उन के ज़रिए राज कपूर से. उस शाम हम आर. के. स्टूडियोज़ पहुँचे तो संदेश मिला कि वह मुझे सीधे उन के संपादन कक्ष में ले आएँ. मुझे वहाँ छोड़ कर वह पता नहीँ कहाँ चले गए.
तो अब उस छोटे से कमरे में बस राज कपूर और मैं ही थे. मैं उन का फ़ैन और वह मेरे हीरो. और भी बहुत कुछ था. राज कपूर के खिले मुसकाते चेहरे पर एक तपाक स्वागत की खुली चमक. और मूवियोला मशीन. फ़िल्म संपादन का उन दिनों का एक यंत्र या उपकरण. फ़िल्म शौटों के गोल डिब्बे अलमारी में रखे थे. मूवियोला के आसपास फ़िल्म शौटों की पट्टियाँ लटक रही थीं. कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ़ था. और धूल प्रूफ़ भी. धूल के एक कण का प्रवेश भी वर्जित था. फ़र्श पर मोटा रोएँदार क़ालीन था जो भूलेभटके भीतर आ जाने वाले धूल कण को अपने में समेट लेता था. कमरे में घुसने से पहले जूते चप्पल बाहर छोड़ देने होते थे.
यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था. जादुई. संगम फ़िल्म की शूटिंग उन दिनों नहीँ हो रही थी. ऐसे में राज हाल ही में उस के फ़िल्मांकित दृश्यों का संपादन कर रहे थे. पत्रपत्रिका का संपादन क्या होता है – यह मैं जानता था. फ़िल्मों का भी संपादन होता है – यह मैं फ़िल्मों में संपादक का नाम पढ़ पढ़ कर जानता था. फ़िल्म में शौट होते हैं. यह पता था. पर शौट होता क्या बला है – यह मुझे पता नहीँ था. और यह भी पता नहीँ था कि राज कपूर की किसी भी फ़िल्म मेँ निर्देशक, लेखक, गीतकार, संगीतकार, संपादक कोई भी हो राज कपूर भी यह सब होता है. इस का पहला आभास मुझे उस शाम हुआ. वह हरफ़न ‘मौला’ नहीँ, हरफ़न ‘मालिक’ थे – यह मैं ने धीरे धीरे जाना.
राज ने औपचारिकता मेँ अधिक समय नहीँ लगाया. संगम का संपादन करने और मुझे दिखाने लगे. फ़िल्म शौटों की जो पट्टियाँ वहाँ चुटकियोँ से झूल रही थीं, वे संगम के झील में नौकायन वाले दृश्य के कई शौट थीं. मूवियोला में उस नौकायन दृश्य का अभी तक अपूर्ण संपादित अंश चढ़ा था. राज ने मुझे वह दिखाया. उस में कभी एक नाव तिरछी बल खाती बाएँ से दाएँ जा रही थी, कभी सीधे, कभी कई नावें हमारी तरफ़ आ रही थीँ. कहीँ वैजयंती माला का एकल शौट था, कभी राज के साथ, या राजेंद्र कुमार के साथ. (मुझे तो इतना सब काफ़ी लग रहा था. यह मैं ने मुँह से कुछ नहीँ कहा.) पर राज संतुष्ट नहीँ थे. झूलती किसी एक पट्टी को उतार कर वह मूवियोला में लगाते, असंतोष के भाव से उतारते, फिर दूसरी लगाते. फिर वही असंतोष. उन्हों ने बताया कि वह किसी ऐसे शौट की तलाश में हैं, जो दृश्य के बहाव को बीच में एक भिन्न दिशा दे सके ताकि दर्शक की आँख को कुछ भिन्न मिले, ब्रेक मिले. काफ़ी देर यह सिलसिला चलता रहा. आख़िर पूरी तरह असंतुष्ट वह उठे, बोले, “चलो, किसी और समय वह इस दृश्य को अंतिम रूप दूँगा. चलो, बाहर चल कर बैठते हैं.”
यह जो बाहर था, वह उसी संपादन कक्ष से सटा लाल मख़मल की चौड़ी गदीली सीटों की तीन चार पंक्तियों वाला बीस-तीस दर्शकों के लायक़ आडिटोरियम था. तब तक की मेरी भाषा में छोटा सा सिनेमाघर. सीटों से काफ़ी दूरी पर परदा था. हम दोनों बीच की दो सीटों में धँस गए. राज कपूर की सीट के साथ ही रखा था एक टेलिफ़ोन.
यहाँ शुरू हुआ राज कपूर का और मेरा एक दूसरे को निजी तौर पर समझने और परखने का, निस्संकोच बातचीत, का दौर. राज ने कहा, “हमारे पीछे मशीन आपरेटर के पास उन की सभी फ़िल्मोँ के गीतोँ संकलन है. मैं जो भी गीत देखना चाहूँ, उस का नाम लूँ.” मैं ने कहा कि मैं आवारा फ़िल्म का वह गीत देखना चाहता हूँ जिस में जब जज रघुनाथ अपनी गर्भवती पत्नी को जग्गा डाकू के अड्डे पर चार दिन रहने के अपराध पर निकाल देता है, तो बरसाती रात में सड़क पर दुकान के थड़े पर बैठे भैया लोग गा रहे हैं – गीत के बोल तो मुझे याद नहीँ, पर कुछ ऐसे हैं – किया कौन अपराध त्याग दई सीता महतारी.
राज कपूर चौंक गए. पास ही रखे टेलिफ़ोन का चोँगा उठा कर आपरेटर को आदेश दिया, और मेरे सामने चल रहा था मेरा पसंदीदा सीन. और मोहम्मद रफ़ी की उन दिनों की टटकी आवाज़ में आरोप लगाता गीत…
पतिवरता सीता माई को
तू ने दिया बनवास
क्यों न फटा धरती का कलेजा
क्यों न फटा आकाश
जुलुम सहे भारी जनक दुलारी
जनक दुलारी राम की प्यारी
फिरे मारी मारी जनक दुलारी
जुलुम सहे भारी जनक दुलारी
गगन महल का राजा देखो
कैसा खेल दिखाए
सीप का मोती, गंदे जल में
सुंदर कँवल खिलाए
अजब तेरी लीला है गिरधारी
जुलुम सहे भारी जनक दुलारी
परदे पर मैं देख रहा था लीला चिटणीस महल-जैसे घर के दरवाज़े से बाहर निकल रही है. जुलुम सहे भारी जनक दुलारी. गगन महल का राजा पृथ्वीराज का क्रुद्ध और अपराध बोध से ग्रस्त क्लोज़अप. बाहर बिजली कड़कड़ा रही है. मेघरेखा चमचमा रही है. कोई आदमी छाता लगाए घनघोर बरसात से भरी सड़क पार कर रहा है. दस बारह लोग तन्मय हो कर गा रहे हैं, गा क्या रहे गुहार कर रहे हैं. जुलुम सहे भारी जनक दुलारी. लीला चिटणीस मारी मारी गिरती पड़ती फिर रही है. नाली के पास बहते मानी में गिर पड़ती है. नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आती है. सीप का मोती, गंदे जल में सुंदर कँवल खिलाए. अजब तेरी लीला है गिरधारी
सशक्त मर्मस्पर्शी फ़िल्मांकन गीत के भाव दर्शकोँ की संवेदनाओँ को सीधा छूते हैं. दिलों पर गहरी चोट करते और पीड़िता के प्रति उन की सहानुभूति जगाते हैं. जो कुछ गीत में सीता के लिए कहा जा रहा है, फ़िल्म में वह अभिनेत्री लीला चिटणीस पर घटित हो रहा है. गीत सीधे राम पर चोट कर रहा था. उसे अन्यायी क़रार दे रहा था. चेहरा पृथ्वीराज कपूर का था. सच कहें तो यही गीत आवारा फ़िल्म का मर्म था, उस का थीम सौंग था. यह गीत फ़िल्म को सीता बनवास और लवकुश प्रसंग की प्रतीक बना देता है.
मैं पूरी तरह विभोर था. मेरी तन्मयता राज से छिपी नहीँ थी. सीन ख़त्म हुआ तो राज ने बताया और पूछा, “अब तक किसी और ने भी यह सीन देखने की इच्छा प्रकट नहीँ की. तुम ने यह क्यों देखना चाहा.” राज की नज़र में अब तक मैं कोई अनोखी शै बन गया था. वह मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, मैँ उन्हें. मैं ने समझाने की कोशिश की, “आप की फ़िल्मों ने देश को जिस तरह की एक नई सामाजिक सोच दी है, उस का एक महत्वपूर्ण घटक है यह दृश्य. इसी दृश्य ने मेरी मानसिकता को गढ़ा है.”
मैं ने राज को यह भी बताया कि कई साल बाद जब मैं ने अपनी विवादास्पद कविता राम का अंतर्द्वंद्व लिखी तो उस के पीछे का बीज यह गीत ही था और थे शैक्सपीयर की संदेहग्रस्त डेस्डेमोना और अपने से जूझते हैमलेट का टु बी और नाट टू बी प्रश्न. राज कपूर और उन के साले प्रेमनाथ दोनों ही कुशल शैक्सपीरियन अभिनेता थे. निश्चय ही राज को मेरा मैयार मिल गया होगा. उस शाम के अंत में मुझे पता चला कि राज ने मुझे पूरी तरह अपना लिया था.
पता नहीँ क्योँ, साथ ही साथ मेरे मुँह से यह भी निकल गया कि अगर इस गीत ने मुझे बनाया तो एक और फ़िल्मी गीत ने मुझे ढहाया भी था. यह सुन कर राज कपूर के एक दम चेतन हो जाने का अंदाज़ा मुझे क़तई नहीँ था. सब कुछ भूल कर उन्हों ने पूछा कि यह दूसरा गीत क्या था.
मैं ने कहा, “साहिर लुधियानवी का गुरुदत्त की फ़िल्म प्यासा का अंतिम गीत, यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है.” गीतकार दुनिया के ऐब गिनाता रहता है. पूरी तरह शून्यवादी यह गीत पढ़तव्यं तब भी मरतव्यं नहीँ, न पढ़तव्यं तब भी मरतव्यं से आगे बढ़ कर पुकार पुकार कर हरएक से कह रहा था – कर्म निरर्थक है. यह संसार तुम्हारे कर्म के लायक़ है ही नहीँ. स्वयं जीवन ही व्यर्थ है.
मेरे लिए यह गीत ऐसे समय आया था जब सोवियत संघ में ख़्रुश्चोव रिपोर्ट के बाद कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्टों से मेरा मोह भंग हुआ था. रिपोर्ट तो वही कह रही थी, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहा था. क्रूरता से मेरी आँखें खोलने वाली असल बात यह थी कि वही कामरेड जो कभी मेरी स्टालिन-निंदा पर नाराज़ हो कर स्टालिन का घनघोर समर्थन करते थे, वही अब उस के उतने ही घनघोर निंदक बन गए थे. मैं पूरी समझ गया कि किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य बनने का मतलब है कठमुल्ला बनना, अपनी बुद्धि को किसी पेड़ पर टाँग आना. मास्को में बैठा नेता दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात. इस से अतिरिक्त तुम कुछ नहीं रह सकते.
प्यासा के इस नकारात्मक गीत ने मुझे गहरे अवसाद से तो भरा ही, एक अजीब शून्य में अधर लटका भी दिया था. मैं ने राज कपूर से कहा, “मैं अभी तक शून्य में हूँ. अपनी तलाश में हूँ.”
बात का रुख़ पलटने के लिए राज कपूर ने कहा, “अब मेरी किसी फ़िल्म का जो भी कोई और गीत सुनना चाहो तो कहो.” मैं श्री 420 का अपना बेहद पसंद गीत मेरा जूता है जापानी भी चुन सकता था. लेकिन मैं ने चुना प्यार हुआ इकरार हुआ. मेरी नज़र में यह गीत और इस में राज कपूर का नरगिस को अपनी छतरी के नीचे लेना भारतीय फ़िल्मों का सब से महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय बिंब है. प्रेमी का प्रेमिका का सहभागी बन जाना. आज भी इस दृश्य के बड़े फोटो रेस्तरानों में लगे मिलेंगे. जिस किसी किताब में फ़िल्मों के इतिहास से चित्र हैं, उस में यह दृश्य सब से अधिक दिखाई देता है. अपने जीवन से एक घटना लिखता हूँ. हम लोग नेपियन सी रोड पर एक सतमंज़िला इमारत में रहते थे. एक बरसाती दिन घर लौटते समय मैं ने नीचे की मंज़िल में रहने वाली श्रीमती वैद्य को अपनी छतरी में ले लिया. हम उस परिवार के लिए घनिष्ठ बन गए. यह था उस बिंब का जनमानस में बस जाने का प्रमाण.
मेरा वह चुनाव राज के प्रसन्न होने का कारण भी बन गया. गीत ख़त्म हुआ तो मैं कह बैठा, “जिस दिन से बंबई आया हूँ जहाँ कहीँ भी जाता हूँ तो वह जगह पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ यह गीत फ़िल्माया गया होगा.”
जवाब मिला, “यह स्टूडियो में बना सैट था.”
मैं अड़ गया. “नहीँ. उस में तो एक ट्रेन भी जाती है.”
राज एकदम बच्चों जैसे चहक उठे. कला निर्देशक आचरेकर को तलब किया गया कि मुझे उस सैट का मौडल दिखाएँ और बारीक़ियाँ समझाएँ. राज कपूर भी साथ थे. मैं ने देखे:
एक मिएचर सड़क… बिजली के छोटे छोटे खंबे जो धीरे धीरे अनुपात से और भी छोटे होते जा रहे हैं… कहीँ घास का मैदान, घास जैसे रंग का क़ालीन जैसा फ़र्श… उतार चढ़ाव… दूर दाहिनी ओर छोटी सी रेल पटरी… कहीँ कहीँ सिगनल हैं… वे ऊपर नीचे किए जा सकते हैं… क्षितिज रेखा… उस के रंग बदले जा सकते हैं… पटरी पर खिलौना टाइप की विशेष रेल… आदेश मिलते ही चलने लगती है… कभी कभी धुआँ भी छोड़ती है… छुक छुक करती है… रेल के डिब्बों में लाइटें जलती बुझती हैं.
पूरे बालसुलभ उत्साह से दोनों मुझे बारीक़ियाँ समझा रहे हैं. मैं चमत्कृत हूँ, फ़िल्म निर्माण का एक और पहलू समझ रहा हूँ. बरसात के दृश्योँ की लोकेशन शूटिंग नहीँ की जाती. वे हमेशा स्टूडियो में नक़ली बारिश कर के शूट किए जाते हैं. जब जिस ऐंगल से जो शौट चाहिए उस के अनुकूल प्रकाश व्यवस्था केवल इनडोर ही संभव है.
अब फिर हम आडिटोरियम में है. बातचीत निर्माणाधीन फ़िल्म संगम की हो रही है. पृष्ठभूमि के तौर पर मुझे बताया जाता है कि इस फ़िल्म का आइडिया राज कपूर को मेहबूब की फ़िल्म अंदाज़ में काम करते करते ही आया था. उस में भी राज कपूर दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहते थे. लेकिन दिलीप राज़ी नहीँ हुए. जब तक सही कलाकार न मिलें किसी कहानी पर फ़िल्म नहीँ बनानी चाहिए. आइडिया ताक़ पर रख दिया गया. अब राजेंद्र कुमार की अभिनय कला के विकास के साथ वह फिर उभर आया. संगम उसी का परिणाम है.
राज कपूर अब तक मुझ से आशवस्त हो चुके थे. पूरी तरह खुल गए थे. निस्संकोच बात कर रहे थे. मेरे सामने अब वह पूरी तरह खुली किताब थे. कभी वैजयंती माला की, कभी उन के प्रति अपने निजी रुझान की बात करते, कभी उस की शिकायत करते. बताया मैं ने (राज कपूर ने) वैजयंती से संगम की बातचीत शुरू की तो सीधा जवाब नहीँ मिला. एक बार मद्रास तार भेजा – संगम होगा कि नहीँ. तत्काल जवाब आया – होगा, होगा, होगा. राज ने बताया कि यह जवाब फ़िल्म संवाद के तौर पर शामिल कर लिया गया. शैलेंद्र ने इसी पर गीत भी लिखा – मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमना का – बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीँ. कई बातें उन दोनों के निजी संबंध की थीँ. वे मैं ने न वह किसी को बताईं या लिखीं, न अब लिखूँगा. फ़िल्मी कलाकार अकसर हम से बेहद निजी बातें कर बैठते हैं. मेरी और माधुरी ने हमेशा इतना संयम बरता कि वे उजागर न करें.
राज कहे जा रहे थे, “अब फिर वैजयंती मद्रास जा बैठी है. शूटिंग पर आने से आनाकानी कर रही है. सभी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं. पहले हाँ कर देती हैं, फिर आनाकानी, किंतु परंतु, बहानेबाज़ी करती रहती हैं.”
इस सब से मैं सीख रहा था कि शूटिंग के लिए सभी प्रमुख कलाकारों की डेट (शूटिंग का समय) मिलना आसान नहीँ होता. निर्माता या निर्देशक को उन के नख़रे सहने को तैयार रहना पड़ता है.
उस शाम पहले तो मैं ने फ़िल्म संपादन क्या होता है, कैसे किया जाता है, और संप्रेषण को प्रबलित करने में उस की क्या भूमिका होती है – यह जाना था. जुलुम सहे भारी में संपादक ने विभिन्न शौटों को एक के बाद एक कैसे रखा था, उस क्रम से गीत के भाव दर्शक को वांछित रूप से प्रभावित करने में सफल थे.
यह भी सीखा कि कोई कितना ही बड़ा हो, फ़िल्मों में है तो भीतर से वह किसी भी कवि या चित्रकार जैसा ही कलाकार है, संवेदनशील इनसान है. सच्ची प्रशंसा का भूखा है. ख़ुशामद की उसे गहरी पहचान है. कौन ऊपरी बात कर रहा है, कौन दिल से – यह वह आसानी से पहचान लेता है.
पता नहीँ कैसे, किस के इशारे से, अब शैलेंद्र भी हमारे साथ थे, और हम दोनों राज कपूर से विदा ले रहे थे. हम चलने लगे तो राज ने मुझ से कहा, “तुम शैलेंद्र के दोस्त हो. मेरा दर तुम्हारे लिए चौबीस घंटे खुला है.” जन्म और स्वभाव से पठान राज कपूर ने अपना यह वचन जब तक मुझ से संबंध रहा, हर दम हर घड़ी निभाया. जब भी मैं ने फ़ोन किया, वह मिले. कभी बिना बताए किसी काम से आर. के. स्टूडियो जाना हुआ तो पता नहीँ कैसे राज तक समाचार पहुँच जाता और मुझे उन की निजी काटेज में बुला लिया जाता. उन के दिल की प्रियतम फ़िल्म मेरा नाम जोकर की समीक्षा में मैं ने बखिया उधेड़ दी. वह नाराज़ नहीँ हुए. वह जानते थे, जो कुछ मैं ने लिखा है ईमानदारी से लिखा है.
1978 में जब मैं माधुरी से जुदा हो कर दिल्ली वापस लौट रहा था, तो मेरी अपनी देखरेख में बने अंतिम अंक में मैं ने अपने दोनों हीरो का अभिनंदन किया. पाठकों से बिदाई लेते अपने संदेश में मैं ने शैलेंद्र के दो गीतों से उद्धरण दिए. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तो, यह दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तो. और अंत में हम तो जाते अपने गाम, सब को राम राम राम. यह अभिनंदन पाने वाले शैलेंद्र तब तक हम सब से जुदा हो चुके थे. और राज कपूर को मुखपृष्ठ पर सजाया – एक सजावटी फ़ोटोफ़्रेम के भीतर उन का क्लोज़अप और भीतर उन पर एक लेख. पता नहीं मेरा यह अभिनंदन वह समझे या नहीं. अब वह भी हमारे बीच नहीँ हैँ, जो उन से पूछ पाऊँ.
दिन 2 – 1966 - मैँ ने देखे दो राज कपूर
मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है. 14 दिसंबर 1966 – राज कपूर का जन्मदिन. उस दिन राज कपूर की आत्मा जाती रही थी. और राज कपूर का हैरान खड़ा शरीर ताक रहा था उन पार्थिव अवशेषों को जो मुंबई में कोलाबा के एक छोटे से नर्सिंग होम में धरती पर रखे थे. ये अवशेष थे लोककवि और फ़िल्म गीतकार शैलेंद्र के. मुझे लगा जो खड़ा है और जो पड़ा है – जो है और जो चला गया है – वह एक ही है.
जो खड़ा था, वह था राज कपूर – अभिनेता. जो चला गया था, वह था – शैलेंद्र. राज कपूर के माध्यम से पूरे संसार के होंठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत आवारा हूँ और सामान्य आधुनिक भारतीय की पहचान बताने वाले गीत मेरा जूता है जापानी…फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का शब्दकार.
महीनों पहले से शैलेंद्र का जिगर काम करना बंद करता आ रहा था. धीरे धीरे उन के जीवन का रस सूखता जा रहा था. सब को अच्छी तरह पता था कि शैलेंद्र किसी भी दिन, किसी भी क्षण जा सकते हैं. फिर भी उन के जाने पर राज कपूर को जैसे यक़ीन नहीं हो रहा था. यक़ीन मुझे भी नहीं हो रहा था…
कुछ घंटे बाद –
उपनगर खार में उन के बंगले रिमझिम के अहाते में, बाहर गली में, भीड़ जमा होती जा रही थी. जैसे पूरा फ़िल्म उद्योग उमड़ता आ रहा हो. शैलेंद्र पहली मंज़िल पर रहते थे. नीचे अहाते में जो एक छोटा सा कमरा अलग थलग था, वहाँ शैलेंद्र को लिटाया गया था.
मेरे नाम की पुकार उठी. उन्हें अंतिम स्नान कराना था – मुझे और बासु भट्टाचार्य को. मैं – उन दिनों उन का घनिष्ठतम मित्र और समर्थक. बासु भट्टाचार्य – उन की फ़िल्म तीसरी क़सम का निर्देशक. बासु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ थीं. उन में से कई उस छोटे से कमरे में शैलेंद्र को स्नान कराते समय मुझे याद आ रही थीं.
अब बासु भी नहीं हैं. उन के बारे में कुछ कहना अनुचित लग सकता है. पर शैलेंद्र के बारे में लिखना हो, और बासु के बारे में कुछ न कहा जाए, और वह साफ़ साफ़ न कहा जाए जो मेरी जानकारी के अनुसार तब पूरा सच था और अब तक है, तो उस क्षण मेरे मन में जो विचार थे, उन का सही चित्रण न होगा.
बासु को निर्देशक बनाने के लिए ही शैलेंद्र ने तीसरी क़सम बनाने का फ़ैसला लिया था. (बिमल दा की बेटी रिंकी से बासु के प्रेम प्रसंग और अंत में विवाह तक में बासु के पक्ष में शैलेंद्र की सक्रिय भूमिका रही थी. यहाँ तक कि शादी के बाद नवदंपति को शैलेंद्र ने सांताक्रुज़ पूर्व में रेलवे स्टेशन के निकट अपने ही एक फ़्लैट में टिकाया भी था. बहुत बाद मेँ एक बार दिल्ली मेँ अचानक मुलाक़ात होने पर रिंकी ने मुझे बताया था कि बासु अक़सर रिंकी को बड़ी क्रूरता से पीटता भी था.)
फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कथा का चुनाव शैलेंद्र का अपना था. कोमल भावों वाली एक नन्हीं सी कहानी जिस में गाँव का गाड़ीवान हीरामन (राज कपूर) अपनी टप्पर वाली गाड़ी में मेले की ओर ले जा रहा है नौटंकी कंपनी की नर्तकी (वहीदा रहमान) को, और अपने भोलेपन में उसे कन्या सुकुमारी और देवी समझता है. कहानी में तथाकथित बंबइया नुस्ख़े नहीं थे. ऐसा नहीं है कि इस तरह की भावप्रधान कहानियों पर बंबई में बनी फ़िल्में सफल न होती रही हों.
लेकिन शुरू से ही तीसरी क़सम को और शैलेंद्र को मुसीबतों का सामना करना पड़ा. सफलता और असफलता की बात तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद आती है. लेकिन जो फ़िल्में बनते बनते अटक जाती हैं, घिसटते घिसटते पूरी होती हैं, और इस कारण जिन पर होने वाला ख़र्चा अनुमान से कई गुना बढ़ जाता है, वे बाक्स आफ़िस पर सफल हों तो भी निर्माता के लिए घाटे का ही सौदा रहती हैं. तीसरी क़सम के साथ यह होना तय हो चुका था.
फ़िल्म उद्योग में यह चर्चा आम थी कि जो रुकावटें इस फ़िल्म के बनने में आईं, उन में से अधिकतर की ज़िम्मेदारी बासु के कंधों पर थी. मेरी निजी धारणा भी कुछ ऐसी ही थी. यूँ किसी फ़िल्म का सही बन पाना, बिकना, और चलना – इन पर किसी का बस नहीं होता. एक तो कवि शैलेंद्र फ़िल्म व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं थे, दूसरे, वितरकों से बासु की दंभितापूर्ण बहसें उन्हें भड़का देती थीं. वितरकों के दृष्टिकोण से तो पूरा प्रपोज़ल अनार्थिक और अयथार्थवादी था. बड़े बड़े सितारों के कारण फ़िल्म बड़े बजट की थी. लेकिन अनजान और असिद्ध निर्देशक के कारण उस का मूल्य ज़ीरो था. बासु ने इस से पहले जो एक दो डाक्यूमेंटरी बनाना शुरू की थीं, वॆ भी पूरी नहीं हो पाई थीं. और शैलेंद्र को ज़िद थी कि कोई यह फ़िल्म निर्देशित करेगा तो बासु भट्टाचार्य. बिमल राय की फ़िल्म मधुमती के गीत शैलेंद्र ने लिखे थे, और उस में बासु एक सहायक था. वह अपने ऊँचे ऊँचे सपने सब को सुनाता था, और शैलेंद्र को महान संभावनाओं से भरपूर नौजवान नज़र आता था.
जो लोग तीसरी क़सम में बासु के साथ सहायक थे – बासु चटर्जी, बाबूराम इशारा – तथा यूनिट के अन्य सदस्य, वे लोग कहते रहते थे कि बासु को अपने काम पर अधिकार नहीं था, अक़सर वह बिना तैयारी के आते थे. आरोप यहाँ तक होते थे कि बासु को चिठिया हो तो हर कोई बाँचे गीत के शब्दार्थ तक पता नहीं थे. अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दृश्य रूप बासु अपनी कल्पनाशीलता के महान उदाहरणों के तौर पर मुझे सुनाया करते थे, उन में से अधिकांश कैमराबद्ध नहीं किए जा सकते थे, और न ही किए जा सके. जो आंचलिकता तीसरी क़सम की कहानी में है – उसे न तो बासु समझते थे, न वह उसे आत्मिक सौंदर्य से रंजित कर के परदे पर उतार पाए. अक़सर दोष वह इस बात पर मँढते थे कि राज कपूर हीरामन नहीं लगते. कभी कभी ऐसे ही आरोप वहीदा पर भी लगाते थे. यह अपनी अपनी नज़र का फ़र्क़ है. लेकिन जब निर्देशक फ़िल्म की कास्टिंग से सहमत नहीं है, तो उसे अपने आप को उस से अलग कर लेना चाहिए. कई बार बासु मुझ से शैलेंद्र के उन निकट समर्थकों की निंदा करते थे, जो शैलेंद्र के सच्चे मित्रों और सहायकों में से थे.
कई कई महीने तीसरी क़सम की शूटिंग बंद रहती थी – कभी अर्थाभाव में, कभी आपसी मनमुटाव में. अक़सर सुबह की सैर पर गायक मुकेश से मेरी मुलाक़ात हैंगिंग गार्डन में होती थी, जहाँ मैं भी सपरिवार जाया करता था. तीसरी क़सम और शैलेंद्र पर जो संकट के बादल मँडरा रहे थे, उन से मुकेश त्रस्त रहते थे. जब शैलेंद्र में दम नहीं रहा झंझटों से निपटने का, तो उन के गहरे शुभचिंतकों ने – मुकेश और राज कपूर ने – मामला अपने हाथ में ले लिया. बजट के अभाव में कामचलाऊ शूटिंग कर के, संपादन राज कपूर ने अपने आप किया आर.के. स्टूडियो में (कौन सा टुकड़ा कहाँ का है, पता नहीं चलता था) जैसे तैसे तीसरी क़सम को रूप दिया गया. मुझे याद है कि उस का अंतिम संस्करण शैलेंद्र और मैं ने राज कपूर के साथ आर.के. के प्रीव्यू थिएटर में देखा था. हम दोनों सहमत थे कि जिन हालात में जहाँ तक पहुँचे हैं, उन में इस से बहुत आगे जा भी नहीं सकते थे.
इसी प्रीव्यू थिएटर में शैलेंद्र ने राज कपूर से मेरी पहली मुलाक़ात कराई थी… (बयोरा इस लेख के पूर्वार्ध मेँ है.)
शैलेंद्र आम आदमी के मन की पुकार को बड़े सहज शब्दों में एक ऐसा आयाम देते थे, जो गहरे अर्थ वाला हो, और दिल की बात करता हो और दिल से दिल तक पहुँचता हो. वही थे जो कह सके – छोटी सी बात न मिर्च मसाला दिल की बात सुने दिल वाला. वही थे जो गा सके – हम भी हैं, तुम भी हो आमने सामने… वही थे जो नायिका से दिल का सौदा इन शब्दों में कर पाए – देती है दिल दे बदले में दिल ले. और वही थे जो इतने कम शब्दों में पूरे देश के सांस्कृतिक परिवेश का बयान कर सके – हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. उसी मेँ शैलेंद्र ने कोरे बुद्धिजीवियोँ पर तीखा कमैंट किया था – जो लोग जो ज़्यादा जानते हैँ – इनसान को कम पहचानते हैँ.
अरथी को पहला कंधा आरके यानी राज कपूर की टीम ने दिया. यह उन्हीँ का हक़ था और कर्तव्य भी. और यह दिन था राज कपूर का जन्म दिन 14 दिसंबर जब उस अनमोल माला का पहला मनका टूट गया.
वहाँ कौन है तेरा, मुसाफ़िर, गया है तू जहाँ
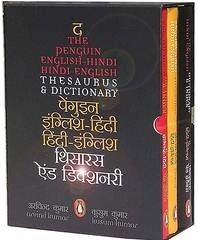


Comments