हिंदी वालोँ ने अपने अहंकार मेँ इल्मी और फ़िल्मी जैसे मुहावरे गढ़ कर जनमानस मेँ अजीब और ग़लत समझ पैदा कर दी. फ़िल्म को घटिया और रद्दी कला मान कर ख़ारिज़ कर दिया, जब कि फ़िल्म पिछली सदी मेँ उभरी ऐसी सर्वांग संपूर्ण कला है जैसी इस से पहले कभी नहीँ देखी गई. कुशल निर्माता निर्देशक के हाथ से ऐसी चीज़ निकलती है जो पूरे समाज को, देश को बदल सकती है.
अच्छी फ़िल्मोँ की संख्या कम नहीँ है. जैसे हर प्रकाशित पुस्तक उच्च कोटि का साहित्य नहीँ होती, वैसे ही हर फ़िल्म उच्च कोटि की नहीँ होती.
माधुरी नाम की फ़िल्म पत्रिका का आरंभ और संपादन करने मैँ बंबई पहुँचा 1963 के अंत मेँ. पहले ही कुछ दिनों मेँ मैँ ने तीसरी क़सम के निर्माता रूप मेँ कवि शैलेंद्र के जीवन के अंतिम तीन साल का कठिन संघर्ष बेहद पास से देखा. देखा कैसे भावुक कवि व्यवसाय की पेचीदगियाँ न समझ पाने के कारण अवश्यंभावी दुःखांत की ओर बढ़ रहा था.
रेणु जी की कहानी पर फ़िल्म बनाना शैलेंद्र की अपनी पसंद और ज़िद थी. कुछ और ज़िदें भी थीँ—
1) हीरामन के लिए राज कपूर का चयन (एक रुपया ले कर काम करने वाले राज कपूर ने अपने आप को पूरी तरह हीरामन बना लिया था),
2) बासु भट्टाचार्य को फ़िल्म का निर्देशक बनाना (जो व्यवसाय बुद्धि के बिल्कुल विपरीत था; राज कपूर जैसे बिकाऊ हीरो और वहीदा रहमान जैसी बिकाऊ हीरोइन, शैलंद्र और हसरत जयपुरी जैसे बिकाऊ गीतकारोँ, शंकर जयकिशन जैसे बिकाऊ संगीतकारोँ के साथ अज्ञात क्षमता वाला निर्देशक फ़िल्म की ऊँची मार्केट वैल्यु को ज़ीरो कर देता था). बासु मेँ स्वभावगत ख़ामियाँ भी थीँ. अपने को दुनिया का सब से बड़ा बौद्धिक समझना, राज कपूर से पटरी न बैठा पाना, डिस्ट्रीब्यूटरोँ को नीचा दिखा कर नाराज़ करना… और
3) फ़िल्म कैसे मैनेज की जाती है, फ़ाइनैंस कैसे किन शर्तोँ पर लिया जाता है, कर्ज़ देने वालोँ से कैसे भुगता जाता है आदि मेँ शैलेंद्र निपट अनाड़ी थे.
फ़िल्म बार बार अटक जाती, धक्के मार कर चलाई जाती, फिर रुक जाती. मुझे पता है कि अंत मेँ गायक मुकेश के इसरार पर किस तरह राज कपूर ने फ़िल्म के शूट किए गए सारे बेतरतीब टुकड़े अपने हाथोँ मेँ कर लिए, दिन रात एक कर के आर.के. स्टूडियो मेँ उन्हेँ कुछ रूप आकार ढंग दे कर अंतिम रूप दिया. आर.के. के प्रीव्यु थिएटर मेँ संपूर्ण फ़िल्म के शो मेँ इस शाम शैलेंद्र के साथ मैँ भी था. तितरबितर माल को राज ने उसे एक उत्कृष्ट कृति बना दिया था. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरोँ ने अपनी लागत जैसे तैसे भुनाने की कोशिश मेँ मूर्खतावश बिना किसी प्रचार के, बिना एक भी विज्ञापन दिए, दिल्ली मेँ गोलचा मेँ रिलीज़ कर दिया. हाल ख़ाली होने पर एक ही शो के बाद उतार भी दिया! फ़िल्म को फ़्लाप मान लिया गया. फ़िल्म तो गई ही, शैलेंद्र को ले साथ ले गई. ”96 की 14 दिसंबर की सुबह कोलाबा के नर्सिंग होम मेँ शकुंतला भाभी सूनी आँखोँ से शैलेंद्र का लेटा शव ताक रही थीँ, अवसन्न राज कपूर ऐसे खड़े थे जैसे ज़मीन पर वह स्वयं लेटे होँ.
बाद मेँ तो फ़िल्म ख़ूब चली. अब तक टीवी चैनलोँ पर दिखाई जाती है. उस के गीत सदाबहार सिद्ध हुए और आय का निरंतर स्रोत बने. लेकिन तब जब शैलेंद्र नहीँ रहे.
दोष न सिनेमा का, न साहित्य का
इस दुःखांत मेँ न सिनेमा का कोई दोष था, न निर्माता का, न साहित्य का. सिनेमा तो साहित्य को ससम्मान अपने से जोड़ रहा था. फिर भी ऐसी ही अन्य अनेक घटनाओँ के आधार पर (जैसे तीसादि दशक मेँ मुंशी प्रेमचंद का बुलाए जाने पर बंबई जाना, कुछ ही महीनों मेँ उकता झुँझला कर वापस लौट आना) हिंदी वालोँ ने अपने अहंकार मेँ इल्मी और फ़िल्मी जैसे मुहावरे गढ़ कर जनमानस मेँ अजीब और ग़लत समझ पैदा कर दी. फ़िल्म को घटिया और रद्दी कला मान कर ख़ारिज़ कर दिया, जब कि फ़िल्म पिछली सदी मेँ उभरी ऐसी सर्वांग संपूर्ण कला है जैसी इस से पहले कभी नहीँ देखी गई. कुशल निर्माता निर्देशक के हाथ से ऐसी चीज़ निकलती है जो पूरे समाज को, देश को बदल सकती है. (सब जानते हैँ कि बाद मेँ स्वयं प्रेमचंद जी की रचनाओँ पर दो बैलोँ की जोड़ी जैसी स्मरणीय फ़िल्में बनीँ.) नए नारे दे सकती है. हाल ही की लगे रहो मुन्ना भाई, चक दे इंडिया, पचास साल पहले की श्री चार सौ बीस, जागते रहो, दो बीघा ज़मीन, प्यासा, मदर इंडिया, साठ सत्तर साल पहले की अछूत कन्या, आदमी, औरत, दुनिया न माने को ऐसी ही फ़िल्मोँ मेँ गिना जा सकता है. साथ ही साथ फ़िल्म समाज को स्वस्थ मनोरंजन भी देती है. अनाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, हम आप के हैँ कौन जैसी रोचक सुरुचुपूर्ण फ़िल्मोँ के उदाहरण असंख्य हैँ. इन मेँ हम आप के हैँ कौन और उस का पुराना रूप नदिया के पार तो एक ही साहित्यिक कथा के दो भिन्न अवतार हैँ.
जैसे शुरू से ही नाटक साहित्य का अंग माना जाता रहा है, वैसे ही सिनेमा (और उस के साथ साथ रेडियो नाटक, फ़िल्म, टीवी सीरियल आदि) लेखन को भी साहित्य की विधाएँ मान लिया जाना चाहिए था. बँगला मेँ तो सिनेमा को कहा ही बोई (पुस्तक) जाता है. जैसे नाटक की तकनीक उपन्यास या महाकाव्य की तकनीक से अलग होती है, वैसे ही फ़िल्म की तकनीक नाटक और उपन्यास आदि से अलग होती है. यह बात कोरा लेखक नहीँ समझता. इसी प्रकार फ़िल्म गीत साहित्यिक गीत से भिन्न होता है. अच्छा गीतकार अच्छा फ़िल्म गीतकार बने यह आवश्यक नहीँ है. आजकल साहित्यकार गुलज़ार, जावेद ने, पहले कवि प्रदीप, जोश मलीहाबादी, साहिर लुधियानवी, मजरूह, नीरज और शैलेंद्र ने सफल फ़िल्म गीत लिखे और ख़ूब चले.
बात यह है ही नहीँ कि किसी पूर्वलिखित रचना पर फ़िल्म बनी है या फ़िल्म के लिए कहानी लिखी गई है. बात है कि अंतिम रूप मेँ फ़िल्म कितनी सुरुचिपूर्ण, साहित्यिक है, उस मेँ कितना आकर्षण है, दर्शक को प्रभावित करने की, उस का मन छूने की ताक़त है या नहीँ. है, तो फ़िल्म को सफल होने से कोई रोक नहीँ सकता–चाहे वह कैसी ही फ़िल्म हो. ख़्बाजा अहमद अब्बास ने अपनी कहानियोँ पर अपने आप जो फ़िल्में बनाईं वे सब असफल रहीँ, राज कपूर ने उन्हीं की कहानियोँ पर जितनी बनाईं वे सब महान और सफल साबित हुईं. प्रकाशित साहित्य पर बनीं सफल फ़िल्मोँ मेँ देवदास, चित्रलेखा, साहब बीबी ग़ुलाम, ओमकारा आदि असंख्य फ़िल्मोँ को गिना जा सकता है. (ओमकारा को मैँ संसार भर मेँ शैक्सपीयर के नाटकोँ पर बनी सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मोँ में गिनने मेँ भी नहीँ हिचकूँगा.) शरच्चंद्र तो फ़िल्मोँ के लिए कहानियोँ का अनंत स्रोत रहे हैँ.
अच्छी फ़िल्मोँ की संख्या कम नहीँ है. जैसे हर प्रकाशित पुस्तक उच्च कोटि का साहित्य नहीँ होती, वैसे ही हर फ़िल्म उच्च कोटि की नहीँ होती.
❉❉❉
आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ
©अरविंद कुमार
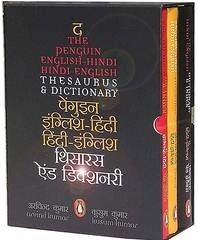
Comments