जितना बड़ा सिनेमाघर होता, उतने ही ज्यादा दर्शकोँ की दरकार होगी. जितने ज़्यादा दर्शक फ़िल्म को सफल करने के लिए चाहिएँ, उतनी ही उन लोगोँ की पसंद पर हमारी फ़िल्म की विषयवस्तु निर्भर करेगी.
अभी हाल मेँ चौंकाने वाले आँकड़े सामने आए. फ़िल्मोँ के बाक्स आफ़िस कलक्शन मेँ मल्टीप्लैक्स सिनेमाओं का योगदान 35 प्रतिशत से ऊपर है, जब कि कुल सिनेमाघरोँ की संख्या (लगभग 12 हज़ार) मेँ मल्टीप्लैक्स कुल दो प्रतिशत के आसपास हैं.
आरंभ मेँ ही इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना इस लिए ज़रूरी था कि फ़िल्मोँ की विषयवस्तु पर और उन की शैली पर इस का सीधा असर पड़ता है.
कलाकार/फ़िल्म निर्माता/निर्देशक लगातार जैसी चाहेँ वैसी फ़िल्मेँ नहीँ बनाते रह सकते. फ़िल्म कोई कहानी या लेख नहीँ है कि हम घर बैठे लिख लेँ. रुपए पैसे के मामले मेँ उस की कुल लागत काग़ज़ और स्याही की क़ीमत जितनी होती है. हाँ, जब उसे प्रकाशित करने की बात आएगी, तो लागत एकदम कई गुना बढ़ जाएगी. इसी प्रकार फ़िल्म की परिकल्पना और उस का आलेख होता है. हमारे कल्पना मेँ हम ने कितनी ही शानदार, बेहतरीन, आला कृति न सोच डाली हो, उस का फ़िल्मांकन भारी लागत के बग़ैर नहीँ हो सकता. इसी बात को एक और तरीक़े से कहेँ तो आप कितने ही कल्पनाशील स्थपति न होँ, आप के मन किसी ताज महल की तस्वीर क्यों न हो. आप वह ताज महल तब तक नहीँ बना सकते जब तक कोई शाहजहाँ उन से निर्माण पर पैसा बहाने के लिए उतारू न हो.
फ़िल्मोँ के संदर्भ मेँ इस बात को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं. हमारे पास अच्छी पटकथा है, निर्देशक है, निर्माता है जो पैसा बहाने के लिए तैयार है. लेकिन वह और आप अकेले कमरे मेँ बैठ कर तो अपनी फ़िल्म नहीँ देखेँगे ना? आप को दर्शक चाहिए. दर्शक सिनेमाघर मेँ आएगा. अगर फिल्म से बड़ा मुनाफ़ा कमाना हमारा उद्देशय नहीँ, तो इतना तो फिर भी है कि सिनेमाघर चलाने का ख़र्चा दर्शकोँ के निकल आए. इस के लिए कम के कम इतने तो दर्शक हमारी फ़िल्म देखने आने चाहिएँ, जिन के टिकट की लागत से उस का बिजली का, स्टाफ़ की तनख़ा का ख़र्चा निकल आए. फिर सिनेमा के मालिक को अपनी लागत पर कुछ तो लाभ मिलना ही चाहिए, है कि नहीँ? यदि हम अपनी फ़िल्म को बड़े स्तर पर चलाना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगोँ तक पहुँचे, तो हमेँ कई सप्ताह तक स्निेमाघर को दर्शकोँ से खचाखच भरना पड़ेगा.
बस, इसी बात पर निर्भर करती है हमारी फिल्म की विषयवस्तु. जितना बड़ा सिनेमाघर होता, उतने ही ज्यादा दर्शकोँ की दरकार होगी. जितने ज़्यादा दर्शक फ़िल्म को सफल करने के लिए चाहिएँ, उतनी ही उन लोगोँ की पसंद पर हमारी फ़िल्म की विषयवस्तु निर्भर करेगी.
अब हम पुराने टाइप के सिनेमाघरोँ की बात करें. बड़े शहरोँ के ही नहीँ, छोटे क़स्बों के सिनेमाघरो की भी… कुरसियाँ बैंचें टूटी फूटी होती हैं. छत से लटकते पंखे जब कभी चलते हैं तो फ़िल्म के संगीत मेँ चूँ चूँ के सुर और मिला देते हैं. यहाँ आम तौर पर थके माँदे करखनदार मज़दूर दिन भर की थकान या जीवन की ऊब से निजात पाने आते हैं. इन्हें हमारे ज़माने मेँ चवन्नी क्लास कहा जाता था. मध्यम वर्ग के या पढ़े लिखे लोग भी उसी सिनेमाघर मेँ थोड़े से ऊँचे दरजे मेँ बैठते हैं. वहाँ भी हालत कुछ बेहतर नहीँ होती. जब कभी बिजली फ़ेल हो जाने पर प्रोजैक्शन मशीन बंद हो जाती है तो सीटियाँ बजने लगती हैं. ज़रा भी रोमांटिक सीन आया या कहीँ हीरइन या वैंप ने कपड़े थोड़ से ऊपरकिए तो फिर सीटियाँ बजने लगहती हैं. पहले तो लोग इकन्नी दुअन्नी भी परदे की तरफ़ फेंकने लगते थे.
अब आप बताइए कि क्या यहाँ सत्यजित राय की 1955 मेँ बनी फ़िल्म पथेर पांचाली जैसी फ़िल्म देखी जा सकती है? यह भारत मेँ नए सिनेमा की पहली उल्लेखनीय फ़िल्म मानी जाती है. यह भी नहीँ है कि इस से पहले अच्छी फ़िल्मेँ नहीँ बनती थीं.
आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ
©अरविंद कुमार
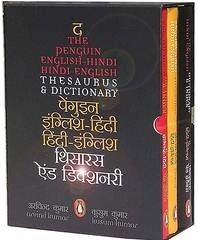
Comments