सूफ़ी मार्क्सवादी
इसी टीम के शेष सदस्योँ ने शैलेँद्र की अरथी को सब से पहले कंधा दिया. यह उन्हीँ का अधिकार था. इस टीम की अलग पहचान यह थी कि यह बौद्धिक होते हुए भी दिल से सोचती थी, दिल से काम करती थी, और दिलोँ तक पहुँचना चाहती थी. इस का गणित दिल का था.
© अरविंद कुमार
देखिए शैलेंद्र पर एक और लेख
मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है. वह दिन था १४ दिसंबर – राज कपूर का जन्मदिन.
उस दिन राज कपूर की आत्मा जाती रही थी. और राज कपूर का हैरान खड़ा शरीर ताक रहा था उन पार्थिव अवशेषों को जो मुंबई मेँ कोलाबा के एक छोटे से नर्सिंग होम मेँ धरती पर रखे थे. ये अवशेष थे लोककवि और फ़िल्म गीतकार शैलेँद्र के. मुझे लगा जो खड़ा है और जो पड़ा है – जो है और जो चला गया है – वह एक ही है.
जो खड़ा था, वह था राज कपूर – अभिनेता. जो चला गया था, वह था – शैलेँद्र. राज कपूर के माध्यम से पूरे संसार के होंठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत आवारा हूँ और सामान्य आधुनिक भारतीय की पहचान बताने वाले गीत मेरा जूता है जापानी… फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का शब्दकार.
महीनोँ पहले से शैलेँद्र का जिगर काम करना बंद करता आ रहा था. धीरे धीरे उन के जीवन का रस सूखता जा रहा था. सब को अच्छी तरह पता था कि शैलेँद्र किसी भी दिन, किसी भी क्षण जा सकते हैँ. फिर भी उन के जाने पर राज कपूर को जैसे यक़ीन नहीँ हो रहा था. यक़ीन मुझे भी नहीँ हो रहा था…
मैँ हैरान था
उपनगर खार मेँ उन के बंगले रिमझिम के अहाते मेँ, बाहर गली मेँ, भीड़ जमा होती जा रही थी. जैसे पूरा फ़िल्म उद्योग उमड़ता आ रहा हो. शैलेँद्र पहली मंज़िल पर रहते थे. नीचे अहाते मेँ जो एक छोटा सा कमरा अलग थलग था, वहाँ शैलेँद्र को लिटाया गया था.
मेरे नाम की पुकार उठी. उन्हेँ अंतिम स्नान कराना था – मुझे और बासु भट्टाचार्य को. मैँ – उन दिनोँ उन का घनिष्ठतम मित्र और समर्थक. बासु भट्टाचार्य – उन की फ़िल्म तीसरी क़सम का निर्देशक. बासु के बारे मेँ अनेक किंवदंतियाँ थीँ. उन मेँ से कई उस छोटे से कमरे मेँ शैलेँद्र को स्नान कराते समय मुझे याद आ रही थीँ.
अब बासु भी नहीँ हैँ. उन के बारे मेँ कुछ कहना अनुचित लग सकता है. पर शैलेँद्र के बारे मेँ लिखना हो, और बासु के बारे मेँ कुछ न कहा जाए, और वह साफ़ साफ़ न कहा जाए जो मेरी जानकारी के अनुसार तब पूरा सच था और अब तक है, तो उस क्षण मेरे मन मेँ जो विचार थे, उन का सही चित्रण न होगा.
मैँ हैरान था – बासु के उस कोमल स्पर्श के बारे मेँ जिस से वह इस अंतिम स्नान का निर्देशन कर रहा था और शैलेँद्र के शरीर को छू रहा था. बासु को निर्देशक बनाने के लिए ही शैलेँद्र ने तीसरी क़सम बनाने का फ़ैसला लिया था. (बिमल दा की बेटी रिंकी से बासु के प्रेम प्रसंग और अंत मेँ विवाह तक मेँ बासु के पक्ष मेँ शैलेँद्र की सक्रिय भूमिका रही थी. यहाँ तक कि शादी के बाद नवदंपति को शैलेँद्र ने सांताक्रुज़ पूर्व मेँ रेलवे स्टेशन के निकट अपने ही एक फ़्लैट मेँ टिकाया भी था.)
फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कथा का चुनाव शैलेँद्र का अपना था. कोमल भावोँ वाली एक नन्हीँ सी कहानी जिस मेँ गाँव का गाड़ीवान हीरामन (राज कपूर) अपनी टप्पर वाली गाड़ी मेँ मेले की ओर ले जा रहा है नौटंकी कंपनी की नर्तकी (वहीदा रहमान) को, और अपने भोलेपन मेँ उसे कन्या सुकुमारी और देवी समझता है. कहानी मेँ तथाकथित बंबइया नुस्ख़े नहीँ थे. ऐसा नहीँ है कि इस तरह की भावप्रधान कहानियोँ पर बंबई मेँ बनी फ़िल्में सफल न होती रही हों.
लेकिन शुरू से ही तीसरी क़सम को और शैलेँद्र को मुसीबतोँ का सामना करना पड़ा. सफलता और असफलता की बात तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद आती है. लेकिन जो फ़िल्में बनते बनते अटक जाती हैँ, घिसटते घिसटते पूरी होती हैँ, और इस कारण जिन पर होने वाला ख़र्चा अनुमान से कई गुना बढ़ जाता है, वे बाक्स आफ़िस पर सफल हों तो भी निर्माता के लिए घाटे का ही सौदा रहती हैँ. तीसरी क़सम के साथ यह होना तय हो चुका था.
फ़िल्म उद्योग मेँ यह चर्चा आम थी कि जो रुकावटेँ इस फ़िल्म के बनने मेँ आईँ, उन मेँ से अधिकतर की ज़िम्मेदारी बासु के कंधों पर थी. मेरी निजी धारणा भी कुछ ऐसी ही थी. यूँ किसी फ़िल्म का सही बन पाना, बिकना, और चलना – इन पर किसी का बस नहीँ होता. एक तो कवि शैलेँद्र फ़िल्म व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीँ थे, दूसरे, वितरकोँ से बासु की दंभितापूर्ण बहसेँ उन्हेँ भड़का देती थीँ. वितरकोँ के दृष्टिकोण से तो पूरा प्रपोज़ल अनार्थिक और अयथार्थवादी था. बड़े बड़े सितारोँ के कारण फ़िल्म बड़े बजट की थी. लेकिन अनजान और असिद्ध निर्देशक के कारण उस का मूल्य ज़ीरो था. बासु ने इस से पहले जो एक दो डाक्यूमेँटरी बनाना शुरू की थीँ, वॆ भी पूरी नहीँ हो पाई थीँ. और शैलेँद्र को ज़िद थी कि कोई यह फ़िल्म निर्देशित करेगा तो बासु भट्टाचार्य. बिमल राय की फ़िल्म मधुमती के गीत शैलेँद्र ने लिखे थे, और उस मेँ बासु एक सहायक था. वह अपने ऊँचे ऊँचे सपने सब को सुनाता था, और शैलेँद्र को महान संभावनाओँ से भरपूर नौजवान नज़र आता था.
1 बाएँ तीसरी क़सम मेँ राज कपूर और वहीदा रहमान – दाहिने फ़िल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और शैलेंद्र
जो लोग तीसरी क़सम मेँ बासु के साथ सहायक थे – बासु चटर्जी, बाबूराम इशारा – तथा यूनिट के अन्य सदस्य, वे लोग कहते रहते थे कि बासु को अपने काम पर अधिकार नहीँ था, अकसर वह बिना तैयारी के आते थे. आरोप यहाँ तक होते थे कि बासु को चिठिया हो तो हर कोई बाँचे गीत के शब्दार्थ तक पता नहीँ थे. अपने निजी अनुभव के आधार पर मैँ यह ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दृश्य रूप बासु अपनी कल्पनाशीलता के महान उदाहरणोँ के तौर पर मुझे सुनाया करते थे, उन मेँ से अधिकांश कैमराबद्ध नहीँ किए जा सकते थे, और न ही किए जा सके. जो आंचलिकता तीसरी क़सम की कहानी मेँ है – उसे न तो बासु समझते थे, न वह उसे आत्मिक सौंदर्य से रंजित कर के परदे पर उतार पाए. अकसर दोष वह इस बात पर मँढ़ते थे कि राज कपूर हीरामन नहीँ लगते. कभी कभी ऐसे ही आरोप वहीदा पर भी लगाते थे. यह अपनी अपनी नज़र का फ़र्क़ है. लेकिन जब निर्देशक फ़िल्म की कास्टिंग से सहमत नहीँ है, तो उसे अपने आप को उस से अलग कर लेना चाहिए. कई बार बासु मुझ से शैलेँद्र के उन निकट समर्थकोँ की निंदा करते थे, जो शैलेँद्र के सच्चे मित्रोँ और सहायकोँ मेँ से थे, जैसे निर्माता जे. ओम प्रकाश.
(यहाँ शैलेँद्र से थोड़ा हट कर मैँ नाटककार मोहन राकेश और अभिनेता ओम शिवपुरी तक जाना चाहूँगा. उन्हेँ शौक़ सवार हुआ राकेश के नाटक आधे अधूरे के फ़िल्मीकरण का. आधे अधूरे मेरा प्रिय नाटक है. लेकिन नाटक और फ़िल्म मेँ ज़मीन आसमान का तकनीकी अंतर होता है. उन लोगोँ ने तय कर लिया था कि वे बासु के निर्देशन मेँ इस के मंचीय रूप का निकटतम फ़िल्मांकन करेँगे. पूणेँ के फ़िल्म संस्थान मेँ एक महीने के भीतर सारी शूटिंग कर ली जाएगी. कलाकार सारे के सारे रंगमंच के थे, और सस्ते थे. शायद बासु ने उन्हेँ समझा दिया था, कि एक लाख से भी कम लागत मेँ फ़िल्म तैयार हो जाएगी, और इस के बाद तो वारे के न्यारे हो जाएँगे! शूटिंग पर जाने से एक दिन पहले, बस एक दिन पहले, मुझे राकेश ने, और उन के और मेरे मित्र राज बेदी ने इस के बारे मेँ बताया. मुझे याद है कि हम लोग एक रेस्तराँ मैँ दोपहर के भोज पर घंटोँ इस पर बातेँ करते रहे थे. मैँ उन्हेँ चेताता रहा कि अब भी समय है – मकड़जाल से बच निकल आएँ. बासु और उस के अनेक मित्र निर्माताओँ के अनुभवोँ के उदाहरण दिए. लेकिन राकेश का कहना था कि बासु मेरे साथ वैसा नहीँ कर सकता. नहीँ कर सकता. नहीँ कर सकता… मेरे पास अपनी सर्वश्रेष्ठ शुभ कामनाएँ देने के अतिरिक्त कोई रास्ता बचा नहीँ था. पुणेँ मेँ शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन समाचार मिला – वही होने लगा था जो मैँ ने कहा था. बासु और राकेश के बीच गंभीर विवाद आरंभ हो गया था. कुछ ही दिनोँ मेँ फ़िल्म का काम बंद हो गया. शायद सतरहवें दिन पूरी यूनिट हताश बंबई लौट आई थी. बहुत बाद मेँ, कई साल बाद, श्रीमती सुधा शिवपुरी ने महान निर्देशक हृषीकेश मुखर्जी को सौंप कर अनगढ़ फ़िल्म को कोई आकार देने की कोशिश की. लेकिन.. परिणाम सब जानते हैँ… यही बासु के मित्र मुग़नी अब्बासी के साथ हुआ… यही… ऐसे ही झगड़े साईँ परांजपे की फ़िल्म स्पर्श की शूटिंग के दौरान हुए. यह बहुत बाद की बात है. तब तक बासु की अपनी फ़िल्में आ चुकी थीँ. इन मेँ कुछ तो उस ने तकनीक की सीमाएँ सीखी थीँ, और जिन के हानि लाभ से उस की अपनी जेब का संबंध था. स्पर्श के पीछे जिन राजनेताओँ का हाथ था, उन से बहुत झगड़ना और जिन्हेँ क्षति पहुँचाना बासु की क्षमता से बाहर था. इस फ़िल्म की शूटिंग के समय तक मैँ मुंबई से दिल्ली आ चुका था, माधुरी का संपादन त्याग कर अपने समांतर कोश की रचना करने. फ़ुटनोट के तौर पर यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि इस के काफ़ी समय बाद सई परांजपे ने कथा नामक फ़िल्म का निर्देशन किया. उस मेँ पाशु नाम का एक पात्र है जो ऊँची ऊँची लेकिन बेबुनियाद बातेँ कर के सब पर रौब ग़ालिब कर के उन्हेँ बहकाता रहता है, जिसे जैसे तैसे बस अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है. पता नहीँ क्योँ मुझे उस पात्र मेँ बासु भट्टाचार्य की झलक दिखाई देती है. क्या सई परांजपे ने इस फ़िल्म मेँ बासु का चरित्र चित्रण कर के खुन्नस निकाली है? और जिस दोस्त को वह धता बता जाता है, वह क्या शैलेँद्र हैँ? पता नहीँ.)
गायक मुकेश – तीसरी क़सम को उबारने की कोशिशेँ
कई कई महीने तीसरी क़सम की शूटिंग बंद रहती थी – कभी अर्थाभाव मेँ, कभी आपसी मनमुटाव मेँ. अकसर सुबह की सैर पर गायक मुकेश से मेरी मुलाक़ात हैँगिंग गार्डन मेँ होती थी, जहाँ मैँ भी सपरिवार जाया करता था. तीसरी क़सम और शैलेँद्र पर जो संकट के बादल मँडरा रहे थे, उन से मुकेश त्रस्त रहते थे. जब शैलेँद्र मेँ दम नहीँ रहा झंझटोँ से निपटने का, तो उन के गहरे शुभचिंतकोँ ने – मुकेश और राज कपूर ने – मामला अपने हाथ मेँ ले लिया. बजट के अभाव मेँ कामचलाऊ शूटिंग कर के, संपादन राज कपूर ने अपने आप किया आर.के. स्टूडियो मेँ (कौन सा टुकड़ा कहाँ का है, पता नहीँ चलता था) जैसे तैसे तीसरी क़सम को रूप दिया गया. मुझे याद है कि उस का अंतिम संस्करण शैलेँद्र और मैँ ने राज कपूर के साथ आर.के. के प्रीव्यू थिएटर मेँ देखा था. हम दोनोँ सहमत थे कि जिन हालात मेँ जहाँ तक पहुँचे हैँ, उन मेँ इस से बहुत आगे जा भी नहीँ सकते थे.
इसी प्रीव्यू थिएटर मेँ शैलेँद्र ने राज कपूर से मेरी पहली मुलाक़ात कराई थी…
लेकिन मैँ बात को थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ. शैलेँद्र से मेरी पहली मुलाक़ात तक.
मैँ दिल्ली मेँ सरिता-कैरेवान पत्रिकाओँ के संपादन विभाग से अलग हो चुका था. कोई कामधंधा नहीँ था. जैसे तैसे फ़्रीलांसिंग कर रहा था. यह बात है नवंबर १९६३ की. तभी अचानक तय हुआ कि मुझे बंबई (तब तक बंबई मुंबई नहीँ बनी थी) जाना है – टाइम्स आफ़ इंडिया के लिए हिंदी मेँ सांस्कृतिक मूल्यों से भरपूर फ़िल्म पत्रिका निकालने. मेरा फ़िल्मोँ का ज्ञान राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, अशोक कुमार, मीना कुमारी, वैजयंती माला, माला सिन्हा, बिमल राय, शांताराम आदि कुछ नामोँ तक ही सीमित था. हाँ, और शैलेँद्र, साहिर, शंकर जयकिशन, ऐस.डी. बर्मन…
तो शैलेँद्र… सरिता के पास ही दफ़्तर था पी.पी.ऐच. का यानी पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस का. वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे – मुंशी. अलमस्त, निस्स्वार्थ, काव्य प्रेमी, प्रगतिशील! वह रामबिलास शर्मा के छोटे भाई थे – यह बात हमारे बीच महत्त्वहीन थी. मुंशी मित्र भी थे और दीवाने भी – शैलेँद्र के. दिल्ली के पनघट पर रास रचाय गयो मनबाटन बड़े रस के साथ सुनाया करते थे. यही नहीँ, शैलेँद्र की अन्य रचनाएँ भी. उन्होँ ने कहा, बंबई जाने पर शैलेँद्र से मेरा नाम भर ले देना, काफ़ी होगा! लेकिन मैँ ठहरा बेहद संकोची और डरपोक क़िस्म का आदमी.
मैँ १९ नवंबर को बंबई पहुँचा था. वहाँ मेरे दो निजी मित्र थे – नंदकिशोर नौटियाल और मुनीश नारायण सक्सेना. तब मुनीश हिंदी ब्लिट्ज़ के संपादक थे, और नौटियाल उन के सहायक. दोनोँ ही मुझे बंबई के कोलाबा और फ़ोर्ट और मैरीन ड्राइव ले गए. और मुनीश तीसरे चौथे दिन मुझे ले गए शैलेँद्र के पास. मैँ ने मुंशी का नाम लिया तो, जैसे शैलेँद्र ने मन के सारे कपाट खोल दिए. उन्होँ ने कहा कि राज कपूर के पास वह स्वयं ले कर जाएँगे मुझे. और राज ने कहा कि तुम शैलेँद्र के मित्र हो इस लिए मेरे घर के दरवाज़े तुम्हारे लिए चौबीस घंटे खुले हैँ.
उस पहली मुलाक़ात के अवसर पर हम लोग बात कर रहे थे उसी प्रीव्यू थिएटर मेँ. समाज की, फ़िल्म की, नई भारतीयता के निर्माण मेँ स्वयं राज कपूर के योगदान की. (जी, हाँ, मैँ राज कपूर को नए भारत के निर्माताओँ मेँ बड़ी ऊँची जगह देता रहा हूँ, और अब भी देता हूँ. आज़ादी के बाद की पहली जवान पीढ़ी के यानी मेरी अपनी पीढ़ी के जो सपने हैँ, सोचने का जो तरीक़ा है – उसे बनाने मेँ राज कपूर का हाथ रहा है.) बात समाज की हो रही थी, फ़िल्मोँ की, शैलेँद्र की, राज कपूर की. और बात मेरी अपनी समझ की भी हो रही थी. शायद राज मुझे टोहना और समझना चाह रहे थे. उन्होँ ने कहा कि इस थिएटर के पीछे जो मशीन है, उस के पास ही उन की सारी फ़िल्मोँ के गीतोँ का औऱ दृश्यों का संकलन रखा है. मैँ अपनी पसंद का जो भी गीत सुनना या दृश्य देखना चाहूँ तो देख सुन सकता हूँ. मैँ ने पूछा, कोई भी? राज ने कहा, हाँ, कोई भी. मैँ ने जो गीत सुनना चाहा उसे सुन कर राज भौँचक्के रह गए. वह गीत देखने सुनने की फ़रमाइश किसी और ने कभी नहीँ की थी. मैँ ने कहा, मैँ वह गीत सुनना चाहता हूँ जो आवारा फ़िल्म मेँ उस समय किसी दुकान के थड़े पर बैठे कुछ भैया लोग गा रहे हैँ, जब भरी बरसात मेँ पृथ्वीराज कपूर अपनी पत्नी को केवल इस लिए घर से निकाल देते हैँ कि एक रात वह डाकुओँ के कब्जे मेँ रही थी.
देश को मिला वरदान थे शैलेंद्र
राज ने पूछा, मैँ ने वह गीत क्योँ चुना? मैँ ने बताया कि शैलेँद्र के उस गीत ने और आवारा फ़िल्म ने मुझे समाज को और राम कथा को एक नए तरीक़े से देखने का नज़रिया दिया था. मुझे ही नहीँ, पूरे भारत को. उस गीत मेँ आरोप लगाती जनता राम से पूछती है – सीता महतारी ने कौन सा अपराध किया था जो आप ने उन्हेँ त्याग दिया? बाद मेँ इसी गीत से प्रेरित हो कर बिमल राय ने अपनी फ़िल्म बिराज बहू मेँ भी एक ऐसा ही गीत रखा था. आवारा का वह गीत मेरे मानस मेँ पैठ गया था. यहाँ तक कि मुझे पता तक नहीँ था कि जब १९५७ मेँ मैँ ने अपनी कविता राम का अंतर्द्वंद्व लिखी, तो एक तरह से मैँ उसी गीत के भावोँ को अपने शब्द दे रहा था.
मुझे याद है कि उसी दिन मैँ ने राज कपूर को बताया था कि जहाँ इस गीत ने मुझे बनाया, वहाँ प्यासा मेँ साहिर के गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ने मुझे निरर्थकता के गहरे अँधेरे कुएँ मेँ धकेल दिया था, जिस से मैँ उन दिनोँ तक पूरी तरह उबर नहीँ पाया था…
बात तो शैलेँद्र की है. शैलेँद्र हिंदी फ़िल्मोँ के ज़रिए देश को मिला वरदान थे. और शैलेँद्र राज कपूर को मिला वरदान भी थे. राज के मन मेँ जो नई मानसिकता उमड़ रही थी, वह इतनी मुखर और प्रभावशाली कभी न हो पाती, यदि स्वयं शैलेँद्र की मानसिकता वही न होती और वह उसे शब्द न देते, शंकर जयकिशन उसे मधुर सरगम मेँ न ढालते और मुकेश और मुहम्मद रफ़ी उसे आवाज़ न देते. आवारा हूँ या गरदिश मेँ हूँ आस्मान का तारा हूँ केवल राज कपूर की ही बात नहीँ कर रहा था, वह उन दिनोँ के निर्माणशील भारत मेँ बेकाम बेकार भटकते हर महत्त्वाकांक्षी ईमानदार नौजवान के दिल के दर्दभरी गुहार था, जिसे करने को काम नहीँ मिल रहा था. यही नहीँ, दूसरे विश्वयुद्ध से उबर कर दुनिया भर के जो नौजवान आवारगी के आलम मेँ वक़्त गुज़ार रहे थे, यह उन के मन का दर्पण भी था. यही कारण है कि यह गीत दुनिया भर के नौजवानोँ का गीत बन गया – चाहे वे भारतवंशी हों, या रूसी, जापानी, चीनी, इंग्लिस्तानी या अमरीकी.
शैलेँद्र आम आदमी के मन की पुकार को बड़े सहज शब्दोँ मेँ एक ऐसा आयाम देते थे, जो गहरे अर्थ वाला हो, और दिल की बात करता हो और दिल से दिल तक पहुँचता हो. वही थे जो कह सके – छोटी सी बात न मिर्च मसाला दिल की बात सुने दिल वाला. वही थे जो गा सके – हम भी हैँ, तुम भी हो आमने सामने… वही थे जो नायिका से दिल का सौदा इन शब्दोँ मेँ कर पाए – देती है दिल दे बदले मेँ दिल ले. और वही थे जो इतने कम शब्दोँ मेँ पूरे देश के सांस्कृतिक परिवेश का बयान कर सके – हम उस देश के वासी हैँ, जिस देश मेँ गंगा बहती है.
मैँ ने शैलेँद्र के गीतोँ के ये सभी उदाहरण जान बूझ कर राज कपूर की फ़िल्मोँ से लिए हैँ – क्योँ कि राज कपूर ही रेलवे यार्ड मेँ काम करने वाले इस मज़दूर कवि को फ़िल्मोँ मेँ लाए, और राज कपूर की ही रूमानियत थी जिस के साथ इस कवि के मन की गहराई को देश की गहराई बनने का मौक़ा मिला. राज कपूर ही थे जिन्होँ ने शैलेँद्र के साथ हसरत जयपुरी को, शंकर जयकिशन को, मुकेश को और मुहम्मद रफ़ी को जोड़ा और एक ऐसी टीम बनाई जो जब तक शैलेँद्र रहे, चलती रही.
सब से पहला कंधा दिया
इसी टीम के शेष सदस्योँ ने शैलेँद्र की अरथी को सब से पहले कंधा दिया. यह उन्हीँ का अधिकार था. इस टीम की अलग पहचान यह थी कि यह बौद्धिक होते हुए भी दिल से सोचती थी, दिल से काम करती थी, और दिलोँ तक पहुँचना चाहती थी. इस का गणित दिल का था. ख़्वाजा अहमद अब्बास अपनी कहानियोँ पर स्वयं भी फ़िल्म बनाते थे, और उन की कहानियोँ पर यह टीम भी अपने कप्तान राज कपूर के नेतृत्व मेँ काम करती थी. अंतर सामने रहता था. अब्बास केवल दिमाग़ तक पहुँच पाते थे, यह टीम दिलोँ तक. कोरी बौद्धिकता सूना मरुथल है. उस मेँ प्रेम की नौका नहीँ चलती – यह बात उद्धव से गोपियोँ ने कही थी. शैलेँद्र ने बुद्धिवादियोँ पर कटाक्ष इन शब्दोँ मेँ किया था – कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैँ, इनसान को कम पहचानते हैँ.
ऐसा नहीँ है कि हिंदी फ़िल्मोँ को समर्थ कवि नहीँ मिले. महाकवि प्रदीप भारत के राष्ट्रवाद के महान गायक थे. चालीसादि दशक मेँ दूर हटो ए दुनिया वालो हिंदुस्तान हमारा है और चल चल रे नौजवान से पचासादि दशक मेँ स्वतंत्रता सेनानियोँ की भूमि को प्रणाम करने वाले गीत इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की लिख कर वे साठादि दशक मेँ चीनी सरहद पर मरने वालोँ के नाम लिखे गीत ऐ मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख मेँ भर लो पानी तक वे देश के अंतस् को अपनी अलग शैली मेँ झकझोरते रहे. हमारे पास मजरूह और साहिर जैसे प्रगतिशील गीतकार भी थे, जो रोटी रोज़ी की बात के साथ साथ रोमांस की बात पूरी कारीगरी और कलाकारी के साथ कहते थे.
लेकिन भारत मेँ बौद्धिक मार्क्सवाद को हार्दिक सूफ़ीवाद जामा पहनाने का काम शैलेँद्र ने किया. एक हद तक हम शैलेँद्र को आधुनिक कबीर कह सकते हैँ. बड़ी से बड़ी दार्शनिक बात साधारण से शब्दोँ मेँ आम आदमी तक पहुँचाने की जो ख़ूबी कबीर मेँ थी, वही हमारे युग मेँ शैलेँद्र मेँ थी. रोटीरोज़ीवाद और प्रगतिवाद के सूखे नारे तो सैकड़ों कवियोँ ने लगाए, लेकिन यह गुण किस और कवि के पास था जो भूख से बिलबिला रहे बच्चोँ की आकांक्षाओँ को इतनी सादगी से बयान कर सके – क्योँ न हम रोटियोँ का पेड़ इक लगा लेँ, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें आम रोटी खा लेँ. है कोई और जिस ने जीवन की क्षणभंगुरता को शम्मी कपूर के होंठों से इतनी सादगी से कहा हो – सबेरे वाली गाड़ी से चले जाएँगे, न कुछ ले के जाएँगे, न कुछ दे के जाएँगे.
और शैलेँद्र सच ही सबेरे वाली गाड़ी से गए. सुबह.
❉❉❉
आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ
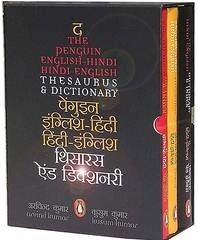



Comments