श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद
ब्रह्म विद्या योग शास्त्र
अध्याय 18
☀ अब गीता ☀
पढ़ना आसान
समझना आसान
अनुवादक
अरविंद कुमार
इंटरनैट पर प्रकाशक
अरविंद लिंग्विस्टिक्स प्रा. लि.
कालिंदी कालोनी
नई दिल्ली 110065
अष्टादशोऽध्यायः
मोक्ष संन्यास योग
अर्जुनोवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशि-निषूदन ॥१॥
अर्जुन ने कहा
महाबाहु, हृषीकेश, केशिनिषूदन! मैँ संन्यास का और त्याग का तत्त्व जानना चाहता हूँ. उन दोनोँ मेँ क्या अंतर है?
श्रीभगवान् उवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्व-कर्म-फल-त्यागं प्राहुस् त्यागं विचक्षणाः ॥२॥
श्री भगवान ने कहा
मेधावी और विद्वान लोग कहते हैँ कि फल की इच्छा से किए कर्मोँ का परित्याग संन्यास है. सब कर्मोँ के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग ‘त्याग’ कहते हैँ.
त्याज्यं दोषवद् इत्य् एके कर्म प्राहुर् मनीषिणः ।
यज्ञ-दान-तपः-कर्म न त्याज्यम् इति चापरे ॥३॥
कई मनीषी जन कहते हैँ कि सभी कर्म दोष देने वाले हैँ. उन का त्याग कर दिया जाना चाहिए. कुछ अन्य मनीषियोँ का कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मोँ का त्याग नहीँ किया जाना चाहिए.
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत-सत्तम ।
त्यागो हि पुरुष-व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥४॥
भरत श्रेष्ठ, पुरुषोँ मेँ सिंह, अर्जुन! त्याग के विषय मेँ मेरा निश्चय, मेरा निर्णय, सुन. त्याग तीन प्रकार का कहा गया है.
यज्ञ-दान-तपः-कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् ।
यज्ञो दानं तपश् चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥
यज्ञ, दान और तप जो कर्म हैँ – उन कर्मोँ का त्याग नहीँ करना चाहिए. ये निस्संदेह करने योग्य हैँ. यज्ञ, दान और तप मनीषी जनोँ को पवित्र करते हैँ.
एतान्य् अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् ॥६॥
लेकिन, पार्थ, इन कर्मोँ को भी आसक्तिहीन हो कर करना चाहिए और इन के फलोँ का त्याग कर देना चाहिए. इन्हेँ मात्र कर्तव्य समझ कर करना चाहिए. यह मेरा सुनिश्चित और उत्तम मत है.
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः ॥७॥
जीवन के आवश्यक कर्म – नित्य नियम –त्याज्य नहीँ है. उन का त्याग मूर्खतावश ही किया जा सकता है. ऐसा त्याग तामसिक कहलाता है.
दुःखम् इत्य् एव यत् कर्म काय-क्लेश-भयात् त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्याग-फलं लभेत् ॥८॥
काया कष्ट के डर से कुछ लोग यह मान लेते हैँ कि कर्म मात्र दुःख है, और कर्मोँ को त्याग देते हैँ, उन का त्याग रजोगुणी है. ऐसा कर्म त्याग निरर्थक और निष्फल है.
कार्यम् इत्य् एव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥
कर्तव्य मान कर नियत कर्म करेँ और आसक्ति को और फल को त्याग देँ, तो वह त्याग सात्त्विक है.
न द्वेष्ट्य् अकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्व-समाविष्टो मेधावी छिन्न-संशयः ॥१०॥
सत्त्व मेँ समाविष्ट त्यागी वह है जो अकुशल कर्म से कतराता नहीँ और कुशल कर्म से आसक्त नहीँ होता. वह मेधावी है, बुद्धिमान है. उस के संशय कट चुके हैँ.
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य् अशेषतः ।
यस् तु कर्म-फल-त्यागी स त्यागीत्य् अभिघीयते ॥११॥
देहधारियोँ के लिए यह संभव नहीँ है कि वे पूरी तरह सब कर्मोँ का त्याग कर देँ, इस लिए त्यागी वही कहा जाता है जो कर्मोँ के फल त्याग दे.
अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
भवत्य् अत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥१२॥
कर्मोँ का तीन प्रकार का फल मिलता है – अच्छा, बुरा और मिला जुला. मरने पर यह फल उन्हेँ मिलता है जो कर्म फल का त्याग नहीँ करते. लेकिन जो संन्यासी हैँ, जो अपने कर्मोँ के फलोँ का त्याग कर चुके हैँ, उन्हेँ कैसा भी फल नहीँ मिलता.
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व-कर्मणाम् ॥१३॥
महाबाहु, सांख्य सिद्धांत मेँ सब कर्मोँ की सिद्धि के पाँच कारण बताए गए हैँ.
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्-विधम् ।
विविधाश् च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥
एक : अधिष्ठान – आधार, आश्रय, शरीर.
दो : कर्ता – करने वाला, पुरुष, गुणोँ का भोक्ता.
तीन : अलग अलग करण – साधन, इंद्रियाँ.
चार : अनेक और अलग अलग चेष्टाएँ, कोशिशेँ, प्रयास, उद्यम.
पाँच : दैव – प्रकृति की शक्तियाँ जो कर्म संपादन मेँ कर्ता के काम आती हैँ.
कर्म की सिद्धि के ये पाँच कारण हैँ.
शरीर-वाङ्-मनोभिर् यत् कर्म प्रारभते नरः ।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥
शरीर, वाणी और मन से मनुष्य कोई भी काम आरंभ करे, वह कर्म चाहे शास्त्र के अनुसार हो या शास्त्र के विरुद्ध, उस कर्म मेँ ये पाँचोँ तत्त्व होते हैँ.
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्य् अकृत-बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥
कर्म के ये पाँच कारण होते हुए भी, जो अपनी बुद्धिहीनता के कारण केवल अपने को कर्ता के रूप मेँ देखता है, उस की मति ठीक नहीँ है.
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमाँल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥
जिस मेँ यह अहंकार नहीँ है कि मैँ कर्मोँ को करता हूँ और जिस की बुद्धि निर्लिप्त है, वह न तो किसी को मारता है, न अपने कर्म से बँधता है.
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म-चोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म-सङ्ग्रह ॥१८॥
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता (ज्ञान, ज्ञान का विषय, और ज्ञानी) – ये तीन मिल कर कर्म की प्रेरणा हैँ. करण, कर्म और कर्ता – ये तीनोँ कर्म संग्रह हैँ – कर्म के सक्रिय अंग हैँ.
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण-भेदतः ।
प्रोच्यते गुण-सङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्य् अपि ॥१९॥
सांख्य के अंतर्गत ज्ञान, कर्म और कर्ता को भी गुणोँ के अनुसार तीन प्रकार का माना गया है.
सर्व-भूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज् ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥
जिस के द्वारा सब पदार्थोँ और जीवोँ मेँ ‘वह’ एक अव्यय दिखाई देता है और सब अलग अलग विभाजित चीज़ोँ मेँ ”वह” अविभक्त और अखंड दिखाई देता है, वह ज्ञान सात्त्विक है.
पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानं नाना भावान् पृथग्-विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज् ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥
जिस के द्वारा मनुष्य को संसार के विविध पदार्थोँ और प्राणियोँ मेँ अलग अलग अस्तित्व दिखाई देते हैँ, वह राजसिक या रजोगुणी ज्ञान है.
यत् तु कृत्स्नवद् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवद् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम् ॥२२॥
तामसी ज्ञान के द्वारा मनुष्य किसी एक कार्य को अपने मेँ संपूर्ण और स्वतंत्र समझ कर उसी से चिमट जाता जाता है. वह समझने लगता है कि हर कार्य अपने आप से उपजता है – उस के पीछे अन्य पूर्ववर्ती कार्योँ की अंतहीन शृंखला नहीँ होती. वह पूर्ण सत्य को नहीँ समझ पाता. ऐसा कम ज्ञान छिछला होता है.
नियतं सङ्गरहितम् अ-राग-द्वेषतः कृतम् ।
अ-फल-प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्त्विक म् उच्यते ॥२३॥
सात्त्विक कर्म वह कहलाता है जो नियत है, निर्धारित है. ऐसा कर्म आसक्ति के बग़ैर किया जाता है. उस मेँ राग द्वेष नहीँ होता. उस कर्म के पीछे उस का फल भोगने की इच्छा नहीँ होती.
यत् तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ।
क्रियते बहुलायासं तद् राजसम् उदाहृतम् ॥२४॥
राजसिक कर्म करने वाला इच्छाओँ, चाहतोँ, से भरा होता है. वह अपने आप को कर्मोँ का कर्ता मानता है और कर्ता होने के अभिमान से भरा रहता है. ऐसा कर्म भारी श्रम से किया जाता है.
अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहाद् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते ॥२५॥
तामसिक कर्म वह है जो मोह – अज्ञान और भ्रम – से आरंभ किया जाता है. इस मेँ न तो पहले से अनुबंध – फल, शुभ, अशुभ, कारण, प्रयोजन, मार्ग आदि आरंभिक तर्क – के बारे मेँ सोचा जाता है, न हानि, हिंसा और सामर्थ्य के बारे मेँ विचार किया जाता है.
मुक्त-सङ्गोऽनहंवादी धृत्य्-उत्साह-समन्वितः ।
सिद्ध्य्-असिद्ध्योर् निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥
सात्त्विक कर्ता मेँ आसक्ति नहीँ होती. वह अहंवादी नहीँ होता. वह धैर्य और उत्साह से भरा होता है. काम के पूरा होने या न होने मेँ, सिद्धि और असिद्धि मेँ वह निर्विकार होता है.
रागी कर्म-फल-प्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्ष-शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥
राजसिक कर्ता रागोँ से युक्त होता है. वह कर्मोँ का फल भोगना चाहता है. वह लोभी होता है. वह हिंसात्मक होता है – दूसरोँ को कष्ट पहुँचाना चाहता है. वह अस्वच्छ होता है – उस का आचरण बरताव शुद्ध नहीँ होता. ख़ुशी से वह फूल उठता है. और शोक मेँ डूब जाता है.
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घ-सूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
तामसिक कर्ता आत्मनियंत्रित, सयंमित नहीँ होता. संस्कारहीन और उजड्ड होता है. गतिहीन, जड़, होता है. धूर्त, चालाक, मक्कार होता है. कर्महीन और आलसी होता है. रोता झीँकता रहता है. टालमटोल करना उस का स्वभाव होता है.
बुद्धेर् भेदं धृतेश् चैव गुणतस् त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥२९॥
गुणोँ के अनुसार बुद्धि और धृति के तीन भेद हैँ. धनंजय, वे भी तू मुझ से अलग अलग सुन.
प्रवृत्तिं च निवृतिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥
सात्त्विक बुद्धि जानती है कि कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त – कहाँ सक्रिय होना है, कहाँ से दूर हट जाना है. सात्त्विक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष का भेद जानती है.
यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यम् एव च ।
अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥
रजोगुणी बुद्धि धर्म और अधर्म को, कार्य और अकार्य को ठीक तरह से नहीँ जानती.
अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान् विपरीतांश् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥
तामसी बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सब उद्देश्योँ को औँधा, उलटा, समझती है. ऐसी बुद्धि अंधकार से ढँकी है.
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय-क्रियाः ।
योगेनाऽऽव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥
सात्त्विक धृति – धारण शक्ति – मेँ मनुष्य एकाग्रता और एकनिष्ठा से मन, प्राण और इंद्रियोँ की क्रियाओँ को स्थिर रखता है.
यया तु धर्म-कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥
जिस धृति से मनुष्य पूरी आसक्ति के साथ धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, और फल की इच्छा करता है, वह रजोगुणी है.
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च ।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥
तमोगुणी धृति के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, शोक, दुःख और मद को जकड़े रखता है.
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥
सुख तीन प्रकार का होता है. एक सुख मेँ मनुष्य अभ्यासपूर्वक आनंद पाता है. इस मेँ वह वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ दुःखोँ का अंत हो जाता है.
यत् तद् अग्रे विषम् इव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् आत्म-बुद्धि-प्रसादजम् ॥३७॥
सात्त्विक सुख आरंभ मेँ विष जैसा लगता है, पर अंत मेँ अमृत समान होता है. ऐसा सुख आत्मबुद्धि के प्रसाद से होता है.
विषयेन्द्रिय-संयोगाद् यत् तद् अग्रेऽमृतोमपम् ।
परिणामे विषम् इव तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥
एक सुख विषयोँ और इंद्रियोँ के संयोग से होता है. आरंभ मेँ यह अमृत जैसा लगता है. लेकिन इस का परिणाम विष जैसा होता है. यह सुख रजोगुणी कहा गया है.
यद् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः ।
निद्रालस्य-प्रमादोत्थं तत् तामसम् उदाहृतम् ॥३९॥
एक सुख आरंभ मेँ और परिणाम मेँ आत्मा को मोह लेता है. यह निद्रा, आलस्य और लापरवाही से होता है. इसे तामसिक कहा गया है.
न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर् मुक्तं यद् एभिः स्यात् त्रिभिर् गुणैः ॥४०॥
पृथ्वी पर या स्वर्ग के देवताओँ मेँ कोई भी सत्ता ऐसी नहीँ है, जो प्रकृति से उपजे इन गुणोँ से मुक्त हो.
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणां च परन्तप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-प्रभवैर् गुणैः ॥४१॥
ब्राह्मणोँ, क्षत्रियोँ, वैश्योँ और शूद्रोँ के कामोँ का विभाजन गुणोँ के आधार पर किया गया है. इन गुणोँ का जन्म उन के स्वभाव से हुआ है.
शमो दमस् तपः शौचं क्षान्तिर् आर्जवम् एव च ।
ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म-कर्म स्वभावजम् ॥४२॥
एक : शम – कल्याण, मंगल कामना, और शांति.
दो : दमन – इंद्रियोँ का निग्रह, आत्म नियंत्रण.
तीन : तप – साधना, तपस्या.
चार : शौच – स्वच्छता, सफ़ाई, तन और मन की पवित्रता.
पाँच : क्षांति – क्षमा, सहनशीलता, उदारता.
छः : आर्जव – सरलता, सादगी, निष्कपटता, खरापन.
सात : ज्ञान – अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान.
आठ : विज्ञान – ब्रह्म के व्यक्त कर्मोँ का ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, पदार्थ ज्ञान.
नौ : आस्तिक्य – आस्तिकता, ईश्वर मेँ विश्वास, भक्ति, श्रद्धा.
ये ब्राह्मणोँ के कर्म हैँ. ये उन के स्वभाव से उत्पन्न हुए हैँ.
शौर्यं तेजो धृतिर् दाक्ष्यं युद्धे चाप्य् अपलायनम्
दानम् ईश्वर-भावश् च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥
एक : शौर्य – शूरवीरता, पराक्रम, बहादुरी.
दो : तेज – शक्ति, ओज, ऊर्जा.
तीन : धृति – धैर्य, दृढ़ता, स्थिरता.
चार : युद्ध मेँ दक्षता – रण की कला मेँ महारत.
पाँच : अ-पलायन – शत्रु के सामने डटे रहने की हिम्मत, हिम्मत न हारना.
छः : दान – उपहार और पुरस्कार देने की भावना, उदारता, दानशीलता.
सात : ईश्वर भाव – अपने को स्वामी समझने की आदत, स्वामित्व.
ये क्षत्रियोँ के कर्म हैँ. ये उन के स्वभाव से उत्पन्न हुए हैँ.
कृषि-गौरक्ष्य-वाणिज्यं वैश्य-कर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥
कृषि – खेती. गोरक्षा – गौ पालन, मवेशियोँ को पालना. वाणिज्य – व्यापार. ये वैश्योँ के कर्म हैँ, जो उन के स्वभाव से उपजे हैँ.
परिचर्या, सेवा, टहल जैसे काम शूद्रोँ के हैँ. ये भी उन के स्वभाव से उपजे हैँ.
स्वे स्वे कर्मण्य् अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्म-निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्रुणु ॥४५॥
अपने अपने काम मेँ लगे मनुष्य को सिद्धि मिलती है. सुन, अपने काम मेँ लगे रहने से सिद्धि कैसे मिलती है.
यतः प्रवृत्तिर् भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् ।
स्वकर्मणा तम् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥
”जिस” ने सब भूत पदार्थोँ और प्राणियोँ को उन के कामोँ मेँ लगाया है, ”जिस” से यह सारा जगत ओतप्रोत है, अपने अपने कर्म से ”उस” की पूजा अर्चना कर के मानव को सिद्धि मिलती है.
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वभाव-नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥
स्वधर्म – अपना काम, अपना धंधा – गुणहीन हो तो भी कौशलपूर्ण परधर्म से अच्छा है. हमारा जो कर्म स्वभाव से नियत है, वह करने से पाप नहीँ मिलता.
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर् इवावृताः ॥४८॥
कौंतेय, जो कर्म आदमी को स्वभाव से ही मिला है, वह दोषोँ से भरा हो तो भी उसे छोड़ना नहीँ चाहिए. संसार मेँ सारे कर्म, सब प्रयास उसी तरह दोषोँ से घिरे हैँ, जैसे अग्नि धुएँ से घिरी होती है.
असक्त-बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत-स्पृहः ।
नैष्कर्म्य-सिद्धिं परमां संन्यासेनाऽऽधिगच्छति ॥४९॥
परम निष्कर्म सिद्धि उसे मिलती है, जिस की बुद्धि संसार मेँ आसक्त नहीँ होती. ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा को जीत चुका होता है. उस की सारी चाहतेँ, कामनाएँ, छूट चुकी होती हैँ. यह निष्कर्म सिद्धि संन्यास से मिलती है.
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥
सिद्धि पा कर मनुष्य ब्रह्म तक कैसे पहुँचता है, कौंतेय, यह तू मुझ से संक्षेप मेँ सुन. ब्रह्म को पाना ज्ञान की पराकाष्ठा है.
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च ।
शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा राग-द्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥
बुद्धि को पूरी तरह शुद्ध कर ले. धीरज के साथ अपने को बस मेँ कर के योग को प्राप्त कर ले. शब्द आदि जो इंद्रियोँ के विषय हैँ, उन्हेँ त्याग दे. राग और द्वेष, इच्छा और अनिच्छा, को दूर कर दे…
विविक्त-सेवी लघ्वाशी यत-वाक्-काय-मानसः ।
ध्यान-योग-परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥
…एकांत का सेवन करने वाला… कम खाने वाला… वाणी, काया और मन को जीतने वाला… नित्य परम ध्यान योग मेँ लगा रहने वाला… वैराग्य की शरण मेँ आने वाला… मनुष्य…
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म-भूयाय कल्पते ॥५३॥
… अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को छोड़ दे. किसी मेँ ममता न रखे. इस प्रकार पूरी तरह शांत हो जाए. तब वह स्वयं ब्रह्म होने लायक़ हो जाता है.
ब्रह्म-भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम् ॥५४॥
ब्रह्म मेँ मिल कर प्रसन्न आत्मा वाला मनुष्य न तो किसी का शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है. सब पदार्थोँ और प्राणियोँ को वह एक समान समझता है. वह मेरी परम भक्ति को पा लेता है.
भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश् चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥
भक्ति के द्वारा वह मेरा स्वरूप अच्छी तरह जान लेता है. फिर वह मुझ मेँ प्रवेश कर लेता है.
सर्व-कर्माण्य् अपि सदा कुर्वाणो मद्-व्यपाश्रयः ।
मत्-प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् ॥५६॥
सारे कर्म करते रहने पर भी वह मेरी शरण मेँ आ कर मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से, उस सनातन और अनाश्य पद को पा लेता है.
चेतसा सर्व-कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धि-योगं उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥
अपने सब कर्मोँ को तू अपनी संपूर्ण चेतना से मुझे अर्पित कर दे. अपने को मुझ मेँ लगा दे. बुद्धि योग का सहारा ले. निरंतर मुझ मेँ अपना चित्त लगा.
मच्चित्तः सर्व-दुर्गाणि मत्-प्रसादात् तरिष्यसि ।
अथ चेत् त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि॥५८॥
मुझ मेँ चित्त लगा कर तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयोँ को पार कर लेगा. लेकिन… अगर तू अहंकार से ग्रस्त है, अपने को कर्ता मानता है, और अगर इस कारण तू मेरी बात नहीँ सुनेगा, तो नष्ट हो जाएगा.
यद्य् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैष व्यवसायस् ते प्रकृतिस् त्वां नियोक्ष्यति॥५९॥
यह मान कर कि कर्म करने वाला स्वयं तू है, तू युद्ध न करने का निर्णय लेता है, तो तेरा यह निर्णय ग़लत है. तेरा स्वभाव तुझे युद्ध मेँ लगा देगा.
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यस्य् अवशोऽपि तत्॥६०॥
कौंतेय, तू अपने स्वभाव से उपजे कर्म से बँधा है. मोह मेँ फँस कर तू जो काम नहीँ करना चाहता, मज़बूर हो कर वह तू करेगा ही.
ईश्वरः सर्व-भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्व-भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥
अर्जुन, सब प्राणियोँ के हृदयस्थल मेँ ईश्वर बैठा है. वह अपनी माया से सब को ऐसे घुमाता है मानो वे किसी यंत्र पर सवार होँ.
तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्-प्रसादात् परां शान्तिं स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥६२॥
अर्जुन, सब प्रकार से तू ‘उसी’ की शरण मेँ जा. ‘उस’ की कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान मिलेगा.
इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ।
विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥
गोपनीयोँ मेँ भी सब से गोपनीय, और रहस्यपूर्ण ज्ञान मैँ ने तुझ से कहा है. इस संपूर्ण ज्ञान पर पूरी तरह सोच विचार कर तू जैसा चाहता है वैसा कर.
सर्व-गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥
एक बार फिर तू मेरे परम रहस्यपूर्ण वचन सुन. तू मुझे बहुत प्रिय है. इस लिए तेरे भले के लिए कहता हूँ.
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
माम् एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥
अपना मन मुझ मेँ लगा. मेरा भक्त बन, अपने यज्ञ मेरे लिए कर. मुझे नमस्कार कर. तू मुझ तक ही पहुँचेगा. मैँ तुझ से सच्चा वादा करता हूँ. तू मुझे प्रिय है.
सर्व-धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज ।
अहम् त्वा सर्व-पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥
सब धर्मोँ को त्याग कर तू एकमात्र मेरी शरण मेँ आ. मैँ तुझे सब पापोँ से मुक्त कर दूँगा. शोक मत कर.
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥
मेरा यह उपदेश तू उस से कभी मत कहना, जो तप नहीँ करता, जो भक्त नहीँ है, जो यह सुनना नहीँ चाहता, जिस मेँ श्रद्धा नहीँ है. मेरे निंदक को भी तू यह उपदेश मत बताना.
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत्य् असंशयः ॥६८॥
मुझ मेँ पूरी भक्ति रख कर जो मेरा यह परम गोपनीय उपदेश मेरे भक्तोँ को बताएगा वह मुझे पाएगा – इस मेँ संदेह नहीँ है…
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय-कृत्तमः ।
भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरे भुवि ॥६९॥
…मेरा प्रिय करने वालोँ मेँ उस से बढ़ कर कोई और मनुष्य नहीँ है, न ही इस पृथ्वी पर उस से अधिक प्यारा मुझे कोई और होगा.
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ।
ज्ञान-यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः ॥७०॥
हम दोनोँ का यह संवाद धार्मिक है. जो इस संवाद का अध्ययन करेगा, मैँ समझूँगा कि वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे अपना इष्ट, अपना प्रिय बनाना चाहता है.
श्रद्धावान् अनसूयश् च शृणुयाद् अपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य-कर्मणाम् ॥७१॥
जो श्रद्धालु और ईर्ष्याहीन मनुष्य इसे सुनेगा, वह भी पापोँ से मुक्त हो जाएगा. वह उन शुभ लोकोँ को जाएगा जहाँ पुण्यात्मा जाते हैँ.
कच्चिद् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिद् अज्ञान-सम्मोहः प्रनष्टस् ते धनञ्जय ॥७२॥
पार्थ, तू ने मेरा यह उपदेश ध्यान से सुना तो है? धनंजय, अज्ञान के कारण तुझे जो भ्रम हो गया था, वह दूर तो हो गया है?
अर्जुनोवाच
नष्टो मोहः स्मृतिर् लब्धा त्वत्-प्रसादान् मयाऽऽच्युत ।
स्थितोऽस्मि गत-सन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥
अर्जुन ने कहा
अच्युत, आप की कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है. स्मृति लौट आई है. संदेह दूर हो गया है. मैँ दृढ़ हूँ. आप का कहा करूँगा.
सञ्जयोवाच
इत्य् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भूतं रोम-हर्षणम् ॥७४॥
संजय ने कहा
मैँ ने वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह संवाद सुना. यह संवाद अद्भुत है और इसे सुन कर रोमांच हो आता है.
व्यास-प्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् ।
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् ॥७५॥
व्यास की कृपा से मैँ ने यह गुप्त और महान योग सुना. स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने यह मेरी आँखोँ के सामने कहा.
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् ।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर् मुहुः ॥७६॥
राजा धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन का यह पुण्य संवाद मुझे बार बार याद आता है. हर बार इसे याद कर के मैँ बार बार रोमांचित होता हूँ.
तच् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥
राजा धृतराष्ट्र, हरि का वह अद्भुत रूप भी मुझे बार बार याद आता है. और हर बार उसे याद कर के मैँ बार बार रोमांचित हो उठता हूँ.
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर् विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम॥७८॥
यहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैँ, वहाँ लक्ष्मी है. वहाँ विजय है. वहाँ कल्याण है. वहाँ अचल नीति का व्यवहार है. यह मेरा मत है.
इति श्रीमद्-भगवद्-गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म-विद्यायां योग-शास्त्रे श्री-कृष्णार्जुन-संवादे मोक्ष-संन्यास-योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः
यह था श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मेँ मोक्ष संन्यास योग नाम का अठारहवाँ अध्याय
॥इति शुभमस्तुश्॥
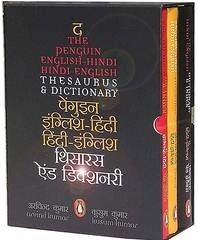
Comments