श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद
ब्रह्म विद्या योग शास्त्र
अध्याय 6
☀ अब गीता ☀
पढ़ना आसान
समझना आसान
अनुवादक
अरविंद कुमार
इंटरनैट पर प्रकाशक
अरविंद लिंग्विस्टिक्स प्रा. लि.
कालिंदी कालोनी
नई दिल्ली
षष्ठोऽध्यायः
आत्मसंयम योग
श्रीभगवान् उवाच
अनाश्रितः कर्म-फलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः ॥१॥
श्री भगवान ने कहा
जो कर्म के फल पर आश्रित नहीँ होता, लेकिन करने योग्य सारे काम करता है, वही व्यक्ति संन्यासी और योगी है, न कि वह जो अग्निहोत्र को, गृहस्थाश्रम को, त्याग कर बैठ जाता है या निठल्ला रहता है.
यं संन्यासम् इति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव ।
न ह्य् असंन्यस्त-सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥
जिसे संन्यास कहते हैँ, उसे ही तू योग समझ. मन के संकल्पोँ से, इरादोँ से संन्यास लिए बिना कोई योगी नहीँ बनता.
आरुरुक्षोर् मुनेर् योगं कर्म कारणम् उच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते ॥३॥
योग साधना मेँ कर्म साधन होता है. योग सिद्धि मिल जाने पर आत्मसंयम को उस का साधन कहा जाता है.
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व् अनुषज्जते ।
सर्व-सङ्कल्प-संन्यासी योगारूढस् तदोच्यते ॥४॥
एक समय ऐसा आता है जब आदमी न तो इंद्रियोँ के भोगोँ मेँ आसक्त होता है, न कर्मोँ मेँ. कर्मोँ से पीछे जो संकल्प होते हैँ, इरादे होते हैँ, उन्हेँ वह त्याग चुका होता है. तभी उस व्यक्ति को योगी माना जाता है.
उद्धरेद् आत्मनाऽऽत्मानं नात्मानम् अवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मनः ॥५॥
अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे गिराना नहीँ. अपने मित्र हम स्वयं ही हैँ और स्वयं ही हम अपने शत्रु हैँ.
बन्धुर् आत्मात्मनस् तस्य येनात्मैवाऽऽत्मना जितः ।
अनात्मनस् तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६॥
अपना मित्र वह है जिस ने अपने आप को जीत लिया है. जिस ने अपने को नहीँ जीता, वह अपने शत्रु जैसा बरताव कर रहा है.
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्ण-सुख-दुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥
जिस ने अपने को जीत लिया है और शांति पा ली है, वह परमात्मा मेँ समा गया है. वह सर्दी गरमी, सुख दुःख और मान अपमान आदि द्वंद्वोँ मेँ शांत रहता है.
ज्ञान-विज्ञान-तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्य् उच्यते योगी सम-लोष्टाश्म-काञ्चनः ॥८॥
उस की आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है. वह अंतर्तम मेँ स्थित है. उस ने अपनी इंद्रियोँ को जीत लिया है. उसे योगी कहते हैँ. मिट्टी, पत्थर और सोने को योगी एक समान समझता है.
सुहृन्-मित्रार्युदासीन-मध्यस्थ-द्वेष्य-बन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु सम-बुद्धिर् विशिष्यते ॥९॥
मित्र और शत्रु मेँ वह भेद नहीँ करता. उस के लिए न कोई बाहर है, न भीतर. उस के लिए मित्र और शत्रु, अपने और पराए सब बराबर हैँ. साधुओँ और पापियोँ को वह एक समान समझता है. ऐसी सम बुद्धि वाला मनुष्य उत्तम है.
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यत-चितात्मा निराशीर् अपरिग्रहः ॥१०॥
योगी को चाहिए कि निर्जन स्थान मेँ वह निरंतर अपने को योग मेँ लगाए. एकांत मेँ अपने आप अपने चित्त और आत्मा को क़ाबू मेँ करे. मन से आशा और आकांक्षा को निकाल दे. अपरिग्रह का पालन करे – आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे.
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः ।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन-कुशोत्तरम् ॥११॥
स्वच्छ भूमि पर अपना आसन इस प्रकार बिछाए कि वह हिले नहीँ. आसन न तो बहुत ऊँचा हो, न बहुत नीचा. आसन के लिए पहले भूमि पर कुशा – घास – हो, उस के ऊपर मृगछाला हो, और मृगछाला पर मुलायम वस्त्र हो.
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत-चित्तेन्द्रिय-क्रियः ।
उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्म-विशुद्धये ॥१२॥
वहाँ बैठ कर मन को एकाग्र करे. चित्त को और इंद्रियोँ की क्रियाओँ को वश मेँ कर के आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे.
समं काय-शिरो-ग्रीवं धारयन्न् अचलं स्थिरः ।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश् चानवलोकयन् ॥१३॥
शरीर, सिर और गरदन को एक सीध मेँ रखे. अचल बैठे. हिले डुले नहीँ. नाक के अगले भाग को देखे. इधर उधर न देखे.
प्रशान्तात्मा विगत-भीर् ब्रह्मचारि-व्रते स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥
अंतःकरण को शांत करे. भय को निकाल दे. ब्रह्माचरण का व्रत ले और उस मेँ स्थित रहे. मन को वश मेँ कर के मुझ मेँ चित्त लगाए. योग की साधना मेँ बैठ कर मेरी और उन्मुख हो.
युञ्जन्न् एवं सदाऽऽत्मानं योगी नियत-मानसः ।
शान्तिं निर्वाण-परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति ॥१५॥
मन को नियंत्रित कर के योगी अपने को इस प्रकार सदा योग से जोड़े. तब मुझ मेँ रहने वाली परम निर्वाण शांति मिलती है.
नात्यश्नतस् तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः ।
न चाति-स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥
योग न तो जो बहुत खाने वाले को मिलता है और न बिल्कुल न खाने वाले को. न यह बहुत सोने वाले को मिलता है, न बहुत जागने वाले को.
युक्ताहार-विहारस्य युक्त-चेष्टस्य कर्मसु ।
युक्त-स्वप्नाऽऽवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥
यथायोग्य आहार, विहार, प्रयास, निद्रा और जागरण योग मेँ दुःखोँ का नाश करते हैँ.
यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य् एवावतिष्ठते ।
निःस्पृहः सर्व-कामेभ्यो युक्त इत्य् उच्यते तदा ॥१८॥
जब अच्छी तरह नियंत्रित चित्त केवल आत्मा मेँ लग जाता है, तभी कहा जाता है कि सब कामनाओँ से दूर हो कर मनुष्य योग मेँ स्थित है.
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यत-चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः ॥१९॥
हवा न चल रही हो, तो दीए की लौ न हिलती है, न काँपती है. मन को जीतने वाले योगी के मन की तुलना इसी से की गई है.
यत्रोपरमते चितं निरुद्धं योग-सेवया ।
यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्न् आत्मनि तुष्यति ॥२०॥
एक अवस्था ऐसी आती है जब योग के अभ्यास के द्वारा मन सब विषयोँ से हट जाता है, और योगी आत्मा के द्वारा आत्मा को देख कर आत्मा मेँ संतोष मनाता है…
सुखम् आत्यन्तिकं यत् तद् बुद्धि-ग्राह्यम् अतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश् चलति तत्त्वतः ॥२१॥
…तब वह योगी ऐसे अथाह और असीम आनंद का अनुभव करने लगता है जो इंद्रियोँ से परे है. यह आनंद शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है. इस अवस्था को अनुभव कर के वह मूल तत्त्व से विचलित नहीँ होता.
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥
इस अवस्था को पार कर लेने पर इस से बड़ा और कोई लाभ मालूम नहीँ पड़ता. बड़े से बड़ा दुःख इस अवस्था मेँ विचलित नहीँ करता.
तं विद्याद् दुःख-संयोग-वियोगं योग-सञ्ज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्ण-चेतसा ॥२३॥
योग से जुड़ने के बाद कर दुःख से कोई संबंध नहीँ रहता. योग की साधना निश्चय ही करने योग्य है. इस की साधना मेँ मन को उकताने से रोकना चाहिए.
सङ्कल्प-प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः ।
मनसैवेन्द्रिय-ग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥
फल की आशा से उत्पन्न होने वाली तमाम कामनाओँ को, चाहतोँ को, इस तरह और इतना त्याग दे कि कुछ भी शेष न रहे. सारी इंद्रियोँ को मन के द्वारा सब ओर से नियंत्रित कर ले.
शनैः शनैर् उपरमेद् बुद्ध्या धृति-गृहीतया ।
आत्म-संस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् ॥२५॥
धीरे धीरे विरक्त हो जाए. बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ ले और बड़े धैर्य से उसे आत्मा मेँ दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दे. किसी भी तरह का कोई और चिंतन न करे… मन को पूरी तरह ख़ाली कर दे.
यतो यतो निश्चरति मनश् चञ्चलम् अस्थिरम् ।
ततस् ततो नियम्यैतद् आत्मन्य् एव वशं नयेत् ॥२६॥
मन चंचल और अस्थिर है. जहाँ जहाँ भी वह जाता है, वहाँ वहाँ से उसे रोक कर वशपूर्वक, ज़बरदस्ती, आत्मा मेँ ही ले जाना चाहिए.
प्रशान्त-मनसं ह्येन योगिनं सुखम् उत्तमम् ।
उपैति शान्त-रजसं ब्रह्म-भूतम् अकल्मषम् ॥२७॥
इस प्रकार मन को शांत कर सकने वाले योगी को उत्तम सुख मिलता है. उस योगी का रजोगुण शांत हो जाता है. ब्रह्म के साथ एकाकार हो कर वह निष्कलंक हो जाता है.
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगत-कल्मषः ।
सुखेन ब्रह्म-संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते ॥२८॥
निष्कलंक हो कर योगी अपने को इस प्रकार सदा योग से जोड़े, तो बड़ी आसानी से ब्रह्म को पाने का परम सुख पा लेता है.
सर्व-भूतस्थम् आत्मानं सर्व-भूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योग-युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥
वह सब मेँ अपने आप को और अपने आप मेँ सब को देखने लगता है. इस प्रकार योग पाने वाला योगी सब ओर से समदर्शी हो जाता है.
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥
जिसे हर तरफ़ मैँ दिखाई देता हूँ, और जिसे मुझ मेँ सब दिखाई देते हैँ, उसे मैँ कभी नहीँ छोड़ूँगा, न वह मुझे छोड़ेगा.
सर्व-भूत-स्थितं यो मां भजत्य् एकत्वम् आस्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥
सब भूतोँ मेँ स्थित मुझे भजने वाला और एकत्व मेँ स्थित योगी सब प्रकार से विद्यमान होने पर भी मुझ मेँ ही निवास करता है.
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥
हर स्थिति मेँ वह हर एक को अपने जैसा और अपने बराबर मानता है. अर्जुन, सुख हो या दुःख, उस का समभाव डिगता नहीँ. ऐसे योगी को परम योगी माना गया है.
अर्जुनोवाच
योऽयं योगस् त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् ॥३३॥
अर्जुन ने कहा
आप ने यह साम्य योग का उपदेश दिया. मधुसूदन, चंचलता के कारण इस मेँ दृढ़ता से स्थिर रह पाना मुझे संभव दिखाई नहीँ देता.
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३४॥
कृष्ण, मन चंचल तो है ही, वह शक्तिशाली और कठोर आतयायी भी है. उसे बस मेँ रखना मुझे हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन मालूम पड़ता है.
श्रीभगवान् उवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥
श्री भगवान ने कहा
निस्संदेह, महाबाहु, मन चंचल है. उसे बस मेँ करना बहुत कठिन है. पर अभ्यास और वैराग्य से यह पकड़ मेँ आ सकता है.
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुम् उपायतः॥३६॥
अपने पर नियंत्रण नहीँ किया तो योग की प्राप्ति कठिन ही है. मेरा यही मत है. लेकिन अनेक उपायोँ से अपने को वश मेँ करने का प्रयत्न करने के योग को पाया जा सकता है.
अर्जुनोवाच
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच् चलित-मानसः ।
अप्राप्य योग-संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥३७॥
अर्जुन ने कहा
कोई पूरा प्रयत्न न करे, लेकिन मन श्रद्धा से भरा हो – अगर ऐसे आदमी का मन योग से बिचल जाए और वह सिद्धि को न पा सके, तो उस की क्या गति होगी?
कच्चिन् नोभय-विभ्राष्टश् छिन्नाभ्राम् इव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥३८॥
कहीँ वह दोनोँ ओर से भ्रष्ट तो नहीँ हो जाएगा? फटे बादल की तरह वह नष्ट तो नहीँ हो जाएगा? ब्रह्म के मार्ग से भटक कर उस का क्या होगा?
एतन् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य् अशेषतः ।
त्वद् अन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥
मेरे इस संशय को, कृष्ण, पूरी तरह काटिए. इस संशय को काटने वाला आप के अलावा कोई और है ही नहीँ.
श्रीभगवान् उवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस् तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥
श्री भगवान ने कहा
पार्थ, भटके योगी का नाश न यहाँ होता है, न वहाँ. मित्र, कल्याण करने वाले किसी जन की कभी कोई दुर्गति नहीँ होती.
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शास्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग-भ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥
पहले वह उन लोकोँ मेँ जाता है जहाँ पुण्यात्मा जाते हैँ. वहाँ काफ़ी समय बिताने के बाद योग से भटके मनुष्य का जन्म सदाचारी धनवानोँ के घर मेँ होता है.
अथवा योगीनाम् एव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशम् ॥४२॥
या फिर उस का अगला जन्म ज्ञानियोँ के कुल मेँ होता है. ऐसा पुनर्जन्म संसार मेँ किसी किसी को ही मिलता है.
तत्र तं बुद्धि-संयोगं लभते पौर्व-देहिकम् ।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु-नन्दन ॥४३॥
उस नए जन्म मेँ उसे अपने पिछले जन्म की बुद्धि और संस्कार मिलते हैँ, जिस से वह फिर सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है.
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुर् अपि योगस्य शब्द-ब्रह्माऽऽतिवर्तते ॥४४॥
पुराने अभ्यास के कारण नए जन्म मेँ भी वह बेबस सा योग के उसी मार्ग की ओर खिँचा चला जाता है. यह गति तो उस की होती है जो एक बार योग का अभ्यास आरंभ कर देता है. और जो मात्र जिज्ञासु होता है, जिस के मन मेँ योग को जानने की इच्छा जाग उठी होती है, वह भी वेदोँ मेँ बताए गए कर्मफलोँ से आगे निकल जाता है.
प्रयत्नाद् यतमानस् तु योगी संशुद्ध-किल्बिषः ।
अनेक-जन्म-संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् ॥४५॥
प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से योगी के पाप शुद्ध हो जाते हैँ. अनेक जन्मोँ के बाद वह सिद्धि पा लेता है. तब उसे परम गति मिल जाती है.
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश् चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन ॥४६॥
तपस्वियोँ से योगी को ऊपर माना गया है. योगी को ज्ञानियोँ और कर्मवीरोँ से भी ऊपर माना गया है. इस लिए, अर्जुन, तू योगी बन.
योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनाऽऽन्तरात्मना ।
श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥
सब योगियोँ मेँ भी अच्छा योगी उसे माना जाता है जो अपनी अंतरात्मा मुझ मेँ लगाता है. उस के मन मेँ श्रद्धा होती है. वह मुझे भजता है. उसे मैँ योगी मानता हूँ.
इति श्रीमद्-भगवद-गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म-विद्यायां योग-शास्त्रे श्री-कृष्णार्जुन-संवादे ध्यान-योगो नाम षष्ठोऽध्यायः
यह था श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद् ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मेँ ध्यान योग नाम का छठा अध्याय
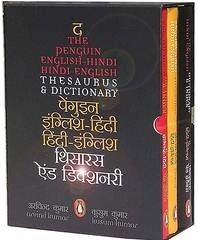
Comments