एक निजी विहंगावलोकन
—अरविंद कुमार
टाइम्स आफ़ इंडिया की वे प्रसिद्ध पत्रिकाएँ कहाँ हैँ, जो हिंदी का गौरव कहलाती थीँ. सब बंद हो गईं या कर दी गईं. हिंदी ही नहीँ, अँगरेजी के इलस्ट्रेटिड वीकली जैसे पत्र भी बंद करने पड़े. क्योँ?
किसी के मन मेँ पत्रिका निकालने का कीड़ा घर कर ले, तो उसे आप लाख समझाएँ, वह अख़बार निकाल कर ही रहता है… बाद मेँ उस मित्र से शुभचिंतक एक ही प्रश्न कर सकते हैँ – क्या हैँ तुम्हारे हाल?
ये बातेँ मैँ ने किसी को हतोत्साहित करने के इरादे से नहीँ कह रहा हूँ. मेरा उद्देश्य इतना ही है कि दुस्साहसी लोगोँ को पहले से ही सावधान कर दूँ. मैँ यह भी जानता हूँ कि जो लोग कुछ करना चाहते हैँ, वही कुछ कर दिखा सकते हैँ. तो पत्रपत्रिका आरंभ करने से पहले निम्न वातेँ जान लेना और उन के लिए पहले से तैयारी कर लेना ज़रूरी होता है…
पत्रपत्रिका का प्रकाशन कोई आसान काम नहीँ है. पत्रिका की घोषणा करते ही आप अपने को बाँध लेते हैँ कि हर सप्ताह या महीना आप उसे छापते रहेंगे. लेकिन कोई भी सावधिक प्रकाशन आत्मनिर्भर हुए बिना जीवित नहीँ रह सकता. यह बात पूरी तरह न समझ पाने के कारण ही अनेक मित्रोँ को आरंभिक संसाधन जुटा पाते ही पत्रिकाएँ आरंभ करते मैँ ने देखा है. कई को कई बार चेताया, समझाया, सलाह दी कि घरफूँक तमाशे मेँ हाथ मत जलाओ. पर वे नहीँ मानते. और कुछ महीनोँ बाद वे या तो पाठकोँ को कोसते नज़र आते हैँ कि अच्छी चीज़ की क़द्र करना नहीँ जानता; या किसी साझीदार को कोसते हैँ, जिस ने धोखा दिया; या विज्ञापकोँ की निंदा करते नहीँ थकते जो विज्ञापनोँ का ख़ज़ाना उन पर वारने को तैयार नहीँ होते… किसी मेँ तमीज़ ही नहीँ है, जो उन की बात समझ सके.
वे लोग भूल जाते हैँ कि किसी पत्रिका के लिए लेख मुफ़्त मेँ मिल सकते हैँ, संपादक के रूप मेँ आप अवैतनिक हो सकते हैँ, लेकिन काग़ज़ क़ीमत चुकाए बग़ैर नहीँ मिलता, छापेख़ाना वाला मित्र हुआ तो एक दो अंकोँ की छपाई ही उधारी पर कर सकता है. सब से बड़ी बात यह कि अख़बार बेचने वाले से आप बिकी प्रतियोँ के नाम पर एक भी पैसा हासिल नहीँ कर सकते. जान पहचान वालोँ से चंदा और कुछ विज्ञापन भी आप ले आए. लेकिन अख़बार चलाने के लिए विज्ञापन प्राप्ति की जो स्थायी व्यवस्था चाहिए होती है, वह अच्छा सरकुलेशन हुए बग़ैर नहीँ बन सकती. और सरकुलेशन बनने से पहले अख़बार के साँस उखड़ने लगते हैँ. अख़बार बंद हो जाता है.
मैँ जानता हूँ कि माधुरी, धर्मयुग, पराग, सारिका जैसी पत्रिकाओँ और नवभारत टाइम्स जैसे सफल प्रकाशनोँ के लिए टाइम्स आफ़ इंडिया जैसे संस्थान को कितना ज़ोर लगाना पड़ता था, फिर भी विज्ञापन पर्याप्त मात्रा मेँ नहीँ जुटते थे. (दस पंदरह साल पहले तक यही हालत थी. उन दिनोँ विज्ञापनदाता की नज़र मेँ हिंदी ग़रीबों की भाषा थी. हालात बदल रहे हैँ, लेकिन यह आज की या आने वाले कल की बात है.) अब टाइम्स आफ़ इंडिया की वे अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाएँ कहाँ हैँ, जो हिंदी का गौरव कहलाती थीँ. सब बंद हो गईं या कर दी गईं. हिंदी ही नहीँ, अँगरेजी के इलस्ट्रेटिड वीकली जैसे पत्र भी बंद करने पड़े. क्योँ?
सारी बातेँ मैँ निजी अनुभवोँ के आधार पर करूँगा. इसलिए यह लेख मेरी आत्मकथा जैसा लग सकता है. पर वादा है कि बात मेरी लगेगी, बात पत्रकारिता की होगी…
मेरा पत्रकारिता से पहला संपर्क
पत्रकारिता से मेरा बाक़ायदा संबंध तो 1949-1950 मेँ हुआ, लेकिन संपर्क सन 45 मेँ पहली अप्रैल को ही हो गया था, जब भविष्य मेँ निकलने वाली पत्रिका सरिता के प्रकाशकोँ और मुद्रकोँ के छापेख़ाने दिल्ली प्रैस मेँ छपाई का काम सीखने दाख़िल हुआ था. मैँ ने मैट्रिक की परीक्षा दी ही थी. यह तय था कि पारिवारिक आर्थिक परिस्थितिवश आगे नहीँ पढ़ पाऊँगा. कोई न कोई काम कर के घरख़र्च मेँ हाथ जुटाना होगा. तो परिणाम घोषित होने का इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा! तत्काल क्योँ नहीँ!
काम क्या हो, यह पिताजी ने तय किया. स्वंतत्रता सेनानी पिताजी मेरठ मेँ कई छापेख़ाने खोल कर, जेल जाने या आंदोलन मेँ सक्रिय होने पर साझीदारोँ पर छोड़े गए प्रैसोँ मेँ बार बार कंगाल हो कर जीवन मेँ असफल हो चुके थे. 1942 से दिल्ली मेँ एक बहुत निम्नस्तरीय नौकरी मेँ लगे थे. हाँ, प्रैस खोलने की तमन्ना दिल से गई नहीँ थी. पिताजी का तर्क था कि अपना प्रैस न भी खोल पाए तो मेरे हाथ मेँ कोई हुनर तो होगा. कभी भूखो मरने की नौबत ज़िंदगी भर नहीँ आएगी! बात पहले से कर ली गई थी.
परीक्षा 26 मार्च को समाप्त हुई थी और 1 अप्रैल 1945 को मैँ (कंपोज़िंग से पहले जो काम सीखा जाता है) डिस्ट्रीब्यूर का काम सीखने कनाट सरकस स्थित दिल्ली प्रैस मेँ दाख़िल हुआ—साथ मेँ थी शागिर्द बनाने की भेँट के तौर डिस्ट्रीब्यूशन के उस्ताद मुहम्मद शफ़ी के लिए लड्डुओँ से भरी परात और ग्यारह रुपए नक़द.
मेरे लिए पहली अप्रैल 1945 ऑल फ़ूल्स डे साबित नहीँ हुआ—यह आज 65 साल बाद 2010 मेँ मैँ दावे के साथ कह सकता हूँ. उन दिनोँ वहाँ से अँगरेजी पत्रिका कैरेवान निकला करती थी, और सरिता का समारंभ आधे साल बाद दशहरे पर अक्तूबर से होने वाला था. इस तरह (चाहे निम्नतम स्तर से ही सही) मुझे सरिता के समारंभ की प्रक्रिया को देखने का मौक़ा मिला और बरसोँ बाद मैँ संपादन विभाग मेँ विश्वनाथ जी का दाहिना हाथ बन गया. इस दौरान मैँ ने उस की प्रगति को निकट से देखा और भाग लिया.
1963 से मेरा संबंध मुंबई मेँ हिंदी पत्रकारिता के शिरोमणि माने जाने वाले संस्थान टाइम्स आफ़ इंडिया से माधुरी के संपादक के रूप मेँ चौदह वर्ष तक रहा. समांतर कोश बनाने की धुन मेँ मैँ 1978 मेँ वहाँ से पद त्याग कर दिल्ली फिर आ गया. फिर आर्थिक तंगी के कारण मेरा संबंध एक अत्यंत लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट से हुआ जिस के हिंदी संस्करण सर्वोत्तम का समारंभ मैँ ने ही किया, और उस के अमरीका स्थित संपादकीय कार्यालय मेँ रह कर उस की संपादकीय और प्रबंध व्यवस्था को निकट से देखने का दुर्लभ अवसर भी मिला.
इस लंबे अनुभव, और बाद मेँ आडिएंस की तरह मैँ पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता को देखने के आधार पर भीतर और बाहर से देखे सच को कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तकनीकी पक्ष मेँ आए परिवर्तनोँ के साथ साथ पत्रकारिता के भाव पक्ष – जिन दोनोँ को आजकल की नई भाषा मेँ हम हार्डवेअर और सौफ़्टवेअर कह सकते हैँ – पर संक्षेप मेँ लिखूँगा.
1945 से 2000 तक – तकनीक मेँ बदलाव
सब से बड़ा अंतर तकनीक मेँ हुआ है – कंपोज़िंग, ब्लाकमेकिंग, छपाई – सभी बदल गए हैँ. उस ज़माने मेँ कंपोज़िंग हाथ से होती थी. कंपोज़्ड मैटर को डिस्ट्रीब्यूट कर के फिर से उन ख़ानोँ मेँ डाला जाता था, जहाँ से कंपोज़ीटर एक एक अक्षर फिर से चुन कर स्टिक पर संजो कर गेली बनाता था. प्रूफ़रीडिंग और करक्शन के बाद गेलियोँ के प्रूफ़ों को चिपका कर संपादन विभाग डमी बनाता था, जिसे देख कर फिर कंपोज़ीटर पेज बनाता था. फिर प्रूफ़रीडिंग होती थी. कहीं कोई लाइन छूट गई है या अतिरिक्त पड़ गई है, तो उपसंपादक अपनी कारीगरी दिखा कर किसी तरह बने बनाए पेजोँ को वहीं का वहीं फ़िट करने का प्रयास करता था.
धीरे धीरे हाथ से कंपोज़िंग की जगह मोनोटाइप मशीन आई, जिस मेँ एक एक अक्षर का संयोजन मशीन करती थी, लेकिन करक्शन का काम हाथ से होता था. पेजोँ मेँ घट बढ़ करनी हो तो वही पुरानी रनऑन की समस्या आ खड़ी होती थी, यानी अगले कालम या पृष्ठ के मैटर को आगे पीछे करना. इस मेँ कई बार बने बनाए पेज टूट जाते थे. फिर से कंपोज़ करवाओ. इस का समय नहीँ होता था. अतः रनऑन से बचने के लिए उपसंपादक जहाँ की तहाँ मैटर फ़िट करता रहता था. फिर कई बार मशीन पर जाते जाते पेज टूट जाता था. यह महान संकट होता था. पूरा पेज दोबारा कंपोज़ करो, वह भी तत्काल! एक एक अक्षर की जगह पूरी लाइन एक साथ ढालने वाली लाइनोटाइप मशीन से मैटर टूट जाने की समस्या का हल तो कुछ आसान हुआ, लेकिन अधिकतर समस्याएँ पूर्ववत ही रहीं. मोनोटाइप और लाइनोटाइप का एक फ़ायदा और था. हैँड कंपोज़िंग मेँ छपते छपते टाइप टूट जाते थे. फिर भी टूटे टाइपों को फिर से काम मेँ लाना पड़ता था. छपाई उच्च स्तर की हो पाना बेहद मुश्किल था. मोनो और लाइनो मेँ यह कमी दूर हो गई थी—हर बार मशीन नया टाइप ढालती थी. टाइप को फिर से काम मेँ लाने के लिए एक एक अक्षर को फिर से कंपोज़िंग केसोँ मेँ डाला जाता था. यही काम मैँ ने सब से पहले सीखा था. इस प्रक्रिया मेँ अ अक्षर का टाइप ह अक्षर के ख़ाने मेँ भी डल जाता था. कई बार दो फ़ौंटों के कुछ टाइप भी ग़लत केस मेँ पहुँच जाते थे. प्रूफ़ रीडरोँ को आँखोँ का तेज़ होना पड़ता था कि हर रौंग फ़ौंट को पकड़ सके. ऐसी अन्य अनेक समस्याएँ तब छपाई और पत्रकारिता का अभिन्न अंग थीँ.
आज फ़ोटो टाइपसैटिंग का ज़माना है. कंपोज़िंग की कोल्ड मैटल (हाथ से कंपोज़िंग) या हौट मैटल (मशीन की ढलाई से कंपोज़िंग) कोई भी विधि हो, तैयार पेजोँ का भारी भरकम लैड का मैटर रखने के लिए गेलियोँ के रैक चाहिए होते थे. 100 पेजोँ की पत्रिका अगर एक साथ तैयार कर रखनी हो तो उस के लिए 100 गेलियोँ की ज़रूरत तो कम से कम थी, पेज बनने से पहले कंपोज़्ड गेलियोँ के लिए भी जगह चाहिए होती थी. टाइप के केसोँ के लिए जगह अलग दरकार थी. फिर प्रूफ़िंग मशीन के लिए जगह. पूरे 8 या 16 पेजी फ़रमोँ के प्रूफ़ निकालने के लिए स्टोन, वग़ैरा, लवाज़मात काफ़ी जगह घेरते थे. जगह की किफ़ायत के लिए पत्रिकाओँ और पुस्तकोँ का प्रकाशन टुकड़ोँ मेँ किया जाता था. आठ आठ या सोलह सोलह पेजोँ के फ़र्मों के हिसाब से कंपोज़िंग कराई जाती थी. अब फ़ोटो टाइपसैटिंग के ज़माने मेँ एक मेज़ पर यह सारा काम हो जाता है. मेरे समांतर कोश के 1,768 और तीन खंडों वाले बृहद् The Penguin English-Hindi/Hindi-English Thesaurus and Dictionary द पेंगुइन इंग्लिश-हिंदी/हिंदी-इंग्लिश थिसारस ऐंड डिक्शनरी के 3140 पेज ही नहीँ, तमाम शब्देश्वरी, विक्रम सैंधव, जूलियस सीज़र, सहज गीता… यही क्योँ तरह तरह के कोशोँ और विश्वकोशोँ के लाखोँ सचित्र पन्ने – कहना चाहिए एक पूरा पुस्तकालय – मेरी एक छोटी सी मेज़ पर छोटे से बक्से मेँ है, और उसी मेज़ पर पास ही स्कैनर रखा है जिस की सहायता से मैँ कोई भी चित्र छपने के लिए तैयार कर सकता हूँ, और एक प्रिंटर भी रखा है, जो प्रूफ़िंग मशीन का काम भी देता है, और पेजोँ को छपाई के लिए भी तैयार कर देता है… साथ साथ मेरे कंप्यूटर मेँ भारत की सभी लिपियोँ के सैकड़ोँ और अँगरेजी के हज़ारोँ लुभावने टाइपफ़ेस लोड हैँ… मेरे पिताजी यह क्रांति देखने के लिए ज़िंदा हो भी जाएँ तो हो सकता है ग़श खा कर फिर परलोक सिधार जाएँ!
हार्डवेअर शरीर है तो आत्मा है सौफ़्टवेअर
इस सब का – तकनीक का और साजसज्जा का – सीधा असर पत्रकारिता पर पड़ता है. मैँ एक पुराना उदाहरण देता हूँ. लाइनोटाइप मेँ एक बड़ी कमी यह थी कि उस के लिए जो हिंदी के फ़ेस बने, वे पढ़ने मेँ आसान और अच्छे नहीँ थे. इस विधि का उपयोग करने वाले दैनिक हिंदुस्तान और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे पत्रोँ के पाठकोँ के सामने यह बड़ी समस्या रहती थी, और इन पत्रोँ को पढ़ने को मन नहीँ करता था. इन संस्थानोँ ने अपने अज्ञान या अड़ियलपन के कारण समस्या का निदान नहीँ किया. परिणाम यह हुआ कि दूसरे पत्र अधिक लोकप्रिय होते चले गए. साप्ताहिक हिंदुस्तान तो बंद ही हो गया. हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी पत्रोँ को जो क्षति तब हुई उस का ख़मियाज़ा दसियोँ साल भुगतते रहे. कंप्यूटर युग मेँ आ कर अब हिंदुस्तान फिर उभरा है, और मृणाल पांडे ने तो उसे नई पीढ़ी की तमाम आकांक्षाओँ की पूर्ति का साधन बना कर लोकप्रियता के नए शिखर तक पहुँचा दिया था.
अभी तक मैँ ने कंपोज़िंग की बात की. उस के साथ ही छपाई के क्षेत्र मेँ क्रांति पर क्रांति हो रही थी. कहाँ मेरे बाचपन का वह ज़माना जब मेरठ मेँ हमारे प्रेस मेँ ट्रेडल मशीन पर छोटे छोटे फ़रमे छपते थे, या फ्लैटबैड मशीन पर बड़े फ़रमे हाथ से दबा कर छापे जाते थे, और कहाँ उन्हीँ दिनोँ के बड़े प्रैसोँ की सिलंडर मशीनोँ और हौट मैटल रोटरी मशीनेँ, जो फ़ोटोग्रेव्योर रोटरी के रास्ते आफ़सैट छपाई के सहारे विशाल रोटरियोँ तक पहुँच गई हैँ.
हार्डवेअर पत्रकारिता का शरीर है, तो सौफ़्टवेअर आत्मा. सौफ़्टवेअर का सीधा संबंध पाठक से और परिवर्तनशील समाज से है, और इस बात से है कि कोई पत्रिका अपने पाठकोँ को बदलते समय मेँ संतुष्ट कर पा रही है या नहीँ? उस पत्रिका के पीछे संपादकोँ की अपने पाठक वर्ग की कोई समझ है या नहीँ, और वह समाज के साथ साथ अपने पाठकोँ की बदलती आवश्यकताओँ को पूरा कर रही है या नहीँ?
सरिता का पत्रकारिता पर प्रभाव
सरिता का प्रकाशन अक्तूबर 1945 मेँ आरंभ हुआ. कोल्ड मैटल तकनीक से, लगभग दस सालोँ मेँ यह अपने संचालक-संपादक विश्वनाथ जी की (जिन्हें मैँ अपना गुरु भी मानता हूँ) दूरदर्शिता के कारण यह मोनोटाइप तकनीक तक पहुँच गई. वह इसे लाइनोटाइप के अस्पष्ट टाइप तक नहीँ ले गए – यह भी उन की समझ का परिणाम था.
सन 45 से पहले हिंदी मेँ लोकप्रियता के शिखर पर थी माया . इलाहाबाद से निकलने वाली माया कहानी पत्रिका थी. उन दिनोँ कोई भी आदमी सफल पत्रिका निकालने की बात मन मेँ लाता, तो वह माया जैसी पत्रिका निकालना चाहता था. कुछ अन्य लोकप्रिय और उल्लेखनीय पत्रिकाएँ हुआ करती थीँ – सरस्वती जिस ने हिंदी को कभी नए आयाम दिए थे, और मानक हिंदी बनाने मेँ जिस का बड़ा हाथ था, चाँद जो स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार का झंडा भी खड़ा करता था. और भी अनेक पत्रिकाओँ के नाम लिए जा सकते हैँ. धार्मिक साहित्य के लिए कल्याण था ही. कुछ लोकप्रिय साप्ताहिक भी थे. कुछ वर्ष बाद निकला नवयुग, बाद मेँ जिस के सफल संपादक बने महावीर अधिकारी, जो मुंबई मेँ नवभारत टाइम्स के अत्यंत सफल संपादक सिद्ध हुए.
यहाँ यह बात भी ध्यान मेँ रखनी चाहिए कि बहुत शीघ्र – दो साल से भी कम समय मेँ – भारत स्वाधीन होने वाला था, और स्वाधीनता के साथ साथ देश का विभाजन भी होने वाला था. उस से देश मेँ, समाज मेँ, पाठक वर्ग मेँ भारी परिवर्तन आने वाला था.
ऐसे मेँ ही आई थी सरिता, बदलते समय और समाज की बदली रुचि मेँ ढलने को तैयार. मैँ अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि आरंभ मेँ सरिता की परिकल्पना माया जैसी किसी कहानी पत्रिका की थी. नक़ल को चलाना आसान नहीँ होता. यह हिंदी पाठक वर्ग और पत्रकारिता का सौभाग्य था कि बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए सरिता को माया की नक़ल नहीँ बनाया गया, बल्कि उस का आदर्श चाँद को बनाया. लेकिन चाँद का रूप आकार नहीँ, और सौफ़्टवेअर भी पूरी तरह चाँद का नहीँ.
यहाँ कुछ शब्द सरिता के प्रकाशक संपादक विश्वनाथ जी के बारे मेँ कहना अनुपयुक्त नहीँ होगा. संपादक का व्यक्तित्व किसी पत्रिका की परिकल्पना मेँ, और उस के लोकप्रिय होने या न होने मेँ महत्त्वपूर्ण योगदान करता है. एकमात्र कारण उसे हम नहीँ कह सकते, क्योँकि सही संचालन प्रतिभा और व्यावसायिक संगठन की भी आवश्यकता होती है. इस के साथ साथ आवश्यक होती है एक तटस्थता, तट पर खड़ा होने का भाव, तट जिस पर खड़ा हो कर कोई बहती नदी को देख सकता है, अपने को उस से अलग रख कर.
जैसा कि मैँ ने पहले बताया दिल्ली प्रैस से अँगरेजी पत्रिका कैरेवान निकलती थी. वह बड़ी सफल पत्रिका थी. कह सकते हैँ कि उस समय की एकमात्र लोकप्रिय भारतीय अँगरेजी पत्रिका थी. इलस्ट्रेटिड वीकली था, लेकिन वह अँगरेजोँ का था. कैरेवान की संपूर्ण परिकल्पना विश्वनाथ जी की अपनी थी. वह शिक्षा दीक्षा से चार्टर्ड अकाउनटैंट थे. साहित्यकारोँ को बड़ा अजीब लगता है कि कोई चार्टर्ड अकाउनटैंट सफल पत्रकार कैसे बन गया! लेकिन चिंतन मनन पर केवल साहित्यकारोँ का एकाधिकार होगा, ऐसा कोई नियम न तो है, न हो सकता है. पढ़ाई पूरी कर के वह अपने पिता अमरनाथ के छोटे से दिल्ली प्रैस मेँ सहायता करने आए थे. प्रैस के ख़ाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होँ ने कैरेवान निकाला था. वह लोकप्रिय हो गया. कारण – उस मेँ प्रकाशित होने वाले विषयोँ का चुनाव और संतुलन. यहाँ तटस्थता की आवश्यकता होती है. आम आदमी के लिए निकाला जाने वाला पत्र किसी आंदोलन का मुखपत्र नहीँ होता, लेकिन उस का अपना एक दृष्टिकोण फिर भी हो सकता है. साथ ही यह भी सही कि आंदोलन विशेषोँ के पत्र भी सफल हुए हैँ. जैसे गाँधी जी का हरिजन . लेकिन आंदोलन की सटीकता काल तक ही.
प्रकाशनीय सामग्री पर विश्वनाथ जी का दृष्टिकोण स्पष्ट था
विश्वनाथ जी के लिए पत्र मेँ प्रकाशित होने योग्य सामग्री वही है, जो उन के अपने पाठक के लिए रोचक हो या लाभप्रद, जिस का उस के जीवन से सरोकार हो. इस का अर्थ यह भी है कि आम आदमी की पत्रिका किसी तकनीकी विषय की पत्रिका नहीँ होती. इंजीयरिंग विषय पर कोई पत्रिका हो तो हम यह आशा नहीँ करनी चाहिए कि आम आदमी भी उसे पढ़ेगा. विज्ञान की पत्रिका दो तरह की हो सकती हैँ – वैज्ञानिकोँ के लिए निकाली जाने वाली पत्रिका या आम आदमी को विज्ञान की जानकारी देने वाली पत्रिका. यही बात हम साहित्य और साहित्यक पत्रिकाओँ पर लागू कर सकते हैँ. कैरेवान बाद मेँ असफल क्योँ हुआ, यह बात मैँ सही अवसर आने पर करूँगा.
45 मेँ जब विश्वनाथ जी ने सरिता निकाली (प्रकाशक के तौर पर; पहले कुछ महीने उस के संपादक थे विश्वनाथ जी के अभिन्न मित्र विजय नारायण जी; संपादन की वैचारिकता मेँ दोनोँ का साझा योगदान था), तो उसे कैरेवान से बिल्कुल अलग ढाँचे मेँ रखा गया. विश्वनाथ जी बख़ूबी जानते थे, अँगरेजी का नुस्ख़ा हिंदी मेँ नहीँ चलेगा. सरिता निकली एक नए आकार के साथ (यह अब तक वही है) और नई साजसज्जा के साथ (इस मेँ अब तक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीँ हुआ है). विश्वनाथ जी आकार शायद रीडर्स डाइजैस्ट जैसा रखना चाहते थे, लेकिन उस के लिए उपयुक्त साइज़ का काग़ज़ युद्धकालीन तंगी के उन दिनोँ उपलब्ध नहीँ था. अतः उस के निकटतम जो साइज़ हो सकता था, वह स्वीकार कर लिया गया. पुस्तक जैसा, लेकिन अलग, माया के, चाँद के, सरस्वती के, स्वयं कैरेवान के आकार से अलग, अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला आकार, जिसे कोई आसानी से हाथ मेँ ले कर पढ़ सके. इस आकार मेँ वैसी साजसज्जा संभव नहीँ थी, जो बड़े आकार के लाइफ़ या गुड हाउसकीपिंग जैसे अमरीकी पत्रोँ मेँ होती थी. लेकिन सुरुचिपूर्णता संभव थी.
सरिता के सौफ़्टवेअर पक्ष पर जाने से पहले मैँ व्यावसायिक नीति पर भी दो एक बातेँ कहूँगा – ये पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग हैँ. बिकरी और विज्ञापन की व्यवस्था धीरे धीरे कैरेवान के समय से विकसित होती आ रही थी, सरिता के आने से उस का विकास करने मेँ और सहायता मिली.
इस से भी बड़ी बात यह थी कि हर रचना पर लेखकोँ को पारिश्रमिक – वह भी प्रकाशित होने पर नहीँ, स्वीकृत होते ही. हिंदी के लिए यह नई बात थी. आज तक हिंदी की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ पारिश्रमिक नहीँ देतीँ. जो देती हैँ, वह बहुत कम. मुझे याद है कि सन 45 मेँ सरिता मेँ प्रकाशन के लिए स्वीकृत हर लेख और कहानी पर 75 रुपए अग्रिम दिए जाते थे – उस ज़माने मेँ यह बहुत बड़ी रक़म थी. यही नहीँ, कभी कोई कहानी बहुत लोकप्रिय हो गई तो विश्वनाथ जी ने लेखक को उतनी ही अतिरिक्त रक़म बाद मेँ भेजी, निजी पत्र और प्रशंसा के साथ. ऐसी ही एक कहानी थी स्वर्गीय श्री आनंद प्रकाश जैन की साँग. (आनंद प्रकाश जी बाद मेँ टाइम्स द्वारा प्रकाशित बालपत्रिका पराग के संपादक बने.)
सरिता का दृष्टिकोण एक पढ़े लिखे आधुनिक मध्यमवर्गीय हिंदी भाषी हिंदू जैसा था, जो दक़ियानूस नहीँ था, जो हिंदू समाज को पुराना गौरव लौटाना चाहता था और इसी उद्देश्य से जो समाज के पुराने पाखंड को उखाड़ फेंकना चाहता था, स्त्रियोँ को जाग्रत करना और सम्मान दिलाना चाहता था, जिसे रोचक कहानियाँ पढ़ने मेँ रुचि थी, जो सहज काव्य से विह्वल होना चाहता था. मुझे याद है कि सरिता के पहले अंक मेँ ही एक लेख था – मठमंदिर और सामाजिक प्रगति. साथ ही स्त्रियोँ के लिए उपयोगी सामग्री थी. सब से बड़ी बात यह थी कि सामग्री मेँ दंभ नहीँ था, पाठक को विद्वत्ता से या शैली से आतंकित करने की इच्छा नहीँ थी, उसे अपने साथ ले कर चलने की भावना थी. साहित्यिक उदाहरण देँ तो इस अंतर को हम तुलसीदास और केशवदास के काव्य का अंतर कह सकते हैँ. दोनोँ ही रामभक्त अच्छे कवि हैँ, लेकिन महान तुलसीदास हैँ.
भाषा के बारे मेँ विश्वनाथ का दिमाग़ पूरी तरह साफ़ था. अपने ही उदाहरण से बताता हूँ, वह मेरे लिखे से ख़ुश रहते थे. मेरे सीधे सादे वाक्य उन्हेँ बहुत अच्छे लगते थे. लेकिन कई शब्द? एक दिन उन्होँ ने मुझे अपने कमरे मेँ बुलाया, पूछा, "क्या तेली, मोची, पनवाड़ी, ये ही क्योँ क्या आम आदमी, विद्वानोँ की भाषा समझ पाएगा? क्या यह विद्यादंभी विद्वान तेली आदि की भाषा समझ लेगा?" स्पष्ट है मेरे पास एक ही उत्तर हो सकता था: विद्वान की भाषा तो केवल विद्वान ही समझेँगे, आम आदमी की भाषा समझने मेँ विद्वानोँ को कोई कठिनाई नहीँ होगी. थोड़े से शब्दोँ मेँ विश्वनाथ जी ने मुझे संप्रेषण का मूल मंत्र सिखा दिया था. जिस से हम मुख़ातिब हैँ, जो हमारा पाठक श्रोता दर्शक आडिएंस है, हमेँ उस की भाषा मेँ बात करनी होगी.
मुझ से उस संवाद का परिणाम था कि विश्वनाथ जी ने सरिता मेँ नया स्थायी स्तंभ जोड़ दिया: यह किस देश प्रदेश की भाषा है? इस मेँ तथाकथित महापंडितोँ की गरिष्ठ, दुर्बोध और दुरूह वाक्योँ से भरपूर हिंदी के चुने उद्धरण छापे जाते थे. उन पर कोई कमैँट नहीँ किया जाता था. इस शीर्षक के नीचे उन का छपना ही मारक कमैँट था.
विश्वनाथ जी की स्पष्ट नीति थी—रचनाएँ अपने तकनीकी कौशल से पाठक को आतंकित न करें, बल्कि उस से उस की भाषा मेँ बातचीत करती हुई उसे अपने साथ साथ आगे बढ़ाएँ.
सरिता मेँ अनेक तत्कालीन बड़े लेखकोँ ने लिखा, और अनेक भावी बड़े लेखकोँ ने सरिता मेँ लिख कर ही हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. स्वर्गीय मोहन राकेश ने तो सरिता के एक अंक का संपादन भी किया था. लेकिन सरिता ने अपने आप को साहित्यिक वाद विवाद से, उठा पटक से अपने आप को हमेशा दूर रखा. यही कारण है कि अनजाने लेखकोँ की अनगिनत रचनाएँ सरिता मेँ छपीँ और छप रही हैँ.
ये रचनाएँ कैसी होती थीँ, पाठक से क्या कहती थीँ – यही है सरिता के सौफ़्टवेअर पक्ष की असली पहचान. उन सब का सीधा संबंध पाठक के जीवन से होता था, चाहे कहानी हो या कविता या लेख, और उस सब मेँ एक सुविचारित विविधता होती थी. यह विविधता अनेक स्तरोँ पर होती थी, जैसे विषय, देश, काल, समाज, वय, लिंग… जिस से पूरे हिंदी क्षेत्र के बच्चोँ, बूढ़ों, जवानोँ, स्त्रीपुरुषोँ को अपनी रुचि की पाठ्य सामग्री मिल जाए, वह भी सहज समझ मेँ आने वाली भाषा मेँ.
विविधता, विविघता, विविधता…
यहाँ मैँ विविधता के उदाहरण देना चाहूँगा. मान लीजिए किसी एक अंक मेँ सात कहानियाँ हैँ. तो उन मेँ से एक या दो का विषय होगा पारिवारिक समस्याएँ, विशेषकर गृहणियोँ के अपने जीवन की समस्याएँ, एक का समाज सुधार; एक कहानी ऐतिहासिक होगी, तो एक विज्ञान कथा, एक कोरी कल्पना की उड़ान या हास्य व्यंग्य. अब इन विषयोँ का संतुलन किया जाएगा लेखोँ से. कुछ लेखोँ मेँ जीवन सुधारने वाली जानकारी होती थी. कुछ मेँ मात्र मनोरंजन. कुछ मेँ यात्रा. लेकिन लेखोँ मेँ सामाजिक सुधार का पक्ष अधिक प्रबल होगा, जीवन की ज्वलंत समस्याओँ को छुआ जाएगा. महापुरुषोँ की जीवनियोँ से नवयुवकोँ को प्रेरित किया जाएगा. (स्वयं मैँ ने महापुरुषोँ पर एक लेखमाला लिखी थी. सामग्री का सुझाव कभी विश्वनाथ जी देते थे, कभी मैँ प्रस्तावित करता था.) छोटे छोटे चुटकुले होंगे, फ़िलर होंगे, सूक्तियाँ होंगी… कुल मिला कर सब रचनाओँ मेँ क्षेत्रीय संतुलन होगा—उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम भारत तो होंगे ही, विश्व के भिन्न क्षेत्र भी पाठक को बिना बताए विविधता की झलक देँगे.
मान लीजिए भारत के विभाजन का काल है. उन दिनोँ समाचार पत्रोँ मेँ पाकिस्तान से भाग कर आती महिलाओँ पर यौन अत्याचारोँ के विवरण भरे रहते थे. जो महिलाएँ आ रही थीँ, उन के दुःखोँ की कहानियाँ मुँहज़बानी घर घर तक पहुँच रही थीँ. आज आप के ज़ेहन मेँ उस ज़माने की वह हिंदू मानसिकता नहीँ आती, जिस के रहते हर उस महिला को परित्यक्त कर दिया जाता था, जिस ने अपनी इच्छा से या मजबूरी मेँ जिस के साथ कोई यौन अतिक्रमण किया गया हो. यौन अतिक्रमण तो बड़ी बात है, कोई विधर्मी अगर किसी अबला को छू भी लेता था, तो उस महिला का परित्याग कर दिया जाता था. ऐसी ”कुलटाओँ” को या तो वेश्या बनना पड़ता था या मुसलमान या ईसाई. संकुचित हिंदू समाज मेँ उन के लिए कोई स्थान नहीँ था.
ऐसे मेँ सरिता मेँ उन लेखोँ की बाढ़ आ गई, जिन मेँ इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती थी. यह बताया जाता था कि इस मेँ बलात्कृत महिला का कोई दोष नहीँ है, अगर किसी का दोष है तो उस पति का जो उस की रक्षा नहीँ कर पाया और उस समाज का जो उसे सम्मान सहित स्वीकार नहीँ कर रहा. आज आप नहीँ समझेँगे, लेकिन उस समय यह कहना साहस का काम था. ऐसी रचनाओँ ने, कहानियोँ ने, लेखोँ ने, पाठकोँ के मन को छुआ. मैँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरिता ने समाज का दृष्टिकोण बदलने मेँ सब से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई. यहाँ तक कि सीता बनवास का सवाल वहीं से उठना शुरू हुआ. लिखा गया कि यदि रावण सीता को ले गया तो दोष सीता का नहीँ था, रावण का था. सीता को इस अतिक्रमण की सज़ा किस लिए दी गई? यह राम का अन्याय था, जो उन्होँ ने बाद मेँ सीता को बनवास दिया. सन 47-48-49 मेँ सरिता द्वारा प्रचारित यही मानसिकता थी, जिस की झलक हमेँ राज कपूर की फ़िल्म आवारा मेँ शैलेंद्र के गीत किया कौन अपराध त्याग दई सीता महतारी (मैँ ने जो शब्द उद्धृत किए हैँ, वे शायद कुछ भिन्न हैँ, लेकिन भाव यही था) मेँ मिली. बाद मेँ कुछ इन्हीँ भावोँ को व्यक्त करना वाला एक गीत हमेँ बिमल राय की बिराज बहू मेँ मिला. बहुत पहले रामराज्य फ़िल्म मेँ विजय भट ने एक गीत मेँ बोल रखे थे—यही राम दरबार कहाँ वैदेही. और कुछ बाद यही भाव मेरी कविता राम का अंतर्द्वंद्व का विषय बना.
शीर्ष पत्रकार
लोग विश्वनाथ जी को कोई ऐसा व्यक्ति समझते हैँ, जो व्यावसायिकता के लिए, अपनी पत्रिका की बिकरी बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म विरोधी उत्तेजक रचनाएँ प्रकाशित करता था. लेकिन ऐसा था नहीँ. हिंदू समाज कमज़ोर हुआ अपने मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासोँ के कारण. आक्रांताओँ ने अपनी सेनाओँ के आगे गाएँ खड़ी कर दीं, और रक्षक राजपूतोँ ने तीर नहीँ चलाए! ऐसी गोभक्ति और गोसेवा क्या है? मूर्खता! इस के लिए विश्वनाथ जी ने मेरे स्वर्गीय मित्र रतनलाल बंसल को भाँति भाँति की संदर्भ सामग्री दे कर आज का सब से बड़ा देशद्रोह गोहत्या लेख लिखवाया. जो रूढ़िवादी थे, उन्होँ ने तूमार खड़ा कर दिया. विश्वनाथ जी अडिग खड़े रहे. आम पाठक सरिता के साथ रहा. उस ने उसे समर्थन दिया. यही बात मैँ ने 1957 मेँ देखी जब विश्वनाथ जी मेरी कविता राम का अंतर्द्वंद्व के समर्थन मेँ पत्थर की चट्टान की तरह खड़े रहे, न कार्यालय पर तोड़फोड़ की परवाह की, न पथराव की, न आगज़नी की, न मारे जाने की धमकी की, न लंबे चलने वाले मुक़दमे की.
हिंदी मेँ मुझे उन जैसा कोई पत्रकार दिखाई नहीँ देता, जो अपनी पत्रिका के द्वारा बात करता हो, भाषणोँ और वक्तव्यों के द्वारा नहीँ. मुझ से पिछले साठ वर्षोँ का शीर्ष हिंदी पत्रकार चुनने को कहा जाए तो मैँ उन्हेँ ही चुनूँगा. उन के व्यक्तित्व ने पत्रिका को बनाया, और पत्रिका ने उन के व्यक्तित्व को. अन्यथा हम क्या देखते हैँ? संपादक बनते ही लोग नेताओँ के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैँ, और अपना निजी प्रचार करते घूमते रहते हैँ. विश्वनाथ जी कभी अपने दफ़्तर से बाहर नहीँ निकले, किसी नेता से कुछ नहीँ माँगा. उन्हेँ जो कुछ चाहिए था अपने पाठक से चाहिए था. उन्हेँ जो कुछ देना है अपने पाठक को और उस के द्वारा अपने समाज को देना है. ख़ैर, समाज मेँ भाँति भाँति के लोग होते हैँ. सभी अपने अपने तरीक़े से काम करते हैँ.
मुझे गर्व है कि पत्रकारिता का पाठ मैँ ने देश की स्वाधीनता के समय से ही सरिता मेँ अनेक पदोँ पर काम करते करते विश्वनाथ जी से सीखा. उन से अनेक मतभेदोँ के बावजूद वह मेरे गुरु हैँ और रहेंगे. मुझे गर्व है कि उन से सीखे पाठोँ के बल पर मैँ 1963 मेँ मुंबई गया – टाइम्स आफ़ इंडिया के लिए हिंदी की फ़िल्म पत्रिका सुचित्रा (बाद मेँ परिवर्तित नाम माधुरी) का समारंभ करने.
लेकिन इस से पहले दो तीन बातेँ और कहनी हैँ. सन 55 मेँ मैँ ने शाम के समय पढ़ते पढ़ते अँगरेजी मेँ ऐमए पास कर लिया था. उस से बहुत पहले ही विश्वनाथ जी ने मुझे कैरेवान मेँ पहले तो उपसंपादक और बाद मेँ सहायक संपादक बना दिया था. वहाँ मुझे संपादन कला मेँ अनेक प्रयोग करने का सुअवसर मिला. सजग देखरेख विश्वनाथ जी की थी, लेकिन अपने विचारोँ को अपने तरीक़े से क्रियान्वित करना मेरे अपने हाथ मेँ था.
उन दिनोँ कैरेवान संकट से गुज़र रहा था. अमरीका से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओँ (एक ओर लाइफ़, टाइम, न्यूज़वीक, तो दूसरी ओर लेडीज़ होम जर्नल, गुड हाउसकीपिंग, कास्मोपोलिटन) से बिकरी को चुनौती मिल रही थी. कभी हम कैरेवान को इस दिशा मेँ मोड़ते, तो कभी उस दिशा मेँ. न पाठक समझ पा रहा था कि हम क्या हैँ, और न स्वयं हम. नौबत कैरेवान को बंद करने के विचार तक आ गई थी. ऐसे मेँ एक दिन मैँ ने, काफ़ी दिनोँ के विचारमंथन के बाद, विश्वनाथ जी से कहा कि एक क्षेत्र ऐसा है, जहाँ अमरीकी पत्रिकाएँ हमेँ चुनौती नहीँ दे सकतीँ, वह है – भारत और भारत का समाज, भारत की राजनीति. हमेँ लेआउट और सामग्री मेँ अमरीकी पत्रिकाओँ के अनुकरण से हट कर सीधी सादी साजसज्जा के साथ अपनी सार्थक सामयिक सामग्री को स्थान देना चाहिए, तभी हम अपने लिए अलग राह बना पाएँगे.
विश्वनाथ जी ने सोचने मेँ एक पल का समय भी नहीँ लगाया. शायद अपने निजी चिंतन से वह भी इसी नतीजे पर पहुँच चुके थे. सारी ज़िम्मेदारी मुझे सौँप दी गई. मैँ ने तत्काल अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया. एक ही साल मेँ कैरेवान की बिकरी दोगुनी हो गई. विविधता वही सरिता वाली, लेकिन विषयोँ का चुनाव भारत के अँगरेजी पाठक को आंदोलित करने वाले प्रश्नोँ पर. आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक. उन दिनोँ अँगरेजी साप्ताहिक लिंक निकलता था. वह पूरी तरह वामपंथी था. अतः उस की सामग्री मेँ सीमाएँ थीँ. वह एक दृष्टिकोण के समर्थकोँ के ही काम की थी. कुछ और साप्ताहिक और पाक्षिक थे, अब नाम ठीक से याद नहीँ आ रहे. शायद एक था फ़ोरम. इलस्ट्रेटिड वीकली था, वही पुराना अँगरेजी ढर्रे का और कला पक्षोँ पर ज़ोर देता हुआ (तब उस की लोकप्रियता का मुख्य आधार थे वर्गपहेली और नवदंपतियोँ के फ़ोटो!). (बाद मेँ मैँ ने देखा कैसे ख़ुशवंत जी ने उसे एक बिल्कुल नए भारतीय साँचे मेँ ढाल सफलता के नए झंडे गाड़े. उन के बाद कोई इलस्ट्रेटिड वीकली के गौरव को मेनटेन नहीँ कर सका.) उन के बीच मेँ कम साधन वाले कैरेवान को फिर से जगह दिला पाना आसान नहीँ था.
बाद मेँ कैरेवान का यह फ़ारमूला पहले पाक्षिक और अब साप्ताहिक इंडिया टुडे ने अपनाया और सफलता पाई. उस के पास साधन बड़े थे, सामग्री जुटाने के लिए भरपूर धन ख़र्च करने का साहस था, जो विश्वनाथ जी कभी नहीँ दिखा पाए. परिणाम सामने है – कैरेवान का नाम बदल कर ऐलाइव हो गया. मैँ ने वह पत्रिका, ऐलाइव, आज तक नहीँ देखी, इस लिए उस पर कमेंट करना मैँ ठीक नहीँ समझता. मेरी अपनी धारणा है कि वह ज़्यादा नहीँ बिक पाता होगा – क्योँ कि कहीं उस का चर्चा दिल्ली प्रैस की ही वूमैन्स ऐरा या गृहशोभा जैसा नहीँ सुना. आश्चर्य नहीँ कि अब फिर हो गया वही कैरेवान.
अक्षय कुमार जैन
तो, नवंबर 1963 मेँ मैँ मुंबई पहुँचा. वहाँ पुराने मित्र केवल दो थे. मुनीश नारायण सक्सेना और नंदकिशोर नौटियाल. दोनोँ हिंदी ब्लिट्ज़ मेँ थे – संपादक और सहायक संपादक. पुराने परिचित थे महावीर अधिकारी, नवभारत टाइम्स के मुंबई संपादक.
हिंदी पत्रकारिता का कोई भी ज़िक्र नवभारत टाइम्स के उदय और उस मेँ स्वर्गीय अक्षय कुमार जैन और महावीर अधिकारी की बात किए बिना बेमानी रहेगा. हिंदी दैनिकोँ मेँ दिल्ली मेँ दैनिक हिंदुस्तान था. मेरा पहला लेख इसी के साप्ताहिक संस्करण मेँ पंडित गोपाल प्रसाद व्यास ने स्वीकृत किया था. शायद सन 50 मेँ, या 51 मेँ. विभाजन के बाद वीर अर्जुन और हिंदी मिलाप थे. मानसिकता और विषयवस्तु मेँ वे अभी तक हिंदुत्व से और पंजाब से बाहर नहीँ निकल पाए, और उन मेँ विभाजन से संबंधित राजनीति का प्रभाव अधिक झलकता था. दिल्ली मेँ पंजाब केसरी का आगमन बहुत बाद मेँ हुआ. वह अभी तक पंजाबी महाशयोँ वाली मानसिकता से निकल नहीँ पाया है, लेकिन अपनी लोकप्रियता के फरफराते झंडे उस ने गाड़ रखे हैँ. हिंदी दैनिकोँ मेँ मैँ नई दुनिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका जैसे पत्रोँ का नाम लेना चाहूँगा, जिन्हों ने राष्ट्रीय और स्थानीय समाचारोँ मेँ कमाल का संतुलन दिखा कर छोटे छोटे शहरोँ से सफल संस्करण निकाले हैँ और नवभारत टाइम्स को कड़ी चुनौती दी. कहना चाहिए कि उस के दाँत खट्टे कर दिए . 21वीँ सदी मेँ नवभारत टाइम्स ने एक बार फिर बढ़त हासिल की. लेकिन पूरी नहीँ.
तो अक्षय जी –
मेरी उन से पहली मुलाक़ात 1957 मेँ तब हुई जब राम का अंतर्द्वंद्व के विरुद्ध दैनिक पत्रोँ मेँ मेरे ख़िलाफ़ ज़हर उगला जा रहा था. उन से मिलाने ले गए थे मुझे मेरे घनिष्ठ मित्र और सहकर्मी चंद्रमा प्रसाद खरे. अक्षय जी से मिलने से पहले हम दैनिक हिंदुस्तान के संपादक श्री मुकुट बिहारी वर्मा के पास गए थे. वर्मा जी और मैँ एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचानते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान के कार्यालय मेँ मेरे मित्र रामानंद दोषी और संपादक श्री बाँकेबिहारी भटनागर के पास मेरा आना जाना होने के कारण. हम वर्मा जी से सिर्फ़ यह कहना चाहते थे कि मुझे भी अपने बचाव मेँ कुछ कहने का मौक़ा दिया जाए. लेकिन वर्मा जी तो हमारी बात सुनने से पहले ही भड़क उठे और बुरा भला कहने लगे. दूसरी ओर भाई साहब (अक्षय जी) ने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि अपनी बात उन के पत्र के द्वारा कहने का हमारा पूरा अधिकार है. मुझ जैसे ”बदनाम” लेखक को उन का यह आश्वासन देना मेरी नज़र मेँ बड़ी बात थी. मेरे मन मेँ उन का सम्मान स्थापित हो गया और यह मुलाक़ात हम दोनोँ के बीच अग्रज और अनुज का रिश्ता बनाने मेँ सहायक हुई. इस के 6 साल बाद यह मुलाक़ात ही मुझे टाइम्स आफ़ इंडिया के मुंबई कार्यालय बोरीबंदर तक पहुँचाने का माध्यम बनी. पता नहीँ भाई साहब ने मुझ मेँ क्या देखा जो स्वर्गीय श्रीमती रमा जैन और साहू शांति प्रसाद जैन को उन्होँ ने 33-वर्षीय युवक को एक बिल्कुल नई पत्रिका का भार सौँपने के लिए राज़ी करा लिया.
विश्वनाथ जी की ही तरह अक्षय जी भी पत्रकारिता मेँ पांडित्य प्रदर्शन की बजाए पाठक की सेवा को महत्व देते थे. ऐसा नहीँ कि उन्हेँ साहित्य का या समाज शास्त्र का ज्ञान न हो. पर वे उस का बिल्ला लगाए घूमते फिरते नहीँ थे. (विश्वनाथ जी के विपरीत वह सामाजिक प्राणी थे. सभाओँ गोष्ठियोँ मेँ भाषण करते फिरते थे. बाँके बिहारी भटनागर और वह इस मामले मेँ कभी कभी हम लोगोँ के बीच हास्य का विषय भी बन जाते थे.) संपादक बनने से पहले रामायण पर उन्होँ ने एक लोकप्रिय फ़ीचर भी लिखा था. हर वह विषय जिस मेँ पाठक की रुचि हो, हर वह चीज़ जो पाठक को जाननी चाहिए, उस पर सामग्री प्रकाशित करना उन का मानो धर्म सा था. लेखक छोटा हो या बड़ा – इस की चिंता उन्हेँ नहीँ थी. हाँ, वह सामग्री विद्वत्ता के दंभ से हीन होनी चाहिए. यह बात ठेठ साहित्यकारोँ और महाज्ञानी पंडितोँ के गले नहीँ उतरती, लेकिन पाठक को यह दृष्टिकोण सुहाता है. जब भी किसी लोकप्रिय पत्रिका का संपादक इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देता है तो वह मुँह की खाता है. इस का एक महान अपवाद भी है – धर्मवीर भारती, और उन के संपादन मेँ धर्मयुग. लेकिन भारती जी और धर्मयुग का विषय एक स्वतंत्र खंड का हक़दार है.
माधुरी और मैँ
जब मैँ ने सुचित्रा-माधुरी का समारंभ किया तो मेरे सामने एक स्पष्ट नज़रिया था. मैँ एक ऐसे संस्थान के लिए पत्रिका का आरंभ करने वाला था, जो पहले से ही अंगरेजी की लोकप्रिय पत्रिका फ़िल्मफ़ेअर का प्रकाशन कर रही थी. आरंभ मेँ वहाँ का मैनेजमैँट फ़िल्मफ़ेअर का हिंदी अनुवाद ही प्रकाशित करना चाहता था. इस के लिए मैँ तैयार नहीँ था. मेरा कहना था, अनुवाद प्रकाशित करना हो तो आप को संपादक की तलाश नहीँ करनी चाहिए, बल्कि किसी ट्रांसलेशन ब्यूरो के पास जाना चाहिए या अपना ही एक ऐसा ब्यूरो खोल लेना चाहिए. फिर तो आप फ़िल्मफ़ेअर क्या, इलस्ट्रेटिड वीकली, फ़ेमिना, टाइम्स आफ़ इंडिया - सभी के हिंदी संस्करण निकाल सकते हैँ! और मैँ ऐसे किसी ब्यूरो का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीँ था. अनुवाद वाली योजना मैनेजमैँट की थी, रमा जी को स्वयं क़तई पसंद नहीँ थी.
जब उन लोगोँ ने मेरी बात स्वीकार कर ली, तो वेतन आदि पर किसी तरह की सौदेबाज़ी किए बिना, यहाँ तक कि वेतन तय किए बिना ही, मैँ मुंबई पहुँच गया. मेरे सामने कई चुनौतियाँ थीँ. मैनेजमैँट हमेँ फ़िल्मफ़ेअर की कसौटी पर कसेगा. हिंदी पाठक की माँगें कुछ और हैँ. उन दिनोँ हिंदी मेँ बहुत सारी फ़िल्मी पत्रिकाएँ निकलती थीँ. अधिकांश मेँ बड़े घटिया ढंग से लिखी फ़िल्म कहानियाँ प्रकाशित होती थीँ. माहौल यह था कि फ़िल्म पत्रिकाओँ का घरोँ मेँ प्रवेश बुरा समझा जाता था. फ़िल्म पत्रिका तो दूर, फ़िल्म देखना भी चारित्रिक पतन का लक्षण माना जाता था. और ऐसे मेँ मैँ अपनी पत्रिका को घर घर जाने वाली फ़िल्म पत्रिका बनाना चाहता था, जिसे बाप बेटी और माँ बेटा निस्संकोच साथ साथ पढ़ सकें. इस के साथ साथ मेरी अपनी सीमाएँ भी थीँ. मैँ सरिता, कैरेवान, मुक्ता, उर्दू सरिता जैसी पत्रिकाओँ मेँ काम कर चुका था. अपने को कुछ कुछ कवि भी समझता था. कलाचित्रोँ और मूर्तियोँ की, नाटकोँ की समीक्षाएँ किया करता था, फ़िल्मोँ की भी. लेकिन न फ़िल्मी कलाकारोँ के बारे मेँ बहुत जानता था, न तकनीक के बारे मेँ, न कला के. मुझे पत्रिका निकालते निकालते सब कुछ जानना और सीखना था.
सब से पहले मैँ ने फ़िल्मफ़ेअर के फ़ारमैट को अपना आधार बनाया, क्योँकि हमारी हिंदी पत्रिका का साइज़ भी वही था. फ़िल्मफ़ेअर जैसे ही कुछ स्थायी स्तंभ. यहाँ तक मैनेजमैँट को ख़ुश करने के लिए था. साजसज्जा के लिए मैँ ने कला विभाग से कहा कि उस से मिलती जुलती न हो कर कुछ अलग हो. हमेँ अपनी एक अलग छवि बनानी थी, पुरानी हिंदी फ़िल्म पत्रिकाओँ से और फ़िल्मफ़ेअर से. फ़िल्मोँ के बारे मे जो मैँ जानना चाहता था, वह जानने मेँ पाठकोँ की रुचि भी होगी – यह सोच कर मैँ ने काफ़ी सामग्री वैसी ही बनवाने की कोशिश की – जैसे एक सचित्र फ़ीचर – फ़िल्मेँ कैसे बनती हैँ. फ़िल्मफ़ेअर मेँ संगीत पर विशेष खंड नहीँ था. मैँ ने सोचा कि हमारी फ़िल्मोँ मेँ सब से लोकप्रिय तत्त्व है संगीत. तो उस के बारे मेँ पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए. फ़िल्मेँ बनाने मेँ अकेले अभिनेता और निर्देशक और निर्माता ही नहीँ होते, अनेक प्रकार के सहयोगी होते हैँ, नृत्य निर्देशक, सैट बनाने वाले, कैमरा चलाने वाले… उन सब के बारे मेँ भी पाठकोँ को बताया जाए.
और इस से भी महत्वपूर्ण यह बात कि उन दिनोँ जो हिंदी फ़िल्मोँ का पेड़ोँ के गिर्द नाचने वाला बचकाने से रोमांस का फ़ारमूला था, उस से दर्शक ऊब चुके थे. मैँ ने सोचा कि ऐसी फ़िल्मोँ की तीखी आलोचना की जाए और जो भी अच्छी फ़िल्मेँ निर्माणाधीन हों, जिन मेँ कुछ साहित्यिकता होने की संभावना हो, कुछ ऐसा हो जो लोकप्रिय भी हो सके और जिस का स्तर ऊँचा और सुरुचिपूर्ण हो, उसे प्रोत्साहन दिया जाए. साहित्यकारोँ को फ़िल्मोँ के बारे मेँ गंभीरता से सोचने का अवसर देने के लिए उन से लिखवाया जाए, निर्माता-निर्देशकोँ से साहित्य की, साहित्यकारोँ की चर्चा की जाए. और विश्व मेँ जो श्रेष्ठ सिनेमा बन रहा है, उस के बारे मेँ हिंदी वालोँ को बताया जाए. सब कुछ एक ऐसी शैली और भाषा मेँ जो पाठकोँ की समझ मेँ आ जाए. मेरे लिए यह इस लिए भी सहज था कि मैँ स्वयं अज्ञानी था. जो बात मेरी समझ मेँ नहीँ आती थी, मैँ मान लेता था कि पाठकोँ की समझ मेँ भी नहीँ आएगी.
इस प्रकार शुरू हुआ सुचित्रा-माधुरी का सफ़र. पहले अंक की प्रतियाँ ले कर हमारे रिपोर्टर जाने माने फ़िल्म वालोँ से मिले. सब ने प्रशंसा की. सब से अच्छी टिप्पणी शांताराम जी ने की थी. वह मुझे अब तक याद है. उन्होँ ने कहा, इस मेँ फ़िल्मफ़ेअर की झलक है, यह अच्छा नहीँ है. मैँ ने उन से तत्काल प्रार्थना की कि भविष्य मेँ भी हम पर नज़र रखें और मार्गदर्शन करते रहें. और उन से हमेँ हमेशा प्रोत्साहन मिलता भी रहा.
माधुरी सफल हिंदी पत्रिकाओँ मेँ गिनी जाती है. लेकिन जो बात मुझे माधुरी मेँ रहते समझ मेँ नहीँ आई, और अब तक नहीँ समझ पाया हूँ, वह यह कि पाठक फ़िल्मी गौसिप क्योँ पढ़ना चाहते हैँ. मैँ कभी गौसिप नहीँ छाप पाया. यही नहीँ, मुझे नहीँ लगता कि हिंदी मेँ कोई भी वैसी गौसिप लिख और छाप पाता है जैसी अँगरेजी फ़िल्म पत्रिका स्टारडस्ट ने शुरू की. हिंदी तो क्या, अँगरेजी की फ़िल्मफ़ेअर जैसी पत्रिकाएँ भी इस मामले मेँ पिछड़ रही थीँ. जिस तरह फ़िल्मफ़ेअर ने अपनी साजसज्जा से फ़िल्मइंडिया (बाद मेँ मदर इंडिया) को पिछाड़ दिया था, उसी तरह स्टारडस्ट ने अपनी चाशनीदार हिंदी-मिश्रित अँगरेजी से और एक अजीब से ईर्षा-मंडित कैटी (बिल्लीनुमा – उस के गौसिप वाले पन्नों मेँ एक बिल्ली बनी होती थी) रवैये से फ़िल्मफ़ेअर को पिछाड़ दिया. उस मेँ फ़िल्म समीक्षा तक नहीँ होती थी. गौसिप वाले फ़ीचरोँ के अतिरिक्त जो भी सामग्री होती थी, वह सिर्फ़ स्टार मैटीरियल होती थी. उस मेँ भी बस गौसिप और गौसिप. मेरी नज़र मेँ यह अच्छा हो या बुरा, लेकिन सच यह है कि यही उस की दिनो दिन बढ़ती बकरी का आधार बना. इस संदर्भ मेँ एक फ़ालतू सा सवाल है कि हमेँ पैसा कमाने के लिए किस हद तक जाना या नहीँ जाना चाहिए? आज तो हर हिंदी अँगरेजी दैनिक समाचार पत्र और सभी टीवी न्यूज़ चैनल पर फ़िल्मोँ और फ़िल्मी गौसिप छाई रहती है. (अच्छा है कि मैँ समांतर कोश बनाने कि लगन मेँ माधुरी छोड़ आया—वरना मेरे लिए माधुरी को गौसिप और अश्लील चित्रोँ वाली पत्रिका बनाना असंभव ही होता.)
धर्मयुग माने धर्मवीर भारती
धर्मयुग को एक समय हिंदी की पताका कहा जा सकता था. उसे यह पद दिलाने का काम किया था डाक्टर धर्मवीर भारती ने. मुंबई जाने से पहले मैँ उन्हेँ कालजयी नाटक अंधा युग के लेखक के तौर पर जानता था. उन से सारे हिंदी जगत को ईर्ष्या है, यह भी मैँ जानता था. इस ईर्ष्या का कारण मैँ न तब समझा, न अब तक समझ पाया हूँ. जहाँ तक पाठक-दर्शक वर्ग का संबंध है, या किसी के कृतित्व के आकलन का प्रश्न है, ये सारी बातेँ संदर्भातीत हो जाती हैँ. पाठक को इस से कोई मतलब नहीँ है कि कौन कैसा है. उस ने क्या लिखा है, उस मेँ कितनी गहराई है, मार्मिकता है – यही पाठक के काम की बात होती है. अगर भारती धर्मयुग मेँ नहीँ आते, तो उन्होँ ने अंधा युग से भी महान कोई अन्य रचना रची होती या नहीँ – यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा. मुझे लगता रहा है कि धर्मयुग का वरण कर के उन्होँ ने अपने को होम दिया. धर्मयुग उन के लिए पत्नी, प्रेमिका, बच्चे, परिवार – सब कुछ था. वही उन का ओढ़ना था, वही बिछौना. पुष्पा जी को धर्मयुग अपनी सौत लगता था. भारती जी का अपना साहित्यिक मत जो भी रहा हो, उन्होँ ने साहित्य के विवादोँ को धर्मयुग मेँ सर्वोच्च स्थान कभी नहीँ लेने दिया. एक एक पन्ने को उपयोगी सामग्री से ढूँसना उन्हीँ का काम था. अपने आप को आधुनिक मानने वाले पत्रकार सजावट के पीछे अपने कम पन्नों का क़ीमती स्थान बरबाद कर देते हैँ. भारती जी तो बहुत सारे फ़ोटो भी डाकटिकट जितने आकार के छापते थे, ताकि पाठक को पढ़ने की सामग्री पूरी मिले. उन्होँ ने हिंदी के पाठक की ज्ञान की पिपासा को पूरी तरह समझ लिया था. वह पाठक को छका कर ज्ञानरस पिलाना चाहते थे. धर्मयुग की बिकरी सें सब से तेज़ी से बढ़त तब हुई जब अमरीका चाँद पर आदमी उतारने वाला था, और धर्मयुग ने अपने पन्नों पर उस की हर तरह की जानकारी बिखरा दी. यह एक मोटा सा उदाहरण है. सौर ऊर्जा हो, तो भी धर्मयुग के पन्नों पर उस के लिए जगह थी. रसोई के काम की नई चीज़ हो तो भी, और पाकिस्तान मेँ जीए सिंध आंदोलन हो तो उस के बारे मेँ भी. बांग्ला देश के युद्ध मेँ तो भारती जी ने स्वयं जा कर रिपोर्टिंग की, और पाठकोँ को अपनी लेखनी से सराबोर कर दिया. बिकरी बढ़ी यह उस का परिणाम था, उद्देश्य नहीँ. ठीक वैसे ही जैसे हिंदू समाज के कूड़ा करकट को निकाल फेंकना विश्वनाथ जी के लिए बिकरी का नहीँ, निजी अभिव्यक्ति का साधन था.
भारती जी का मन जब धर्मयुग से ऊबने लगा (अनेक कारणोँ से, जिन मेँ टाइम्स समूह के बदलते मैनेजमैँट का भी हाथ था), तो धर्मयुग मेँ वह बात नहीँ रह गई. तब तक मैँ दिल्ली आ चुका था, इस लिए बहुत कुछ नहीँ कह सकता. भारती जी के बाद तो धर्मयुग गिरता ही चला गया. मैँ यही कहूँगा कि मैनेजमैँट की ज़िम्मेदारी तो है ही, उन लोगोँ की भी है, जो उस के संपादकीय कर्ताधर्ता बने. उन्होँ ने पाठक को समझने की कोशिश कम की, और अपनी निजी पसंद या नापसंद को, मैँ तो कहूँगा अपने नासमझ को, अधिक प्रश्रय दिया. एक दो बार मैँ ने बाद का धर्मयुग देखा. मैँ अपने से पूछता कि क्या यह ख़रीदने के लिए मैँ अपना पैसा ख़र्च करूँगा? उत्तर नकारात्मक होता. मैँ उस पर अपना समय भी लगाना उचित नहीँ समझता.
पराग और सारिका
मैनेजमैँट किस प्रकार किसी पत्रिका का भला चाहते हुए भी समाप्त कर सकता है, इस का सर्वोत्तम उदाहरण है पराग . (बाद मेँ यही थोड़े बहुत अंतर के साथ अन्य पत्रिकाओँ के साथ भी घटा.) उस के संपादक थे सरिता के दिनोँ से ही मेरे मित्र और सिद्धहस्त कथाकार और कल्पनाशील आनंद प्रकाश जैन. तमाम उन बंधनोँ और सीमाओँ के जो कि प्रकाशकोँ ने पराग पर लगा रखी थीँ, पराग अच्छा ख़ासा चल रहा था. एक बंधन और सीमा यह थी कि उस मेँ परियोँ की कहानियाँ नहीँ छापी जाएँगी. प्रकाशकोँ का विचार था कि बच्चोँ के लिए यह कोई अच्छी चीज़ नहीँ होती. मैँ समझता हूँ कि परीकथाएँ बच्चोँ की कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता को प्रोत्साहित करने का उत्तम साधन होती हैँ. देवी देवताओँ की कहानियाँ भी इसी लिए बंद थीँ. इस का भरपूर लाभ मिल रहा था हिंदुस्तान टाइम्स के नंदन को, और दक्षिण से प्रकाशित होने वाले चंदा मामा को . फिर भी, पराग अच्छा ख़ासा चल रहा था.
उन दिनोँ अँगरेजी मेँ स्टेट्समैन वाले कलकत्ता से जूनियर स्टेट्समैन निकालने लगे थे. अँगरेजी पढ़े लिखे शहरी तबक़ों मेँ उस का काफ़ी रुआब बन गया था. मैनेजमैँट ने कहा कि पराग को किशोरोँ की पत्रिका बना दिया जाए और जूनियर स्टेट्समैन से प्रेरणा ली जाए. यह तथ्य नज़रअंदाज कर दिया गया कि चंद बड़े शहरोँ के बाहर जूनियर स्टेट्समैन का अस्तित्व ही नहीँ था. सवाल यह था और अब भी है कि हिंदी का जो पाठक बड़े शहरोँ मेँ रहता था वह भी उस कृत्रिम और नक़लची संस्कृति को नहीँ जानता समझता था जो बचपन से ही अँगरेजी वातावरण मेँ पनपने वाले वर्ग को मिलती है. बड़े शहरोँ से निकलते ही, वह संस्कृति विलीन हो जाती है. हिंदी बाल पत्रिका वहीं बेची जाने वाली है. इस के साथ ही साथ यह समस्या भी है कि जब पत्रकार उस संस्कृति को जानते ही नहीँ, तो उस मेँ पले बढ़े पाठक के लिए वे काम की सामग्री कैसे दे सकते हैँ? देँगे तो पाठक कहाँ से आएँगे? दिक़्क़त यह थी कि धनी प्रकाशकोँ के अपने बच्चे उसी संस्कृति मेँ पले बढ़े थे, और वे अपने संपादक से वही चाहते थे. वह नहीँ दे पाता था तो उसे मूर्ख, अज्ञानी और अयोग्य समझते थे. सत्तर आदि दशक मेँ मूर्ख, अज्ञानी और अयोग्य कौन था – यह कहना कठिन है.
नया रूप नहीँ चला तो पराग को एक बार फिर बच्चोँ की पत्रिका बनाने के आदेश दिए गए. लेकिन न आनंद प्रकाश जी, न उन के बाद कोई और संपादक पराग को पहले जैसा वैभव दे पाया. एक बार वह पाठक के मन से उतरा तो उतरा ही रहा. न ख़ुदा ही मिला न विसाले सनम! हाँ, बाद मेँ हरिकृष्ण देवसरे कुछ जान पराग मेँ डाल पाए. बहुत दिन वह भी पराग को जीवित नहीँ रख सके.
मोहन राकेश के बाद सारिका पर आनंद प्रकाश जैन और चंद्रगुप्त विद्यालंकार हाथ आज़मा चुके थे. कहानियोँ जो विविधता चाहिए, उस की ओर इन दोनोँ ने ध्यान नहीँ दिया. तब कमलेश्वर आए. वह उसे कहानी की बहुचर्चित पत्रिका बना पाए. उस का कारण विविधता नहीँ थी. कमलेश्वर का अपना सजीव चेतन व्यक्तित्व था. सभी साहित्यकारोँ के लिए सारिका लेना एक तरह से आवश्यक बन गया. साहित्यकार भी संख्या मेँ कम नहीँ हैँ.
अतः पत्रिका एक बार फिर विकासोन्मुख हुई. कमलेश्वर ने यह भी ध्यान रखा कि कहानियाँ रोचक हों. फिर उन्होँ ने समांतर कहानी आंदोलन छेड़ दिया. पहले आनंद प्रकाश जैन सचेतन कहानी आंदोलन छेड़ चुके थे. पत्रिका मेँ प्रकाशित होने वाले लेखकोँ की संख्या आंदोलन से जुड़े लोगोँ तक रह गई. फिर भी पत्रिका चलती रह सकती थी, क्योँकि उस आंदोलन के लेखकोँ की रचनाओँ मेँ पठनीयता थी, और जब तक सामग्री पठनीय है, पाठक को इस से कोई फ़र्क़ नहीँ पड़ता कि लेखक यह है या वह. लेकिन तभी कुछ व्यक्तिगत कारणोँ से संचालक परिवार के दो एक सदस्यों को कमलेश्वर अप्रिय हो गए. सन 77-78 के कुछ राजनीतिक कारण भी रहे कहे जाते रहे हैँ. मेरी राय मेँ कमलेश्वर के जाने मेँ राजनीति नहीँ ही थी. जो भी हो, कमलेश्वर ने सारिका छोड़ दी. बाद मेँ वह पनप नहीँ पाई. किसी को भी समझ मेँ नहीँ आया कि जो कमलेश्वर का अपना पाठक वर्ग था, उस के रूठ जाने के बाद सामान्य पाठक को कैसे आकर्षित किया जाए.
बात कहानी की चल रही है. मैँ स्वयं कहानीकार नहीँ कहानी पाठक हूँ. तो मैँ यह भी कहना चाहूँगा कि हिंदी कहानी अपने को पाठक से काटने पर तुली है. कहानीकार अपने को प्रथम श्रेणी का साहित्यकार मानते हैँ, और वे लोग पाठक के लिए नहीँ, समालोचकोँ को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैँ. उन की रचनाएँ पत्रकारिता के नहीँ, साहित्यकारिता के दायरे मेँ आती हैँ. हिंदी मेँ साहित्यकारिता मेँ आज सफलतम हैँ – राजेंद्र यादव और उन का मासिक हंस. हंस मेँ कहानियाँ प्रकाशित करने के साथ समाज पर भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित करते हैँ, और अपने लिए अच्छा ख़ासा सामान्य पाठक वर्ग तैयार कर पाए हैँ. यदि राजेंद्र जी को बुरा न लगे, तो मैँ कहूँगा कि उन्होँ ने विश्वनाथ जी के सुधारवादी आंदोलन पर दलित और नारी विमर्ष का मुलम्मा भर चढ़ाया है. लेख सरिता जैसे सामाजिक और पारिवरारिक विषयोँ पर नहीँ होते. उन्हेँ सैद्धांतिकता से मँढा जाता है. पर अंततोगत्वा वे हिंदू धर्म और समाज मेँ परिवर्तन का अलख तो जगाते ही हैँ. विश्वनाथ जी की जब अपनी ऊर्जा चुक सी गई और संपादकीय बाग़डोर उन के पुत्र परेशनाथ के हाथों आई तो नए युग के लिए नई पहचान वाली जो इंग्लिश पत्रिका Woman’s Era शुरू की थी, और विश्वनाथ जी की ही देखरेख मेँ जिस का हिंदी संस्करण गृहशोभा निकाला गया था, उसे परेशनाथ लगातार परिवर्तनशील सामयिक रूप देते रहे हैँ. यहाँ तक कि किसी भी अन्य महिला पत्रिका का इन के मुक़ाबले टिक पाना असंभव हो गया है.
सर्वोत्तम
अस्सी आदि दशक के आरंभ मेँ टेलिविज़न के विस्फोट ने हिंदी पत्रोँ से सामान्य पाठक को और भी दूर कर दिया था. एक तो पहले ही हिंदी पाठक अपनी अकर्मण्यता और रुचिहीनता के लिए सुविख्यात या कुख्यात है, वह कम से कम पढ़ना चाहता है, ख़रीद कर तो और भी कम पढ़ना चाहता है, ऊपर से उस के जीवन मेँ जो थोड़ा बहुत ख़ाली समय था, उसे टीवी ने भर दिया. वहाँ उसे काव्य, गीत, संगीत, कहानी, हास्य – सब मिलता था, सहज पाच्य शैली मेँ. टीवी ने विज्ञापकोँ भी अपनी ओर खींचा. उन के बजट का बड़ा हिस्सा टीवी पर चला गया. प्रिंट मीडिया मेँ केवल कुछ बड़े अख़बारोँ तक, वह भी अधिकतम बिकरी वाले अख़बारोँ तक ही ख़र्च करने के लिए विज्ञापकोँ पर पैसा बचा था. इस चैलेंज से अमरीकी प्रिंट मीडिया भी नहीँ बच पाया था. लाइफ़ जैसी पत्रिकाएँ धराशायी हो गईं. सामान्य मध्यम वर्गीय पाठक की पत्रिकाओँ मेँ केवल रीडर्स डाइजेस्ट ही बच पाया था. इस का कारण यह था कि विज्ञापकोँ ने इस वर्ग के पत्रोँ मेँ से रीडर्स डाइजेस्ट को समर्थन देने के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया था. लेकिन अपने आप को बदलते समाज के अनुरूप न ढाल पाने के कारण अमरीका मेँ पिछले कुछ सालोँ से उस की लोकप्रियता दिनोदिन घटती जा रही है. सुधार के अनथक प्रयासोँ के बावजूद कोई बहुत आशाप्रद तस्वीर बन नहीँ बन पा रही है. भारत मेँ वैसी हालत नहीँ है. उस का भारतीय अँगरेजी संस्करण अब भी बिक पा रहा है. एक कारण है— उस के भारतीय पाठक उस वर्ग के हैँ जिसे हम नक़लची कह सकते हैँ. सर्वोत्तम के पाठक उस कोटि मेँ नहीँ आते थे. यहाँ भी कुछ उदाहरण दे कर ही बात स्पष्ट की जा सकती है. कनाडा मेँ आधी से अधिक सामग्री कनाडा की छपती है, भारत मेँ भारत की नहीँ. भारत मेँ कुछ भी घटता रहे, यहाँ के डाइजेस्ट मेँ उस के बारे मेँ कुछ नहीँ छपता था. लगता था उस का संपादन मंडल किसी अमरीकी ओलिंपस पर्वत पर बैठा है, नैसर्गिक बादलोँ के नीचे जो भारतीय संसार है, वह उसे नहीँ दिखाई देता. दूसरा कारण है उस का स्वामित्व टाटा से हट कर इंडिया टुडे के हाथों आ जाना.
लेकिन कहना होगा कि डाइजेस्ट के लेख बहुत अच्छी तरह लिखे होते हैँ. उन की शैली से हिंदी वाले बहुत कुछ सीख सकते हैँ. लेकिन पत्रकारिता मात्र शैली नहीँ होती. लेखक संसार को कैसे देख रहा है – इस से भी उस का सरोकार होता है. केवल एक उदाहरण – मान लीजिए श्रीलंका के बारे मेँ कोई लेख है. कोई अमरीकी वह लेख लिखता है, तो वह पश्चिम की नज़र से उस के इतिहास को देखेगा, यह बताएगा कि अंगरेजी का सैरेनडिपिटी शब्द उस द्वीप के अरबी नाम सेरेनदीव से बना है, कि वहाँ आर्थर क्लार्क रहते हैँ…. यदि कोई भारतीय लिखेगा तो वह श्रीलंका से भारत के पुराने संबंधों की बात करेगा, रामायण की बात करेगा, सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा के बारे मेँ बताएगा, आज वहाँ की राजनीति मेँ तमिल और सिंहल टकरावोँ के पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेगा. भारतीय पाठक को अँगरेजी के डाइजेस्ट मेँ यह सब नहीँ मिलता, और उसे इस की परवा भी नहीँ है, क्योँकि वह अपने आप को आम भारतीय से कुछ भिन्न, कुछ अलग, कुछ ऊपर समझता है. अब हालत थोड़ी बहुत बदल रही है. संस्थापक वालेस दंपति के लेआउट फ़ारमूले को बदल दिया गया है. स्थानीय सामग्री की मात्रा बढ़ी है.
लेकिन हिंदी पाठक वैसा नहीँ है. जब मैँ वहाँ था, तो सर्वोत्तम मेँ हम ने हिंदी पर और भारतीय विषयोँ पर कुछ विशेष लेख लिखवाए थे. मैँ ने पंडित गोपाल प्रसाद की एक पुस्तक मेँ से मथुरा पर एक अद्वितीय लेख छापा था, जिस मेँ वहाँ के त्योहारोँ का, छप्पन भोगोँ का वर्णन था; रामायण पर परिभाषात्मक पुस्तक लिखने वाले डाक्टर कामिल बुल्के पर विशेष लेख छापा था…
इलस्ट्रेटिड वीकली भी
साप्ताहिकोँ की बात करें तो हमेँ देखना होगा कि केवल धर्मयुग और दिनमान ही बंद नहीँ हुए, इलस्ट्रेटिड वीकली भी बंद हुआ. क्योँ? ख़ुशवंत सिंह जी के जाने के बाद वीकली फिर रट मेँ पड़ गया. पाठक को हर अंक मेँ जो नवीनता और चुनौती ख़ुशवंत फेंकते थे, वह समाप्त हो गई. उस के जो संपादक आए उन मेँ वह सजग सृजनशीलता और कल्पनाशीनता नहीँ थी, जो चाहिए थी. धर्मयुग मेँ भारती जी ने कभी कमाल दिखाया था. लेकिन टीवी विस्फोट के बाद जो चुनौती आई थी, जिस तरह तेजी से पाठक की माँगें बदली थीँ, वह उस से सामंजस्य स्थापित नहीँ कर पाए तो इस मेँ मैनेजमैँट का भी हाथ था.
इसी प्रकार दिनमान का प्रश्न है. दिनमान को इंडिया टुडे से बड़ी पत्रिका बनाया जा सकता था. लेकिन न तो उस के लिए खुले दिल से संसाधन जुटाए गए, न उस के संपादन विभाग को वैसी जिम्मदारी सँभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया, न तैयार. ऊपर से बंद करने की धमकी हमेशा सिर पर सवार रखी जाती थी.
इस संदर्भ मेँ श्री अशोक जैन के पुत्र समीर जैन का नाम बार बार उछाला जाता है. मैँ समीर से एक दो बार तब मिला था, जब वह बहुत कमउम्र थे. उन का दृष्टिकोण बन ही रहा था. वह स्वामीनाथन के चित्रोँ के दीवाने थे. उन मेँ एक नई दृष्टि थी, और वह उतावले थे. वह भारतीय पत्रकारिता को एक दम से आधुनिकतम रोचक अमरीकी स्तर तक ले जाना चाहते थे. ऐसा चाहना पूरी तरह ग़लत नहीँ कहा जा सकता. (इक्कीसवीँ सदी मेँ उन के विचारोँ ने भारतीय पत्रकारिता के लिए नए पैमाने स्थापित किए हैँ) लेकिन तब उन की उतावली उन्हेँ अच्छा मालिक-संचालक बनने से रोक रही थी. अपने संपादकोँ को अपनी बात न समझा पाना उन की अपनी कमज़ोरी कहा जाएगा. अपने उतावलेपन से संपादकोँ के मन मेँ अपने प्रति अरुचि जगा देना भी उन की अपनी भूल कहा जाएगा. एक दो संपादकोँ से मैँ ने सुना है कि वह सब के सामने किसी भी संपादक का अपमान करने से नहीँ चूकते थे. संपादकोँ को श्रीमती रमा जैन के शिष्ट व्यवहार की आदत थी. दूर से जो कुछ मैँ ने सुना है, समझा है, उस के आधार पर मैँ यह कह सकता हूँ कि समीर के मन मेँ अपने पत्रोँ को नए युग के अनुरूप ढालने की सही आकांक्षा रही होगी. लेकिन उन के अपने व्यवहार ने उन के उद्देश्यों को, जहाँ तक हिंदी पत्रोँ का सवाल है, असफल कर दिया.
मैनेजमैँट ने बिना सोचे समझे ऊटपटांग और पूरी तरह अव्यावसायिक आदेश देने शुरू कर दिए. धर्मयुग मेँ इलस्ट्रेटिड वीकली से अनूदित रचनाएँ छापने के आदेश दिए जाने की बात मैँ ने सुनी है. पता नहीँ कहाँ तक सही है. माधुरी को हिंदी फ़िल्मफ़ेअर बना दिया गया – यह तो सब जानते हैँ. कुछ दिन मैँ ने वामा को नज़दीक से समझने की कोशिश की थी. मैँ जानता हूँ उसे हिंदी फ़ेमिना बनाया जाने वाला था. जैसे हिंदी फ़िल्मफ़ेअर नहीँ चल पाया वैसे ही हिंदी फ़ेमिना भी नहीँ चल पाती. मैँ ने सुना है पहले इसी तरह की योजना नवभारत टाइम्स को हिंदी टाइम्स आफ़ इंडिया बनाने की थी! हिंदी ब्लिट्ज़ के साथ आधी समस्या यह भी थी. कुछ ऐसी ही समस्या हिंदी इंडिया टुडे के साथ भी है. इन सब अँगरेजी पत्रोँ के लेखक संपादक भारतीय हैँ – यहाँ तक तो ग़नीमत है, लेकिन अँगरेजी हिंदी पाठकोँ की रुचियोँ मेँ स्तर मेँ जो अंतर है, पत्रकारिता मेँ उसे भी नज़रअंदाज नहीँ किया जा सकता. अगर पत्रिका माल है, तो हमारा माल अपने ग्राहक की आवश्यकताओँ को पूरा करने वाला तो होना चाहिए. मुझे गुलाब जामन पसंद हैँ, तो आप मुझे केक तो नहीँ बेच सकते.
यह कहना ग़लत है कि हिंदी पाठक के पास पैसा नहीँ है. छोटे से छोटे कस्बे मेँ धनी व्यापारी भरे पड़े हैँ. कितने सरकारी अफ़सर हैँ, पुलिसिए हैँ, आयकर वाले हैँ, पटवारी हैँ, ज़मींदार हैँ, जिन्हों ने बेतहाशा सफ़ेद और धन कमाया गया है. वे सब पैसा ख़र्च करने को उतावले हैँ. ये सब लोग मूलतः हिंदी के पाठक हैँ. यही लोग संगीत की दुनिया को मालामाल कर रहे हैँ. दिक़्क़त सिर्फ़ यह है कि उन्हेँ हिंदी मेँ वह माल नहीँ मिल रहा जिस पर वे पैसा ख़र्च करना चाहें.
सांध्य टाइम्स
टाइम्स के ही हिंदी सायंकालीन दैनिक सांध्य टाइम्स का उल्लेख करना आवश्यक है. जब जब मेरे मित्र सत सोनी के हाथ मेँ यह पत्र आया और जब तक रहा, ख़ूब चमका. वर्तमान हिंदी पत्रकारोँ मेँ सत सोनी सब से अधिक आधुनिक और पाठक के नए तेवर को समझने वाले पत्रकार हैँ – यह मैँ उन से पिछले पचास सालोँ के संपर्क के आधार पर कह सकता हूँ. सोनी के जाने के बाद देखने मेँ आया कि सांध्य टाइम्स मेँ कुछ पन्ने अँगरेजी मेँ छापे गए. क्योँ? मैँ नहीँ जानता. हिंदी पाठक अँगरेजी सामग्री के लिए पैसा क्योँ ख़र्चे?
बात इतनी ही नहीँ है. जब कोरी व्यावसायिकता पत्रकारिता पर हावी हो जाती है, तो मैनेजमेँट बहुत सारी बातेँ सोचने लगते हैँ. जहाँ कार्यालय है, उस जगह का बाज़ार भाव क्या है? उस भाव के हिसाब से जो मुनाफ़ा समाचार पत्र दे रहे हैँ, क्या वह उस से मिल सकने वाले मासिक सूद से कम है? यदि वहाँ, मान लीजिए, होटल खोल दिया जाए, तो कितना मुनाफ़ा कमाया जा सकता है? जब इस तरह हानि लाभ की गिनती की जाने लगेगी, तो शहर के बीच मेँ बने हर अख़बार के दफ़्तर को या तो बंद करना पड़ेगा, या फिर दूर किसी गाँव मेँ ले जाना पड़ेगा! मैँ ने यह उदाहरण जान बूझ कर दिया है. ऐसा एक बार सोचा गया था – मुंबई मेँ टाइम्स के बोरीबंदर स्थित कार्यालय के बारे मेँ. कार्यालय तो बंद नहीँ किया गया, लेकिन पत्रोँ को दूकान बना दिया गया. फ़ेमिना को फ़ैशन शो का व्यापारी बना दिया गया, और फ़िल्मफ़ेअर को पुरस्कार समारोह से मिलने वाली आमदनी की दूकान. इन के प्रायोजित कार्यक्रमोँ से करोड़ोँ कमाए जाने लगे. अब ये पत्रिकाएँ हैँ या कुछ और? मुक़ाबले मेँ हम देखते हैँ कि फ़ेमिना जैसी और दिल्ली प्रैस से विश्वनाथ जी की देखरेख मेँ प्रकाशित होने वाली अँगरजी पत्रिका वूमैन्स ऐरा और हिंदी की गृहशोभा बड़ी शान से पत्रकारिता का झंडा लहरा रही हैँ.
अँगरेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटिड वीकली के बारे मेँ बात करने के लिए भी यह सही प्रसंग है. जो पत्रिका मर रही थी, उसे ख़ुशवंत सिंह जी ने जीवंत बना दिया और दौड़ा दिया. उन के बाद वह जीवंतता फिर विलीन हो गई. यदि इलस्ट्रेटिड वीकली को भी व्यवसाय बनाने का कोई माक़ूल तरीक़ा मैनेजमैँट को मिल जाता तो वह बंद नहीँ होता. यही धर्मयुग के साथ हुआ, सारिका के साथ भी.
जहाँ तक फ़ेमिना का प्रश्न है, या फ़िल्मफ़ेअर का, या अँगरेजी मेँ मुंबई से निकलने वाले इन जैसे अन्य पत्रिकाओँ का, उन की चमक दमक ही अब सब कुछ है. यह महँगी चमक दमक अपने आप को मौड कहने वाले पाठक को और विज्ञापक को प्रभावित करती है. जितना पैसा इन के एक अंक के मुद्रण पर ख़र्च किया जाता है, उतना किसी हिंदी पत्रिका पर पूरे साल मेँ भी नहीँ होता था. यह सही है कि हर व्यवसायी पहले व्यवसायी होता है. तत्काल लाभ कमाना उस के लिए प्राथमिकता है. अन्यथा वह ज़्यादा दिन टिक नहीँ सकता. लेकिन भविष्य के बाज़ारोँ को पहले से तैयार करना और साधना भी व्यावसायिकता है, और दूरदर्शी व्यावसायिकता है.
पिछली सदी के अंत के सालोँ मेँ पत्रकारिता के क्षेत्र मेँ निराशाजनक दृश्य दिखाई दे रहा था. अधिकांश पत्रकार अपने आप को नई चुनौतियोँ के लिए तैयार नहीँ कर रहे थे. जो बडे व्यवसायी हैँ, वे भविष्य के लिए तैयार नहीँ थे.
लेकिन नई सदी के पहले दशक मेँ सारी तस्वीर बदल चुकी है. लगता है एक दम नवजीवन का, नई ऊर्जा का विस्फोट हो चुका है. ❉❉
© अरविंद कुमार
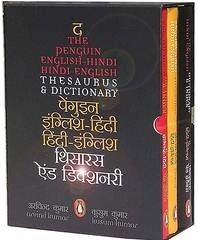
Comments