Original article: http://lekhakmanch.com/?p=2417
ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत ही कम होते हैं जिन्हें अपने सपने साकार करने में पूरे परिवार का निरंतर सहयोग मिले। विशेषकर ऐसे जोख़िमभरे सपने जिस में स्वप्नद्रष्टा को अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़नी हो, अनुदान तो दूर की बात है, कहीं से कैसी भी आर्थिक सहायता न मिलने वाली हो, जिनका पूरा होना भी अनिश्चित हो। इतना ही नहीं, जिसके रास्ते में एक के बाद एक भारी से भारी अड़चन आती रहे, फिर भी किसी का मनोबल न टूटे, ऐसी मिसालें दुनिया में कुछ कम ही हैं। अरविंद कुमार ऐसे ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। प्रस्तुत हैं उनसे अनुराग की बातचीत के कुछ अंश-
आपको शलाका सम्मान प्रदान किया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
कभी सपने में भी कल्पना नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। ग़ालिब के शब्दों में इतना ही कह सकता हूं– बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हिंदी अकादेमी के उपाध्यक्ष श्री अशोक चक्रधर और उनके चयन मंडल ने मुझे इस योग्य समझा—चमत्कृत हूं और बहुत प्रसन्न।
आपको यह नहीं लगता कि भाषा के क्षेत्र में जितना काम किया है, उस हिसाब से आपको समुचित मान-सम्मान नहीं मिला ?
काम करने वाले का काम है काम करना, मान-सम्मान करने वाले का काम है मान-सम्मान करना। उनके बारे में मियाँ ग़ालिब के ही अल्फ़ाज़ हैं– चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वे अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। इसका संदर्भ तो बिल्कुल दूसरा है, पर सम्मान देने वालों पर भी चस्पाँ होता है।
जब पंद्रह साल की उमर में बालश्रमिक के रूप में छापेख़ाने में दाख़िल हुआ, तभी से मेरे लिए काम, अपने आप में सम्पूर्ण आत्मसम्मान रहा है। कभी किसी से कोई गिला नहीं किया। सन् 45 में ही मैं करोलबाग़, दिल्ली के कांग्रेस सेवादल और आज़ादी के दीवाने एक उग्र दल ‘लालक़िला ग्रुप’ का सदस्य बन गया था। सन् 47 में देश आज़ाद हुआ तो मुझ जैसे कुछ दोस्तों ने देशभक्ति की एक परिभाषा गढ़ी। वह यह कि हर काम मेहनत से करना, ईमानदारी से करना ही 47 के बाद देशभक्ति का पैमाना है। मैं अभी तक उस पर क़ायम हूँ—हर नारेबाज़ी से दूर, जितना कर सकता हूँ, करता हूँ। दूसरों की बात दूसरे जानें।
‘समांतर कोश’, ‘द पेंगुइन इंग्लिश हिंदी/हिंदी इंग्लिश थिसारस एंड डिक्शनरी’ और अब ‘अरविंद लैक्सिकन’। क्या इन सबके लिए आपको किसी संस्थान या सरकार से आर्थिक सहायता या अन्य तरह की मदद मिली ? आपने इसके लिए कभी कोशिश की ? इसे लेकर आपको किस तरह के अनुभव हुए।
शुरू में, यानी 1973-74 में कई जगह कोशिश की। किसी-न-किसी बहाने टाल दिया गया। हिंदी के किसी काम के लिए कुछ माँगना सब से बड़ी ज़लालत है। अगर कोई कुछ देता भी है तो पहले सारे काम का श्रेय लेना चाहता है, फिर किसी-न-किसी बहाने टालता रहता है। सहायता के पीछे भागते-भागते न जाने कितना समय निकल जाता। मैंने सोचा, चलो समुद्र में कूद पड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक सहारा बिल्कुल अपना था। दिल्ली के मॉडल टाउन में अपना मकान था। रहन-सहन सादा था। मुंबई में ‘माधुरी’ के संपादन काल की थोड़ी-बहुत बचत थी। सोचा था कि दो साल में थिसारस बनाने का काम पूरा हो जाएगा।
पर ऐसा हुआ नहीं। कहावत है सिर मुँडाते ही ओले पड़े। मुझ पर ओले नहीं पड़े, बारिश पड़ी। 1978 की 21 मई को दिल्ली पहुँचे थे। कुछ ही महीने बीते थे। 4 सितंबर को यमुना की मैनमेड भारी बाढ़ ने हमारे घर को सात फ़ुट तक ग़र्क़ कर दिया। मुंबई का जो भी थोड़ा-बहुत अच्छा सामान था, यमुना में बह गया। घर माँ-बाप और भाई और उसकी पत्नी के लिए छोटा था। बस, यही हमारा तारनहारा बना। ‘समांतर कोश’ का काम हम कार्डोँ पर कर रहे थे। मकान में ऊपर ज़ीने के रास्ते में छः फ़ुट ऊँची, गरमी में आँवे जैसी तपती मियानी थी। वहीं कार्ड जमाए थे। यमुना मैया वहाँ तक नहीं गईं। हमारा भविष्य बच गया। वहीं पूरा टब्बर पाँच दिन टंगा रहा। चारों ओर पानी था। हम बिना किसी ख़र्चे के वैनिस में रहने का मज़ा उठाते रहे। चारों तरफ़ कामचलाऊ किश्तियाँ चलती देखते रहे।
मेरा विश्वास है कि ‘समांतर कोश’ ने अपने होने का संकल्प कर लिया था। वह अपने को तो बचाता रहा, और इसके लिए हर क़दम पर मेरी रक्षा करता रहा।
हिंदी की व्यापारिकता और हिंदी के नाम पर सरकारी तंत्रोँ की कृपणता कई बार दयनीय लगती है। स्वयं हिंदी वाले इसमें आगे बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हिंदीवालों के शोषण में सहभागी बनते हैं। एक कारण यह है कि हम हिंदी वाले अपना अवमूल्यन आप करते हैँ। हिंदी को इंग्लिश से हीनतर समझने की आदत हमें पड़ गई है। अपने 65 साल के प्रिंटमीडिया और अब कंप्यूटर पर काम के बल पर मैँ कह सकता हूँ कि हम अंगरेजी वालोँ से कहीँ आगे और बढ़ कर हैं।
जब ‘समांतर कोश’ प्रकाशित हुआ तो DOE नाम की एक सरकारी संस्था की ओर से मुझे फ़ोन मिला। फ़ोन पर ही उसे इंटरनेट पर डालने की अनुमति तत्काल चाहते थे। मैंने पछा, ‘बीस-पच्चीस साल के तनदेही के बदले मुझे क्या मिलेगा।’ जवाब मिला, ‘कुछ नहीं। आप यह कोश जनहित में सरकार को दे दीजिए!’ मैँ हक्का बक्का रह गया। फिर एक पल बाद मैंने हिंदी के उन लाभभोक्ता से पूछा कि ‘क्या आप महान जनहित वाली नौकरी अवैतनिक कर रहे हैं। चलिए नहीं, तो भी क्या आप भविष्य में पगार लेना बंद कर देंगे। यदि हाँ तो मैं जनहित के लिए यह कोश सरकार को देने के लिए तत्पर हूँ।’ उधर से फ़ोन काट दिया गया।
इसी प्रकार अब मेरे ई-कोश के लिए मेरी बेटी ने उस विभाग से संपर्क किया। अब भी वही उत्तर था ‘अरविंद लैक्सिकन आप हमें जनहित में दे दीजिए…’

अरविंद कुमार का परिवार– ऊपर बाएं पुत्र सुमीत कुमार, बेटी मीता लाल, दामाद अतुल बिहारी लाल। नीचे बीच में अरविंद कुमार और कुसुम कुमार, बाएँ धेवती तन्वी, दाहिने धेवता अक्षय
जो काम कोई संस्था नहीँ कर सकी, आप ने कर दिखाया। कैसे इतना बड़ा काम कर सके ?
किसी संस्था ने यह काम नहीं किया तो कारण यह था कि किसी संस्था ने ऐसा करने का विचार नहीं किया। भारत सरकार ने कोश निर्माण के लिए कई संस्थाएँ बनाई थीं। जहाँ तक मुझे पता है, किसी के पास ऐसा कार्यक्रम नहीं था। अगर कोई संस्था इसमें लगती तो जो होता वह मैंने जापान में देखा है। 1997 में मुझे वहाँ की भाषा संस्था के निमंत्रण पर विश्व में थिसारसों की विशाल गोष्ठी में जाना पड़ा। उस संस्था ने 200 लोगों के स्टाफ़ के साथ लगभग बीस साल में जो थिसारस बनाया था, वह समांतर कोश के सामने पिद्दी-सा था। मेरे पास उनका थिसारस है। शायद अब दस-बारह साल में वह कुछ बड़ा हो गया हो।
आपकी दिनचर्या क्या है?
आज जब डाटा का काम एक तरह से पूरा हो चुका है, उसमेँ एक-एक अभिव्यक्ति संस्करणानुसार क्रमांकित हो चुकी, तो भी काम को पूरी तरह पूरा नहीं माना जा सकता। मूल डाटा में शब्दकोशोँ जैसी परिभाषाएँ नहीँ थीँ। आख़िर हम तो थिसारस बना रहे थे, न कि शब्दार्थ कोश। पर अब मुझे लगा कि सभी मुखशब्दों या शीर्षशब्दोँ की हिंदी और इंग्लिश परिभाषाएँ जोड़ दी जाएँ तो ‘अरविंद लैक्सिकन’ और भी उपयोगी हो जाएगा। यह काम अब धीरे-धीरे चल रहा है। लगभग 15 प्रतिशत काम हो गया है। शेष भी कालांतर में हो जाएगा। ऑनलाइन संस्करण का सबसे बड़ा लाभ ही यह है कि इसकी सामग्री जब चाहे परिष्कृत होकर सभी उपभोक्ताओँ को मिल जाती है।
आज भी अकसर मैं सुबह सबेरे पाँच बजे उठ जाता हूँ। आचमन आदि से निवृत्त होकर कंप्यूटर के सामने आ बैठता हूँ। बीच-बीच मेँ नहाने के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए ब्रेक लेता रहता हूँ। इससे काम की ऊब से आराम मिल जाता है।
शाम के समय, सात बजते-बजते टीवी के सामने जा बैठता हूँ, तथाकथित सस्ते सोप आपेरा यानी सीरियल सपत्नीक देखता हूँ। इसी बीच शाम का खाना भी हो जाता है।
और हाँ, जब से हमारे इलाक़े में बहुत सारे मल्टीप्लैक्स सिनेमा खुल गए हैँ, तो जब भी मन करता है फ़िल्म देख आते हैं। हर तरह की, अच्छी हो या बुरी– इससे कोई मतलब नहीँ होता। घर से निकलने का बहाना भर होता है। जब तब कोई रंगमंचीय नाटक। या कोई साहित्यिक गोष्ठी- यह बहुत ही कम।
थिसारस की रचना प्रक्रिया क्या है। मसलन आप शब्दों को कहां-कहां से और कैसे ढूंढते हैं। उनसे जुडे़ शब्दों को कैसे ढूंढते हैं। शब्दों के बीच के संबंध को ध्यान में रखकर उन्हें कैसे क्रम देते हैं ?
पहले हमें थिसारस और शब्दकोश का अंतर समझना चाहिए।
थिसारस को हम शब्द सूची भी कह सकते हैं। बस, फ़र्क़ यह है कि इसमें शब्दों का संकलन संदर्भ क्रम से किया जाता है। यह संदर्भ क्या हो, यह तय करना बड़ी टेढ़ी खीर है। अपने अनुभव से बताता हूँ। मूर्खतावश मैंने जब दो साल मेँ हिंदी का थिसारस बना डालने की बात सोची थी, तो रोजेट के थिसारस के आधार पर। मुझे लगा था कि उसका संदर्भ क्रम तो बना बनाया है, उसी के खाँचों में हिंदी के शब्द डालने ही तो हैं। पर बाबा रे, ऐसा संभव नहीं था।
हमने हिंदी कोशोँ के ‘अ’ से शब्द खोजने शुरू किए और उन्हें रोजेट के खाँचों में डालना चाहा तो पता चला कि वहाँ उनके उपयुक्त आर्थी कोटियाँ थीं ही नहीं। वे संदर्भ, वे भाव ही वहाँ नहीं थे। भारत के लिए वह मॉडल बेकार था। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई।
उसका थिसारस 1852 में बना था। 20वीं सदी का साठादिक दशक आते-आते उसके बृहद संस्करण बनने लगे। तब तक रोजेट का क्रम अधूरा मालूम पड़ने लगा था। मूल में कुल छः मुख्य विभाग थे। उनमें दो और जोड़े गए। खेद की बात यह है कि इन बृहद् तथाकथित अंतरराष्ट्रीय संस्करणोँ की रचना रोजेट के उत्तराधिकारियोँ से फ़्रैंचाइज़ लेकर कई प्रकाशकों द्वारा संपादक नियुक्त करवा के की गई। इन लोगों ने ऊपरी टीमटाम मात्र की। इधर-उधर किसी ऐंट्री की क्रम संख्या बदल दी गई– किसी अन्य प्रकाशक का कापीराइट ब्रेक करने भर के लिए। मूल आधार रोजेट का वही पुराना संदर्भ क्रम रहा।
रोजेट वैज्ञानिक थे, और उनका वर्गीकरण विज्ञान पर आधारित था। पर मानव मन वैज्ञानिक वर्गीकरण थोड़े ही जानता है! आम आदमी के लिए गेहूँ का संबंध अनाजों से है। विज्ञान में गेहूँ एक घास है। अतः रोजेट में गेहूँ, केला और घास एक साथ हैं। यह क्रम आम आदमी के काम का हो ही नहीँ सकता। हम स्टील या इस्पात की बात करते हैं, दिमाग़ में लोहा भी आता है। पर रोजेट में इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। लोहा धातुओं में है, इस्पात एलौय के अंतर्गत। शेर बिल्ली के साथ है, रीछ आदि वन्य पशुओं के साथ नहीं।
जब यह आधार छिन गया, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं। हमारा अपना छठी सदी का सुप्रसिद्ध ‘अमर कोश’ तो है ही। उसी को मॉडल बना लेते हैं। यह विचार और भी लचर निकला। कहाँ छठी सदी का वर्णाश्रम से ग्रस्त समाज और कहाँ आज का भारत। ‘अमर कोश’ में संगीत तो नैसर्गिक गतिविधि निकली, गायक शूद्र। कैसे संबंध बैठाएँ, कैसे कहाँ जोड़ें!
आपने अभी बताया कि रोजेट का खाँचा काम नहीं आया और न ही अमर कोश का। ऐसे में आपने कौन-सा तरीका अपनाया?
हम तो एक तरह से मर ही गए थे। कहाँ दो साल में काम पूरा करने की बात सोची थी, कहाँ कामचलाऊ क्रम की तलाश में ही चौदह साल निकल गए। बस, इतना था कि हमने शब्दों का संकलन एक दिन के लिए भी नहीं रोका। हर विषय और उसके उपविषय के कार्ड एक स्वतंत्र ट्रे में रखते गए। ट्रे हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनवाई थीं, और कार्ड भी अपने काम के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए थे। संदर्भ क्रम बदलना होता तो ट्रेओं का क्रम बदल देते। इसे ही मैँ अपनी शब्दोँ को कोई क्रम देने की तलाश की प्रक्रिया कह सकता हूँ। यह आसान सा तरीक़ा ही हमारे काम आया।
थिसारस का विचार आपके मन में कब आया और आपको यह काम इतना महत्वपूर्ण क्यों लगा कि आपने जमी-जमाई नौकरी छोड़ दी और अपना जीवन थिसारस को समर्पित कर दिया।
मैं आपको 22-23 साल के एक लड़के से मिलवाता हूँ। इससे पहले वह ‘सरिता’ पत्रिका में उपसंपादक था। शाम के समय सांध्य कॉलेज में पढ़ रहा था। बीए में पहुँचा, और मालिक तथा संपादक विश्वनाथ जी ने उसकी इंग्लिश के साथ-साथ विश्व साहित्य में रुचि देखी तो ‘कैरेवान’ (CARAVAN) में उप संपादक बना दिया। सबसे पहला काम था- सरिता की हिंदी कहानियों का इंग्लिश अनुवाद। साथ-साथ प्रकाशनार्थ आई इंग्लिश रचनाओं को पढ़ना, लेखकों से वांछित विषयों पर लिखवाना, और छपने के लिए तैयार करना। वह ठहरा नौसिखिया! बहुत से शब्द तो वह जानता ही नहीं था। हिंदी से अनुवाद करना हो या किसी इंग्लिश शब्द को बदल कर बेहतर करना हो, तो शब्द संपदा समृद्ध चाहिए। तभी किसी ने उससे रोजेट का थिसारस ख़रीदने को कहा। वह मगन हो गया, उसका दीवाना हो गया। जब वह ‘सरिता’ में था तो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद भी करता था। तब हिंदी शब्द नहीं मिलते थे। इसीलिए रोजेट देखते ही वह सोचने लगा कि ऐसी कोई किताब हिंदी में होनी चाहिए।
लेकिन वह जो लड़का था, जिससे मैंने आपको अभी मिलवाया, वह लड़का मैं था। मैं यह हिमाक़त सोच ही नहीं सकता था कि मैं वैसी कोई किताब बनाऊँ। मैं तो यही सोचता था, सोचता क्या था, मुझे पूरा भरोसा था कि तब (बीसवीं सदी के पचासादि दशक में) हिंदी शब्दावली बनाने के जो ताबड़तोड़ प्रयास हो रहे थे, उन्हीं में से हिंदी का थिसारस भी कभी-न-कभी निकलेगा ही। मैं तो अपने काम को बेहतर करने में लगा रहा। मेहनत कर रहा था, तो तरक्क़ी भी होती रही। लेकिन कभी इतना भी नहीं सोचा था कि मैं उस समूह की सभी पत्रिकाओं का एग्ज़क्टिव सहायक संपादक बन जाऊँगा। इस सैंस में मेरी कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। अगर भविष्य की कोई तस्वीर मन में थी थी तो बस यही कभी-न-कभी कंपोज़िंग विभाग का फ़ोरमैन बन पाऊँगा। बस, काम करता रहा, बढ़ता गया, बढ़ता क्या गया, बढ़ाया जाता रहा।
1973 तक वह लड़का 43 साल का अधेड़ हो चुका था। ‘माधुरी’ जैसी यशस्वी और लोकप्रिय पत्रिका का प्रथम संपादक बन चुका था। लेकिन दस साल वहाँ रह कर ऊब चुका था। बार-बार वह सोचता कि क्या इसीलिए पैदा हुआ हूँ। क्या यही उस की नियति है। और तब फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध भरी पार्टियों से परेशान थका-हारा वह 25-26 दिसंबर की रात देर रात तक सो नहीं पा रहा था। न जाने किसने उस रात में उसे याद दिलाया–
‘बीस साल पहले जो तेरी चाहत थी, हिंदी थिसारस की, वह अभी तक अधूरी है। तुझे जो तलाश है जीवन में कुछ करने की, तो उस चाहत को पूरा कर। इच्छा तेरी थी, सपना तेरा था। बस, उसे पूरा करने में जुट जा।’
तब तक मेरे जीवन का कोई सुनिश्चित उद्देश्य नहीँ था। अगली सुबह (26 दिसंबर 1973 की सुबह) मलाबार हिल पर सैर करते करते कुसुम और मैंने मिल कर संकल्प कर लिया चाहे जो हो, हम हिंदी को थिसारस देंगे।
आपके परिवार ने आपकी किस तरह मदद की।
उस सुबह से ही मैं और कुसुम पति-पत्नी से बढ़ कर सहकर्मी हो गए। बच्चे छोटे थे। सुमीत 13 साल का था, मीता 8 की। सबसे पहला काम था महाप्रयास के लिए अपने को तैयार करना। हर तरह के संदर्भ ग्रंथ ख़रीदे—अधिकतर हिंदी और इंग्लिश कोश थे। इंग्लिश के दसियों थिसारस भी ख़रीद डाले। यह भी पता था कि नौकरी छोड़ने के बाद जेब हल्की होगी। काफ़ी कपड़े भी बना लिए। साथ-साथ प्रोविडेंट फ़ंड बचत की दर बढ़ा दी। घर का ख़र्च कम से कम कर दिया।
19 अप्रैल, 1976 को नासिक में गोदावरी स्नान के बाद हमने किताब को पहला कार्ड बनाया। उस पर हम चारोँ के दस्तख़त हैं। सुमीत और मीता थे तो बच्चे, लेकिन उनके मन में सहभागिता की बात कहीँ अड़ी रही होगी। जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, हमारे काम के सक्रिय भागीदार बनते गए। कोई 1988 से सुमीत ने हमारे काम के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पर बल देना शुरू किया। बाद में उसने कार्डों के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया सँभाली। मीता ने इंग्लिश डाटा की आधारशिला तैयार की।
समाज के लिए कोश ग्रंथों की क्या उपयोगिता है ? या कहें की जीवंत समाज के लिए शब्दकोश क्यों ज़रूरी हैं ?
शब्द मानव की महानतम उपलब्धि हैं। शब्दों ने ही ज्ञान-विज्ञान को जन्म दिया, एक पीढ़ी से दूसरी तक, एक देश से दूसरे तक पहुँचाया, मानवों में संप्रेषण सहज बनाया। यही कारण है कि भाषा के जन्म के साथ ही थिसारस (शब्द सूचियाँ) और शब्दार्थ कोश बनने लगे थे। सबसे पहले सटीक थिसारस और शब्दकोश भारत में बने। निघंटु था तो कुल 1,800 शब्दों की सूची, लेकिन तत्कालीन समाज ने उसके निर्माता कश्यप को प्रजापति कह कर सम्माना। और फिर महर्षि यास्क ने निघंटु की व्याख्या के रूप में संसार को सबसे पहला शब्दार्थ कोश और ऐनसाइक्लोपीडिया दिया- निरुक्त। ये दोनों अभी तक पूरे सम्मान के भागी हैं।
शब्दकोश एक आदमी से दूसरे तक पहुँचे शब्द को प्रमाणित करते हैं, ताकि ग़लतफ़हमी की गुंजाइश न रहे। थिसारस हमें अपनी बात कहने के लिए सही शब्दावली देता है। शब्दकोश और थिसारस एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दो अलग तरह की चीज़ें हैं।
हिंदी का भविष्य क्या है ? वैश्वीकरण के दौर में क्या हिंदी सिमट कर रह जाएगी?
हिंदी को कई निराशावादी लोग एक मरती हुई ज़बान समझते और कहते फिर रहे हैं। वे उसी तरह के लोग हैं जो इस्लाम ख़तरे में, हिंदुत्व संकट में जैसे नारे लगाते रहते हैं। हिंदी में इंग्लिश शब्दों के बढ़ते चलन को देख कई बार उनकी बात सही लग सकती है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। बदलते समाज, बदलती तकनीक के साथ हिंदी का बदलना ज़रूरी है। यह बात हर भाषा पर लागू होती है। आज हिंदी वह नहीं है जो ‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ के ज़माने में थी, न ही वह जो भारतेंदु जी के युग में थी। और सन् 2050 में वह नहीं होगी, जो आज है। वह हर जगह से शब्द लेगी, विचार लेगी। नए मुहावरे आएँगे। नए लोग नई शैलियाँ लाएँगे। वे लोग नई वर्तनी भी ला सकते हैं। तब हिंदी संसार में शायद सबसे अधिक प्रचलित भाषाओं में बहुत ऊपर होगी।
आप देख रहे हैं, हिंदी के समाचार पत्र प्रसार संख्या में सबसे आगे हैं, और उनकी गुणवत्ता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। हिंदी के टीवी चैनल संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनलों में गिने जाते हैं। हमारी फ़िल्में पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय हो चुकी हैं। तो डर कैसा, डर किससे। आप यह बात समझ लीजिए कि हिंदी बोलने वाले संख्या में इतने अधिक हैं और आज हिंदी वाले संसार में एक बहुत बड़ा ग्राहक समूह हैं। उन तक माल पहुँचाने और बेचने के लिए दुनिया को नाक रगड़ कर उनके पास आना होगा। हिंदी ही क्योँ, दुनिया को भोजपुरी, ब्रजभाषा, गढ़वाली—सब के पास आना होगा।
आज विश्व की कई भाषाएँ मरणासन्न हैं। क्या उन्हें बचाया जा सकता है ?
जिन भाषाओं के बोलने वाले कम हैं, या कम होते जा रहे हैं, वे म्यूज़ियम पीस बन कर ही बची रह सकती हैं। यही बात शब्दों की भी है। मेरे बचपन के वे सब शब्द मर चुके हैं, जो उन चीज़ों के थे जो तब काम आती थीं, या उन रीतिरिवाज़ों के हैं जो तब चलते थे। दमड़ी, छदाम, कौड़ी, अधन्ना, इकन्नी कुछ ऐसे ही शब्द हैं। कुछ ही दिनों में चवन्नी शब्द भी भुला दिया जाएगा। यह होना अवश्यंभावी है।
अब आप की क्या योजनाएँ हैं ? हिंदी-इंग्लिश के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के कोश भी बनाएँगे क्या ?
हमारे सपने बहुत बड़े हैं। और योजनाएँ भी बहुत बड़ी हैं। अरविंद लैक्सिकन से जो पैसा आएगा, उसका बहुत बड़ा भाग हमारे डाटा में नई भाषाएँ जोड़ने में काम आएगा। तमिल और चीनी भाषाएँ हमारी प्राथमिकता हैं।
इसके पीछे जो राष्ट्रीय और देशभक्ति से भरा विचार है, आप वह समझने की कोशिश करें। भारत की आर्थिक और राजनीतिक सामर्थ्य बढ़ रही है, बढ़ेगी। जिस तरह इंग्लिश भाषी समाजों ने दुनिया भर के देशों से उनकी भाषाओं के कोश बनाए, जैसे इंग्लिश-हिंदी-इंग्लिश या इंग्लिश-चीनी-इंग्लिश, इंग्लिश-जापानी-इंग्लिश, उसी तरह हमारे देश को करना होगा- हिंदी-इंग्लिश-हिंदी, हिंदी-चीनी-हिंदी, हिंदी-जापानी-हिंदी… । सरकार तो इस तरफ़ कुछ करती नज़र नहीं आ रही। इतनी दूरदृष्टि भी उनके पास कभी नहीं रही है। सरकार न ही करे तो ठीक ही है। इंग्लिश में भी ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ अनेक निजी प्रकाशकों ने यह काम किया।
आपने बाहरी आर्थिक सहायता की बात शुरू में ही पूछी थी। तब मेरे पास अपने को सुपात्र सिद्ध करने का कोई साधन नहीं था। क्या था मैं ? एक महत्वाकांक्षी कोशकार तो था, पर था तो कोरा फ़िल्म पत्रकार ही। लेकिन अब तो मैं अपने को सिद्ध कर चुका हूँ। फिर भी मैं जानता हूँ कि मुझे या मेरे समूह को कहीं से कैसी भी सहायता नहीं मिलेगी। शायद मुझे माँगने की कला ही नहीं आती। लेकिन अब एक हद तक मैं और मेरे साथी आत्मनिर्भर हैं। हम समर्थ हैं, हमारे पास इरादा है। हम न सिर्फ़ तमिल और चीनी शब्द सँजोएँगे, हम जापानी, अरबी, फ़्रैंच, जरमन, स्पेनी—सभी भाषाएँ समाहित करेंगे। बरसों लगेंगे, शायद पीढ़ियाँ, लेकिन जो काम शुरू होता है, या होना चाहता है वह अपना कारिंदा भी चुन लेता है और उसके कंधे पर सवार होकर उसे धकेलता रहता है। इस काम ने हमें चुन लिया है।
‘अरविंद लैक्सिकन’ में आपने रोमन लिपि को भी शामिल किया है। इसकी ख़ास वज़ह क्या है ?
रोमन लिपि शामिल करने के पीछे एक सीधी सी समझ थी। कितने लोग हैं जो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं ? कितने सारे अ-हिंदी भारतीय हैं, जैसे, लदाखी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ जो हिंदी तो समझते हैं पर पढ़ना नहीँ जानते या समझना चाहते हैं पर देवनागरी न जानने के कारण पढ़ नहीं सकते, उनके लिए किसी कोश में हिंदी शब्दों की खोज के लिए रोमन लिपि होनी चाहिए। मेरे छोटे भाई विनोद अमरीका में रहते हैं। उनका बेटा रोहित बड़ा अफ़सर है, पर हिंदी नहीं जानता। विदेशों में बसे भारतीय परिवारोँ की दूसरी पीढ़ी का यही हाल है। पर उनका भारत प्रेम या हिंदी से लगाव कम नहीं हुआ है। अगर रोमन लिपि के साथ-साथ वे लोग वही शब्द देवनागरी में लिखा देखेंगे तो हिंदी का रंगरूप उनकी समझ में आने लगेगा।
अरविंद लैक्सिकन 24 जून से उपलब्ध हो गया है। उसे http://arvindkumar.me पर देखा जा सकता है। हो सकता है कुछ कमियाँ हों, हमारे सर्वर अभी उतने समर्थ न हों। पर हम और सर्वरों पर ख़र्च करने के संसाधन जुटा रहे हैं। मैं समझता हूँ उस साइट पर उपलब्ध अरविंद लैक्सिकन का नि:शुल्क संस्करण आम हिंदी भाषी परिवार की दैनिक शब्दावली की सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। हिंदी और इंग्लिश के ढेर सारे पर्याय और एक भाषा से दूसरी भाषा के लिए शब्दों की तलाश यहाँ पूरी होगी। लेकिन इसके लिए साइट पर रजिस्टर कराना– अरविंद परिवार का सदस्य बनना ज़रूरी है। आवश्यक फ़ार्म या प्रपत्र साइट पर ही मिलता है।
प्रेस में बाल श्रमिक के रूप में आपने करियर की शुरूआत की। बाद में वहाँ की सभी पत्रिकाओं के प्रभारी सहायक संपादक बने। ‘माधुरी’ और ‘सर्वोत्तम’ जैसी पत्रिकाओं के प्रथम संपादक बने। आपकी सफलता का राज़ क्या है ?
तीन राज़ हैं— मेहनत, लगन, ईमानदारी।
आपका जन्म मेरठ में हुआ। बचपन के कुछ वर्षों को छोड़कर आप मेरठ में नहीं रहे। दुनिया भर में घूमे। क्या मेरठ याद आता है ?
मेरठ शहर में जन्मा और वहाँ रहा बंदा मेरठ को कभी भूल ही नहीं सकता। नौचंदी उसे हमेशा याद आती रहेगी, वहाँ की रेवड़ी गज़क़ हमेशा मुँह में लार लाती रहेगी।
एक बार टाइम्स संस्थान की कर्ताधर्ता श्रीमती रमा जैन ने मुझ से पूछा था कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है। मेरा जवाब था, गुज़ारे लायक़ आमदनी और मेरठ में वास। उन्होंने कहा था कि गुज़ारे लायक़ आमदनी की बात समझ में आती है, मेरठ में रहना क्यों ? जवाब में मैंने पूछा था– आपने कभी मेरठ की चाट खाई है। वह हँस पड़ी थीं, और बोली थीं- मैं समझ गई।
आपको बताऊँ कि हम मेरठ वाले चटोरे होते हैं। सुबह नाश्ते में हलवाई की बेड़वीं के साथ जलेबी पर रखा हलवा, तीसरे पहर चाट पकौड़ी। चाट की बात यह है, कभी समोसा, कभी आलू का लच्छा, आलू का भल्ला (टिकिया, कटलेट), दही सौंठ वाली पकौड़ियाँ, गोलगप्पे (पानी पूरी) तो खाते ही हैं, वहाँ शादी-ब्याह में जो ख़ास तरह की कचौरी बनती है, वह कहीं और नहीं मिलती। बाहर हम उसके लिए तरसते रहते हैँ। यह और बात है कि अब न तो वैसा स्वास्थ्य है, न वैसा हाज़मा कि ये लज्जत पूरी तरह उठा सकें।
और एक बात। मेरठ खड़ी बोली का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन वहाँ की बोली वह नहीं है, जो आज की लिखत की हिंदी है। वहाँ के कुछ अजीब मुहावरे हैं। जैसे: अजी, हुआ बहुत! इस का मतलब होता है कि होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे कितने ही मुहावरे मैं गिनाता रह सकता हूँ। काश कोई उनका कोश बनाए।
Original article: http://lekhakmanch.com/?p=2417
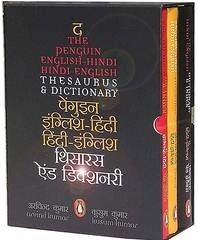


Comments