द्वितीयोऽध्यायः
सांख्य योग
सञ्जयोवाच
तं तथा कृपयाऽविष्टम् अश्रुपूर्णाऽऽकुलेक्षणम् ।
विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॥१॥
संजय ने कहा
अर्जुन का मन करुणा से भरा था. व्याकुल आँखोँ मेँ आँसू भर आए थे. वह विषाद से भरा था. उस की ऐसी हालत देख कर मधुसूदन ने कहा –
श्रीभगवान् उवाच
कुतस् त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्य-जुष्टम् अर्स्वग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन ॥२॥
श्री भगवान ने कहा
इस विषम काल मेँ तुझ पर मैल कैसा? यह आचरण आर्योँ जैसा नहीँ हैँ. अर्जुन, इस से स्वर्ग नहीँ मिलेगा, बल्कि बदनामी होगी.
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्वय्य् उपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदय-दौर्बल्यं त्यक्त्वोऽत्तिष्ठ परंतप ॥३॥
कायर मत बन! पार्थ, यह तुझे शोभा नहीँ देता. हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दे. उठ! खड़ा हो! तू परंतप है – तेरा काम है शत्रुओँ को हराना.
अर्जुनोवाच
कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रति-योत्स्यामि पूजार्हाव् अरिसूदन ॥४॥
अर्जुन ने कहा
भीष्म और द्रोण से मैँ कैसे लड़ूँ? मधुसूदन, उन पर बाण कैसे चलाऊँ? अरिसूदन, ये दोनोँ मेरे पूज्य हैँ.
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके ।
हत्वाऽऽर्थकामांस् तु गुरून् इहैव
भुञ्जीय भोगान् रुधिर-प्रदिग्धान् ॥५॥
महानुभाव गुरुजनोँ की हत्या करने से अच्छा तो यही है कि इस लोक मेँ मैँ दर दर का भिखारी बन जाऊँ. माना कि मेरे गुरुजन लालची हैँ, पर उन्हेँ मार कर मुझे क्या मिलेगा? ख़ून से सने भोग ही तो भोगूँगा!
न चैतद् विद्मः कतरन् नो गरीयो
यद् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्
तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥
यह भी तो नहीँ पता कि हमारी भलाई किस मेँ है. और यह भी तय नहीँ है कि हम जीतेँगे या वे. इन्हेँ मार कर हम जीना नहीँ चाहते. हमारे सामने जो खड़े हैँ, वे धृतराष्ट्र के बेटे हैँ.
कार्पण्य-दोषोपहत-स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्म-सम्मूढ-चेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन् मे
शिष्यस् तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥७॥
लाचारी ने मेरे स्वभाव को ग्रस लिया है. मैँ धर्मसंकट मेँ पड़ गया हूँ. आप ही बताइए. मेरे लिए क्या करना उचित है. मैँ आप का शिष्य हूँ. मुझे शिक्षा दीजिए. मैँ आप की शरण मेँ पड़ा हूँ.
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
यच्छोक म् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमाव् असपत्नम् ऋद्धं
राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् ॥८॥
मेरी इंद्रियाँ भारी शोक से सूख रही हैँ. इसे दूर करने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीँ देता. पूरी पृथिवी का राज्य अकेले मुझे मिल जाए या मैँ देवलोक का स्वामी बन जाऊँ तो भी यह शोक कम नहीँ होगा.
सञ्जयोवाच
एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः ।
न योत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥९॥
संजय ने कहा
इतना कह कर अर्जुन फिर बोला, ‘गोविंद, मैँ युद्ध नहीँ करूँगा!’ और चुप हो गया.
तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन्न् इव भारत ।
सेनयोर् उभयोर् मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः ॥१०॥
उस की बातेँ सुन कर पहले तो कृष्ण कुछ हँसे. फिर विषाद मेँ फँसे अर्जुन से बोले –
श्रीभगवान् उवाच
अशोच्यान् अन्वशोचस् त्वं प्रज्ञावादांश् च भाषसे ।
गतासून् अगतासूंश् च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥
श्री भगवान ने कहा
जिन के लिए दुःख नहीँ करना चाहिए, उन के लिए दुःख कर रहा है. और बातेँ ज्ञानियोँ जैसी बना रहा है! समझदार लोग उन के लिए शोक नहीँ करते जो चले गए हैँ, और न ही उन के लिए जो नहीँ गए हैँ.
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥
ऐसा नहीँ है कि कभी मैँ, तू और ये राजा लोग नहीँ थे. यह भी नहीँ है कि इस के बाद हम सब नहीँ होँगे.
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तर-प्राप्तिर् धीरस् तत्र न मुह्यति ॥१३॥
इस देह मेँ आ कर हमारी आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्थाओँ मेँ से गुज़रती है. बाद मेँ आत्मा एक से दूसरी देह मेँ चली जाती है. इस देह परिवर्तन पर धीरबुद्धि वाले लोग भ्रमित नहीँ होते.
मात्रा-स्पर्शास् तु कौन्तेय शीतोष्ण-सुख-दुःख-दाः ।
आगमाऽऽपायिनोऽनित्यास् तांस् तितिक्षस्व भारत ॥१४॥
भूत पदार्थोँ से स्पर्श होने पर सर्दी गरमी और सुख दुःख आदि महसूस होते हैँ. ये स्पर्श हमेशा नहीँ रहने वाले नहीँ होते. भरत वंशी अर्जुन, इन्हेँ सहन कर.
यं हि न व्यथयन्त्य् एते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
सम-दुःख-सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥
पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जिसे ये स्पर्श व्यथित नहीँ करते, वह धीर पुरुष दुःख और सुख को बराबर समझता है और अमर होने योग्य होता है.
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोर् अपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस् तत्त्व-दर्शिभिः ॥१६॥
जो नहीँ है – वह हो नहीँ सकता. जो है – वह मिट नहीँ सकता. तत्त्वदर्शी लोगोँ ने ये दोनोँ बातेँ अच्छी तरह समझ ली हैँ.
अविनाशि तु तद् विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् ।
विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति ॥१७॥
अविनाशी वही है जो इस सारे जगत मेँ फैला है. कोई भी ऐसा नहीँ है जो उस अव्यय – उस अविनाशी – का विनाश कर सके.
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥१८॥
ये सारे के सारे नाशवान शरीर नित्य नाशहीन और अप्रमेय आत्मा के हैँ. इस लिए, भारत, तू युद्ध कर.
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥
कोई कहता है कि आत्मा मारती है. कोई कहता है कि आत्मा को मारा जा सकता है. ये दोनोँ ही नहीँ जानते कि आत्मा न तो मारती है, न मारी जाती है.
न जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥
आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है. ऐसा भी नहीँ है कि हो कर यह फिर न हो. आत्मा अजन्मी है. लगातार रहती है. हमेशा से है. पुरानी है. शरीर के मरने पर भी मरती नहीँ.
वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनम् अजम् अव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥२१॥
जो आदमी जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मी और अव्यय है, पार्थ, वह कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है!
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य्
अन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
पुराने कपड़ोँ को उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है. वैसे ही पुराने शरीरोँ को उतार कर आत्मा नए शरीरोँ मेँ चली जाती है.
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्य् आपो न शोषयति मारुतः ॥२३॥
आत्मा को न शस्त्र काटते हैँ. न आग जलाती है. और न पानी भिगोता है. न हवा सुखाती है.
अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः ॥२४॥
इसे छेदा नहीँ जा सकता. जलाया नहीँ जा सकता. भिगोया नहीँ जा सकता और सुखाया भी नहीँ जा सकता. आत्मा नित्य है. सब मेँ है. स्थिर है. अचल है. सनातन है – हमेशा रहती है.
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते ।
तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि ॥२५॥
आत्मा न तो यह प्रकट है, न इस का कोई आकार है. अचिंत्य है – इसे बुद्धि से समझा नहीँ जा सकता. विकारहीन है – इस मेँ कैसा भी परिवर्तन नहीँ किया जा सकता. आत्मा को इस प्रकार जान लिया तो इस के लिए शोक करना उचित नहीँ रह जाता.
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि ॥२६॥
और यदि तू यह मानता है कि यह बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है तो भी, महाबाहु अर्जुन, इस का शोक करना तेरे लिए उचित नहीँ है.
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि ॥२७॥
जो जन्म लेता है उस की मृत्यु को टाला नहीँ जा सकता. जो मरता है उस का जन्म फिर हो कर रहेगा. जिस होनी को टाला नहीँ जा सकता, उस का शोक करना तेरे लिए उचित नहीँ है.
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त-मध्यानि भारत ।
अव्यक्त-निधनान्य् एव तत्र का परिवेदना ॥२८॥
भारत, संसार मेँ होने वाले जितने भी भूत पदार्थ और प्राणी हैँ, आरंभ मेँ उन का कोई रूप, रंग और आकार नहीँ होता. केवल मध्य काल मेँ वे व्यक्त होते हैँ. अंत मेँ वे फिर अव्यक्त हो जाते हैँ. तब उन का दुःख कैसा?
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्
आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच् चैनं अन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥२९॥
इस बात को कोई बड़े अचरज से देखता है. कोई इस का वर्णन आश्चर्य के रूप मेँ करता है. कोई इसे सुन कर अचरज मेँ डूब जाता है. लेकिन देख सुन कर भी कोई इसे पूरी तरह नहीँ समझता.
देही नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि ॥३०॥
सब के शरीर मेँ जो देह धारण करने वाली आत्मा है, वह नित्य है. इस का वध नहीँ किया जा सकता. भारत, भौतिक प्राणियोँ के लिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीँ है.
स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥
तू क्षत्रिय है. तू क्षत्रियोँ के स्वधर्म का, कर्तव्य का भी ख़्याल कर! काँपना घबराना तुझे शोभा नहीँ देता. क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़ कर कोई अन्य श्रेयस् कर्म नहीँ है.
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग-द्वारम् अपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् ॥३२॥
अनायास ही तुझे स्वर्ग का द्वार खुला मिल गया है. पार्थ, क्षत्रियोँ को युद्ध का ऐसा मौक़ा बड़े भाग्य से मिलता है.
अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि ॥३३॥
अगर इस धर्मयुद्ध से मुँह मोड़ लेगा, तो तू अपने क्षत्रिय धर्म को खो बैठेगा. इस से तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुझे पाप लगेगा.
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते ॥३४॥
तेरी ऐसी भारी बदनामी होगी जो कभी नहीँ मिटेगी. माननीय पुरुषोँ के लिए बदनामी मौत से भी बड़ी होती है.
भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्॥३५॥
बड़े बड़े महारथी योद्धा कहेँगे कि डर कर तू रण से भाग गया. अब तक जो लोग तेरी प्रशंसा करते हैँ वही अब तुझे तुच्छ समझने लगेँगे.
अवाच्य-वादांश् च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस् तव सार्मथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥३६॥
तेरा बुरा चाहने वाले लोग तेरी सार्मथ्य की – तेरी वीरता की – निंदा करेँगे. वे अनकहनी बातेँ कहेँगे. इस से बड़े दुःख की बात और क्या होगी?
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-निश्चयः ॥३७॥
युद्ध मेँ जो तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा. जीत गया तो पृथिवी का राज्य भोगेगा. इस लिए, कौंतेय, युद्ध का निश्चय कर, उठ, खड़ा हो.
सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि ॥३८॥
सुख और दुःख को, लाभ और हानि को, जीत और हार को बराबर समझ. युद्ध के लिए तैयार हो. ऐसा करने से तुझे पाप नहीँ लगेगा.
एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर् योगे त्विमां शृणु ।
बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म-बन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥
यह ज्ञान मैँ ने तुझे सांख्य योग के आधार पर बताया है. अब मैँ तुझे बुद्धि योग के आधार पर ज्ञान सुनाता हूँ. इस से प्राप्त बुद्धि से तू कर्म के बंधनोँ को काट देगा.
नेहाभिक्रम-नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥४०॥
इस योग मेँ प्रयत्न का – उपक्रम का, प्रयास का – नाश नहीँ होता. उस का उलटा प्रभाव भी नहीँ पड़ता. इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महाभय से मुक्ति दिलाता है.
व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश् च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥
कुरुनंदन, इस योग मेँ व्यवसाय बुद्धि – कर्म निर्धारक बुद्धि – बस एक है. लेकिन अव्यवसायी बुद्धि वालोँ की, कर्महीनोँ की सोचने समझने की शक्ति इधर उधर बिखरी होती है.
याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य् अविपश्चितः ।
वेद-वाद-रताः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः ॥४२॥
वे अज्ञानी लोग बड़ी लुभावनी, लच्छेदार, पुष्पित बातेँ करते हैँ. वेदोँ के अर्थ की खीँचतान मेँ लगे रहते हैँ. बड़े दावे के साथ कहते हैँ कि उन के सिद्धांतोँ के अतिरिक्त कुछ नहीँ है.
कामात्मानः स्वर्ग-परा जन्म-कर्म-फल-प्रदाम् ।
क्रिया-विशेष-बहुलां भोगैश्वर्य-गतिं प्रति ॥४३॥
उन का मन इच्छाओँ और कामनाओँ से भरा होता है. स्वर्ग पाना चाहते हैँ. उन का कहना है कि जीवन की सभी क्रियाएँ और कार्य के फल की इच्छा से और ऐश्वर्य भोगने के लिए किए जाते हैँ.
भोगैश्वर्य-प्रसक्तानां तयापहृत-चेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥४४॥
ऐसी बातोँ से भ्रमित हो कर भोग और ऐश्वर्य मेँ लिप्त लोगोँ की कर्मबुद्धि – कर्तव्य चेतना – एकाग्र नहीँ होती.
त्रैगुण्य-विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्य-सत्त्वस्थो निर्योग-क्षेम आत्मवान्॥४५॥
सत्त्व, रज और तम – ये तीन गुण वेदोँ का विषय हैँ. अर्जुन, तू इन तीन गुणोँ से अलग हो जा. तू हर्ष और विषाद, सर्दी और गरमी, आदि परस्पर विरोधी द्वंद्वोँ से ऊपर उठ. नित्य सत्त्व – परम सत्य – मेँ हमेशा स्थित रह. तू निर्योग क्षेम हो – सांसारिक आशाओँ और आशंकाओँ से मुक्त हो कर अपनी आत्मा को पाने मेँ सफल हो.
यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥४६॥
भारी बाढ़ आ जाने पर बेचारे पोखर की क्या बिसात! ज्ञान पा लेने पर ब्राह्मण के लिए वही हालत सारे वेदोँ की हो जाती है.
कर्मण्य् एवाधिकारस् ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्म-फल-हेतुर् भूर् मा ते सङ्गोस्त्व् अकर्मणि॥४७॥
तेरा अधिकार कर्म मेँ ही है, फल मेँ कभी नहीँ. तू कर्म मेँ फल की इच्छा मत कर. कभी कर्म से मुँह मत मोड़!
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धय्-असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥
योग मेँ स्थित हो. कर्म कर. आसक्ति को त्याग. धनंजय, कर्म की सफलता और असफलता को एक समान समझ. इस सम भाव को योग कहते हैँ.
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि-योगाद् धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फल-हेतवः॥४९॥
कर्म तो बुद्धि योग के सामने अत्यंत तुच्छ है. धनंजय, तू बुद्धि की शरण मेँ जाने की इच्छा कर. फल की कामना करने वाले लोग कंजूस हैँ, दीन हैँ.
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते ।
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥५०॥
बुद्धि को योग मेँ लगा कर पुरुष पुण्य और पाप को त्याग देता है. इस लिए तू योग की साधना कर. काम को अच्छी तरह करने का, कर्म मेँ कुशलता का, दक्षता का, नाम योग है.
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्म-बन्ध-विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य् अनामयम्॥५१॥
बुद्धि योग प्राप्त हो जाने पर समझदार लोग कर्म का फल त्याग देते हैँ. ऐसा कर के वे जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैँ और दोषहीन पद को पाते हैँ.
यदा ते मोह-कलिलं बुद्धिर् व्यति-तरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥५२॥
तेरी बुद्धि मोह के – भ्रम के, अज्ञान के – दलदल को पार कर लेगी तो तू श्रुत (वेद जो सुने जा चुके हैँ) और श्रोतव्य (वेदोँ पर प्रवचन जो सुनने योग्य हैँ) तेरे लिए निरर्थक हो जाएँगे.
श्रुति-विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्याति निश्चला ।
समाधाव् अचला बुद्धिस् तदा योगम् अवाप्स्यसि ॥५३॥
उन की परस्पर विरोधी बातेँ सुन सुन कर तेरी बुद्धि विचलित हो चुकी है. समाधि मेँ केंद्रित हो कर, स्थिर हो कर, आत्म चिंतन करने से तुझे बुद्धि योग प्राप्त होगा.
अर्जुनोवाच
स्थित-प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थित-धीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् ॥५४॥
अर्जुन ने कहा
केशव, समाधि मेँ स्थित और स्थिर बुद्धि वाले – स्थितप्रज्ञ – पुरुष की परिभाषा क्या है, उस के लक्षण क्या हैँ? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोले, कैसे बैठे, कैसे चले?
श्रीभगवान् उवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्य् एवात्मना तुष्टः स्थित-प्रज्ञस् तदोच्यते ॥५५॥
श्री भगवान ने कहा
जब कोई अपने मन की सारी कामनाओँ – इच्छाओँ, चाहतोँ – को त्याग देता है, तो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैँ. वह आत्मा द्वारा आत्मा मेँ संतुष्ट रहता है.
दुःखेष्व् अनुद्विग्न-मनाः सुखेषु विगत-स्पृहः ।
वीत-राग-भय-क्रोधः स्थित-धीर् मुनिर् उच्यते ॥५६॥
दुःख मिलने पर उस का मन शोक से व्याकुल नहीँ होता. सुख की लालसा उसे नहीँ होती. वह रागहीन हो जाता है – उस का मन कहीँ आसक्त नहीँ होता. उसे डर नहीँ होता. उसे क्रोध नहीँ आता. ऐसे मननशील मुनि को स्थितधी या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है.
यः सर्वत्राऽऽनभिस्नेहस् तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥
उसे कहीँ भी लगाव नहीँ है, स्नेह नहीँ है. भला और बुरा मिलने पर वह न ख़ुश होता है और न दुःख मनाता है. ऐसे मनुष्य की प्रज्ञा स्थिर है.
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीऽऽन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥
स्थिर होने के लिए कछुआ अपने अंगोँ को पूरी तरह भीतर समेट लेता है. वैसे ही जब कोई अपनी सारी इंद्रियोँ को उन के विषय भोगोँ से हटा कर आत्मकेंद्रित कर लेता है, तब उस की प्रज्ञा स्थिर होती है.
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥
भोगोँ का त्याग करने से देहधारी आत्मा के विषय भोग छूट जाते हैँ. पर उन विषयोँ का रस, उन की चाहत, नहीँ छूटती. लेकिन परम सत्य को पा कर यह चाहत भी छूट जाती है.
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥
कौंतेय, प्रयत्नशील और बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियाँ ज़बरदस्ती विचलित कर देती हैँ, क्योँ कि वे बड़ी शक्तिशाली होती हैँ.
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥
उन सब इंद्रियोँ को संयमित कर के योग की साधना मेँ बैठे और मुझ मेँ मन लगाए. इस प्रकार जो इंद्रियोँ को वश मेँ कर लेता है, उस की प्रज्ञा स्थिर है.
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस् तेषूपजायते ।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते॥६२॥
विषय भोगोँ मेँ मन रमाने से मनुष्य भोगोँ मेँ आसक्त हो जाता है. आसक्ति से कामना का – चाहत का – जन्म होता है. और चाहत से क्रोध उपजता है.
क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति-विभ्राम ।
स्मृति-भ्रंशाद् बुद्धि-नाशो बुद्धि-नाशात् प्रणश्यति ॥६३॥
क्रोध से सम्मोह – भ्रम, अविवेक – उपजता है. सम्मोह से स्मरण शक्ति जाती रहती है. स्मरण शक्ति न रहे तो बुद्धि का नाश हो जाता है. बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है.
राग-द्वेष-वियुक्तैस् तु विषयान् इन्द्रियैश् चरन् ।
आत्म-वश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति ॥६४॥
मनुष्य राग और द्वेष से दूर हो तो उसे न तो सुख की इच्छा होती है न दुःख की अनिच्छा. वह मात्र अपनी इंद्रियोँ से सांसारिक विषयोँ का भोग करता है. वह अपने को पूरी तरह नियंत्रण मेँ रखता है. उसे मन की शांति मिलती है. आंतरिक प्रसाद मिलता है.
प्रसादे सर्व-दुःखानां हानिर् अस्योपजायते ।
प्रसन्न-चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥
आंतरिक प्रसाद मिलने पर उस के सारे दुःख दूर हो जाते हैँ. ऐसे प्रसन्नचित् पुरुष की बुद्धि पूर्णतः स्थिर हो जाती है.
नास्ति बुद्धिर् अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६६॥
जिसे बुद्धि योग न मिला हो, उस मेँ बुद्धि नहीँ होती, न ही उस मेँ भावना – दृढ़ निष्ठा – होती है. भावनाहीन को शांति नहीँ मिलती. जिसे शांति नहीँ, उसे सुख कहाँ?
इन्द्रियाणां हिं चरतां यन् मनोऽनुविधीयते ।
तद् अस्य हरति प्रज्ञां वायुर् नावम् इवाम्भसि ॥६७॥
इंद्रियोँ के पीछे पीछे भागने वाला मन बुद्धि को वैसे ही भगा ले जाता है जैसे हवा नाव को पानी मेँ भगा ले जाती है.
तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीऽऽन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥
इस लिए, महाबाहु, जिस ने अपनी इंद्रियोँ को विषय भोगोँ से पूरी तरह हटा लिया है, उस की प्रज्ञा स्थिर है.
या निशा सर्व-भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥
सांसारिक प्राणी जब सोते हैँ, तब संयमी जागता है. जब संसार जागता है, तो मुनि रात मानता है.
आपूर्यमाणम् अचल-प्रतिष्ठं
समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्ववत्
तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिम् आप्नोति न काम-कामी ॥७०॥
सब ओर से भरे पूरे समुद्र मेँ चारोँ ओर से आ कर नदियाँ समाती रहती हैँ और उसे विचलित नहीँ कर पातीँ. इसी तरह सारी कामनाएँ जिस पुरुष मेँ समा जाती हैँ, शांति उसे मिलती है, न कि कामनाओँ के पीछे भागने वाले को.
विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश् चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति ॥७१॥
कामनाओँ को त्याग कर जो पुरुष बिना लालसा के आचरण करता है, उस मेँ ममता नहीँ होती – उस मेँ अपनी अलग सत्ता का भाव नहीँ होता. वह निरहंकार होता है – उस मेँ ‘मैँ’ नहीँ होता. वह अपने को कर्मोँ का कर्ता नहीँ मानता. उसे शांति मिलती है.
एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म-निर्वाणम् ऋच्छति ॥७२॥
पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है. इसे पा कर मोह – भ्रम – नहीँ रहता. अंत काल मेँ, मृत्यु के समय भी, इस मेँ स्थित हो तो मनुष्य को ब्रह्म निर्वाण मिलता है.
इति श्रीमद्-भगवद्-गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म-विद्यायां योग-शास्त्रे श्री-कृष्णार्जुन-संवादे सांख्य-योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः
यह था श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मेँ सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय
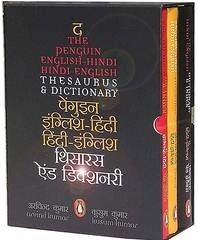
Comments